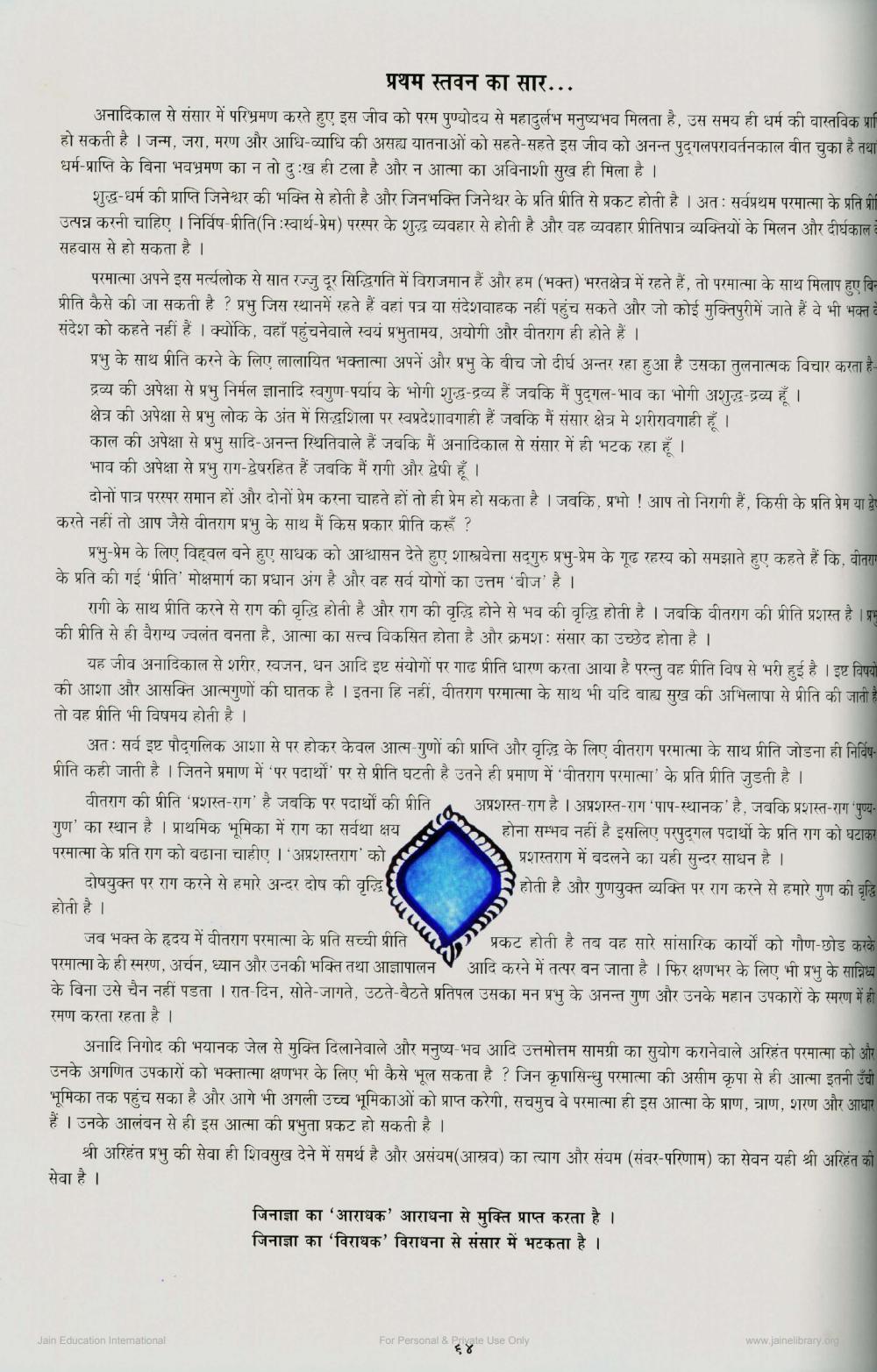________________
प्रथम स्तवन का सार... अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए इस जीव को परम पुण्योदय से महादुर्लभ मनुष्यभव मिलता है, उस समय ही धर्म की वास्तविक प्रा हो सकती है । जन्म, जरा, मरण और आधि-व्याधि की असह्य यातनाओं को सहते-सहते इस जीव को अनन्त पुद्गलपरावर्तनकाल बीत चुका है तथा धर्म-प्राप्ति के बिना भवभ्रमण का न तो दु:ख ही टला है और न आत्मा का अविनाशी सुख ही मिला है।
शुद्ध-धर्म की प्राप्ति जिनेश्वर की भक्ति से होती है और जिनभक्ति जिनेश्वर के प्रति प्रीति से प्रकट होती है । अतः सर्वप्रथम परमात्मा के प्रति प्रो उत्पन्न करनी चाहिए । निर्विष प्रीति(निःस्वार्थ-प्रेम) परस्पर के शुद्ध व्यवहार से होती है और वह व्यवहार प्रीतिपात्र व्यक्तियों के मिलन और दीर्घकाल सहवास से हो सकता है। ____ परमात्मा अपने इस मर्त्यलोक से सात रज्जु दूर सिद्धिगति में विराजमान हैं और हम (भक्त) भरतक्षेत्र में रहते हैं, तो परमात्मा के साथ मिलाप हुए दिन प्रीति कैसे की जा सकती है ? प्रभु जिस स्थानमें रहते हैं वहां पत्र या संदेशवाहक नहीं पहुंच सकते और जो कोई मुक्तिपुरीमें जाते हैं वे भी भक्त । संदेश को कहते नहीं हैं । क्योंकि, वहाँ पहुंचनेवाले स्वयं प्रभुतामय, अयोगी और वीतराग ही होते हैं ।
प्रभु के साथ प्रीति करने के लिए लालायित भक्तात्मा अपने और प्रभु के बीच जो दीर्घ अन्तर रहा हुआ है उसका तुलनात्मक विचार करता है। द्रव्य की अपेक्षा से प्रभु निर्मल ज्ञानादि स्वगुण पर्याय के भोगी शुद्ध-द्रव्य हैं जबकि मैं पुद्गल-भाव का भोगी अशुद्ध द्रव्य हूँ । क्षेत्र की अपेक्षा से प्रभु लोक के अंत में सिद्धशिला पर स्वप्रदेशावगाही हैं जबकि मैं संसार क्षेत्र मे शरीरावगाही हूँ। काल की अपेक्षा से प्रभु सादि-अनन्त स्थितिवाले हैं जबकि मैं अनादिकाल से संसार में ही भटक रहा हूँ | भाव की अपेक्षा से प्रभु राग-द्वेषरहित हैं जबकि मैं रागी और द्वेषी हूँ।
दोनों पात्र परस्पर समान हों और दोनों प्रेम करना चाहते हों तो ही प्रेम हो सकता है । जबकि, प्रभो ! आप तो निरागी हैं, किसी के प्रति प्रेम या द्वे करते नहीं तो आप जैसे वीतराग प्रभु के साथ मैं किस प्रकार प्रीति करूँ ?
प्रभु-प्रेम के लिए विह्वल बने हुए साधक को आश्वासन देते हुए शास्त्रवेत्ता सद्गुरु प्रभु-प्रेम के गूढ रहस्य को समझाते हुए कहते हैं कि, वीतरा के प्रति की गई 'प्रीति' मोक्षमार्ग का प्रधान अंग है और वह सर्व योगों का उत्तम 'बीज' है ।
रागी के साथ प्रीति करने से राग की वृद्धि होती है और राग की वृद्धि होने से भव की वृद्धि होती है । जबकि वीतराग की प्रीति प्रशस्त की प्रीति से ही वैराग्य ज्वलंत बनता है, आत्मा का सत्त्व विकसित होता है और क्रमशः संसार का उच्छेद होता है ।
यह जीव अनादिकाल से शरीर, स्वजन, धन आदि इष्ट संयोगों पर गाढ प्रीति धारण करता आया है परन्तु वह प्रीति विष से भरी हुई है । इष्ट विषय की आशा और आसक्ति आत्मगुणों की घातक है । इतना हि नहीं, वीतराग परमात्मा के साथ भी यदि बाह्य सुख की अभिलाषा से प्रीति की जाती है तो वह प्रीति भी विषमय होती है ।
अतः सर्व इष्ट पौदगलिक आशा से पर होकर केवल आत्म-गुणों की प्राप्ति और वृद्धि के लिए वीतराग परमात्मा के साथ प्रीति जोडना ही निर्विषप्रीति कही जाती है । जितने प्रमाण में पर पदार्थों' पर से प्रीति घटती है उतने ही प्रमाण में वीतराग परमात्मा' के प्रति प्रीति जुडती है |
वीतराग की प्रीति ‘प्रशस्त-राग' है जबकि पर पदार्थों की प्रीति अप्रशस्त-राग है । अप्रशस्त-राग पाप-स्थानक' है, जबकि प्रशस्त-राग 'पुण्यगुण' का स्थान है । प्राथमिक भूमिका में राग का सर्वथा क्षय 6 होना सम्भव नहीं है इसलिए परपुद्गल पदार्थो के प्रति राग को घटाकर परमात्मा के प्रति राग को बढाना चाहीए । 'अप्रशस्तराग' को
प्रशस्तराग में बदलने का यही सुन्दर साधन है । दोषयुक्त पर राग करने से हमारे अन्दर दोष की वृद्धि
होती है और गुणयुक्त व्यक्ति पर राग करने से हमारे गुण की वृद्धि होती है।
जब भक्त के हृदय में वीतराग परमात्मा के प्रति सच्ची प्रीति ५ " प्रकट होती है तब वह सारे सांसारिक कार्यों को गौण-छोड करके परमात्मा के ही स्मरण, अर्चन, ध्यान और उनकी भक्ति तथा आज्ञापालन आदि करने में तत्पर बन जाता है । फिर क्षणभर के लिए भी प्रभु के सान्निध्या के बिना उसे चैन नहीं पडता । रात-दिन, सोते-जागते, उठते-बैठते प्रतिपल उसका मन प्रभु के अनन्त गुण और उनके महान उपकारों के स्मरण में ही रमण करता रहता है।
अनादि निगोद की भयानक जेल से मुक्ति दिलानेवाले और मनुष्य-भव आदि उत्तमोत्तम सामग्री का सुयोग करानेवाले अरिहंत परमात्मा को और उनके अगणित उपकारों को भक्तात्मा क्षणभर के लिए भी कैसे भूल सकता है ? जिन कृपासिन्धु परमात्मा की असीम कृपा से ही आत्मा इतनी उँची भूमिका तक पहुंच सका है और आगे भी अगली उच्च भूमिकाओं को प्राप्त करेगी, सचमुच वे परमात्मा ही इस आत्मा के प्राण, त्राण, शरण और आधार हैं । उनके आलंबन से ही इस आत्मा की प्रभुता प्रकट हो सकती है।
श्री अरिहंत प्रभु की सेवा ही शिवसुख देने में समर्थ है और असंयम(आस्रव) का त्याग और संयम (संवर-परिणाम) का सेवन यही श्री अरिहंत की सेवा है।
जिनाज्ञा का 'आराधक' आराधना से मुक्ति प्राप्त करता है । जिनाज्ञा का 'विराधक' विराधना से संसार में भटकता है ।
Jain Education Intemational
For Personal & Plate Use Only
www.jainelibrary.org