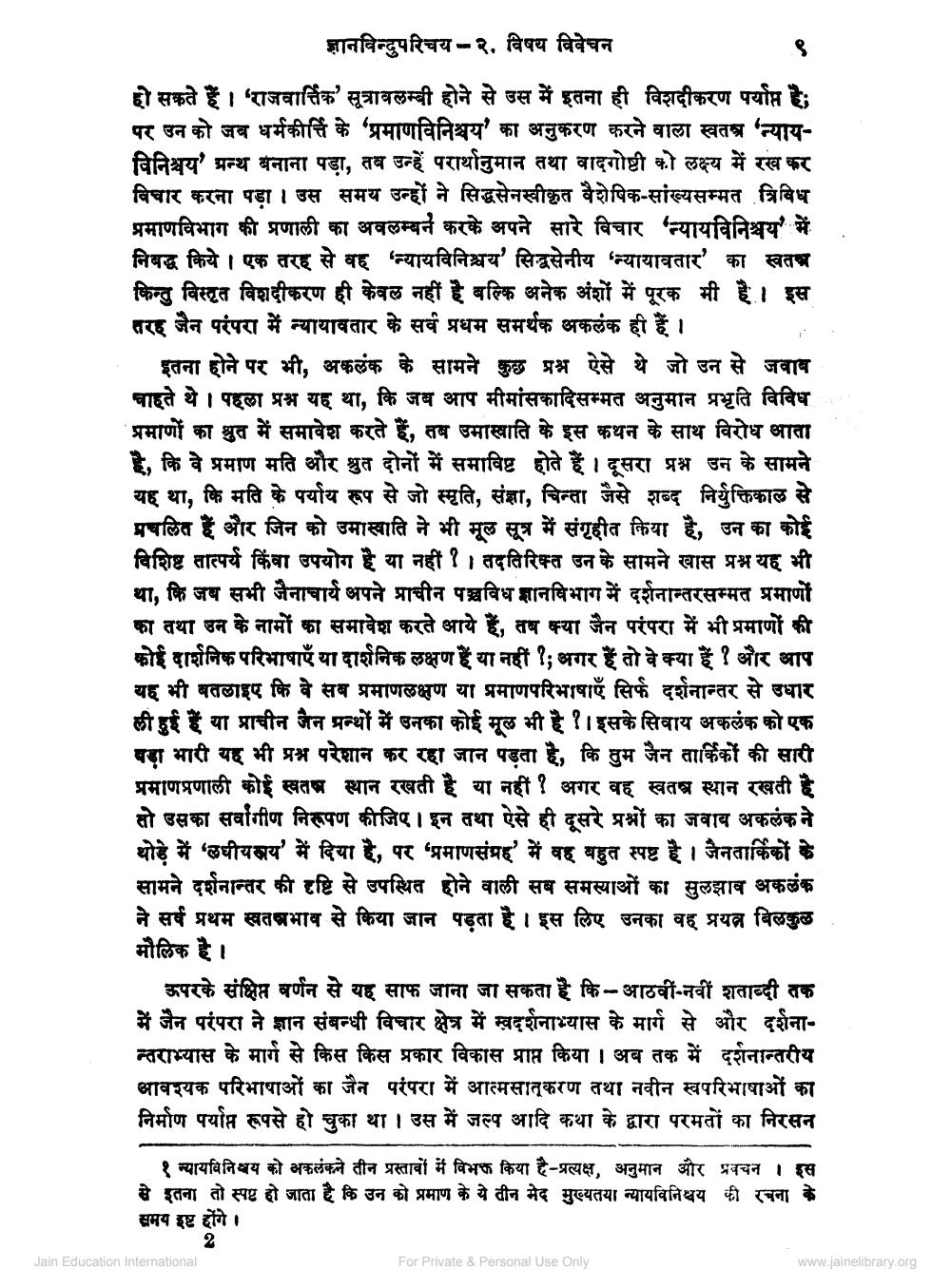________________
ज्ञानविन्दुपरिचय - २. विषय विवेचन हो सकते हैं। 'राजवार्तिक' सूत्रावलम्बी होने से उस में इतना ही विशदीकरण पर्याप्त है। पर उन को जब धर्मकीर्ति के 'प्रमाणविनिश्चय' का अनुकरण करने वाला स्वतत्र 'न्यायविनिश्चय' ग्रन्थ बनाना पड़ा, तब उन्हें परार्थानुमान तथा वादगोष्टी को लक्ष्य में रख कर विचार करना पड़ा। उस समय उन्हों ने सिद्धसेनस्वीकृत वैशेषिक-सांख्यसम्मत त्रिविध प्रमाणविभाग की प्रणाली का अवलम्बन करके अपने सारे विचार 'न्यायविनिश्चय में निबद्ध किये । एक तरह से वह 'न्यायविनिश्चय' सिद्धसेनीय 'न्यायावतार' का स्वतत्र किन्तु विस्तृत विशदीकरण ही केवल नहीं है बल्कि अनेक अंशों में पूरक भी है। इस तरह जैन परंपरा में न्यायावतार के सर्व प्रथम समर्थक अकलंक ही हैं। ___ इतना होने पर भी, अकलंक के सामने कुछ प्रश्न ऐसे थे जो उन से जवाब चाहते थे। पहला प्रश्न यह था, कि जब आप मीमांसकादिसम्मत अनुमान प्रभृति विविध प्रमाणों का श्रुत में समावेश करते हैं, तब उमास्वाति के इस कथन के साथ विरोध आता है, कि वे प्रमाण मति और श्रुत दोनों में समाविष्ट होते हैं। दूसरा प्रश्न उन के सामने यह था, कि मति के पर्याय रूप से जो स्मृति, संज्ञा, चिन्ता जैसे शब्द नियुक्तिकाल से प्रचलित हैं और जिन को उमास्वाति ने भी मूल सूत्र में संगृहीत किया है, उन का कोई विशिष्ट तात्पर्य किंवा उपयोग है या नहीं ? । तदतिरिक्त उन के सामने खास प्रभ यह भी था, कि जब सभी जैनाचार्य अपने प्राचीन पश्चविध ज्ञान विभाग में दर्शनान्तरसम्मत प्रमाणों का तथा उन के नामों का समावेश करते आये है, तब क्या जैन परंपरा में भी प्रमाणों की कोई दार्शनिक परिभाषाएँ या दार्शनिक लक्षण हैं या नहीं ?; अगर है तो वे क्या है ? और आप यह भी बतलाइए कि वे सब प्रमाणलक्षण या प्रमाणपरिभाषाएँ सिर्फ दर्शनान्तर से उधार ली हुई है या प्राचीन जैन प्रन्थों में उनका कोई मूल भी है । इसके सिवाय अकलंक को एक पड़ा भारी यह भी प्रश्न परेशान कर रहा जान पड़ता है, कि तुम जैन तार्किकों की सारी प्रमाणप्रणाली कोई स्वतन्त्र स्थान रखती है या नहीं ? अगर वह स्वतन्त्र स्थान रखती है तो उसका सर्वांगीण निरूपण कीजिए । इन तथा ऐसे ही दूसरे प्रभों का जवाब अकलंकने थोड़े में 'लघीयत्रय' में दिया है, पर 'प्रमाणसंग्रह' में वह बहुत स्पष्ट है । जैनतार्किकों के सामने दर्शनान्तर की दृष्टि से उपस्थित होने वाली सब समस्याओं का सुलझाव अकलंक ने सर्व प्रथम स्वतत्रभाव से किया जान पड़ता है। इस लिए उनका वह प्रयत्न बिलकुल मौलिक है।
ऊपरके संक्षिप्त वर्णन से यह साफ जाना जा सकता है कि-आठवीं-नवीं शताब्दी तक में जैन परंपरा ने ज्ञान संबन्धी विचार क्षेत्र में स्वदर्शनाभ्यास के मार्ग से और दर्शनान्तराभ्यास के मार्ग से किस किस प्रकार विकास प्राप्त किया। अब तक में दर्शनान्तरीय आवश्यक परिभाषाओं का जैन परंपरा में आत्मसातकरण तथा नवीन स्वपरिभाषाओं का निर्माण पर्याप्त रूपसे हो चुका था। उस में जल्प आदि कथा के द्वारा परमतों का निरसन
१न्यायविनिक्षय को अकलंकने तीन प्रस्तावों में विभक्त किया है-प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रवचन । इस से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि उन को प्रमाण के ये तीन मेद मुख्यतया न्यायविनिश्चय की रचना के समय इष्ट होंगे।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org