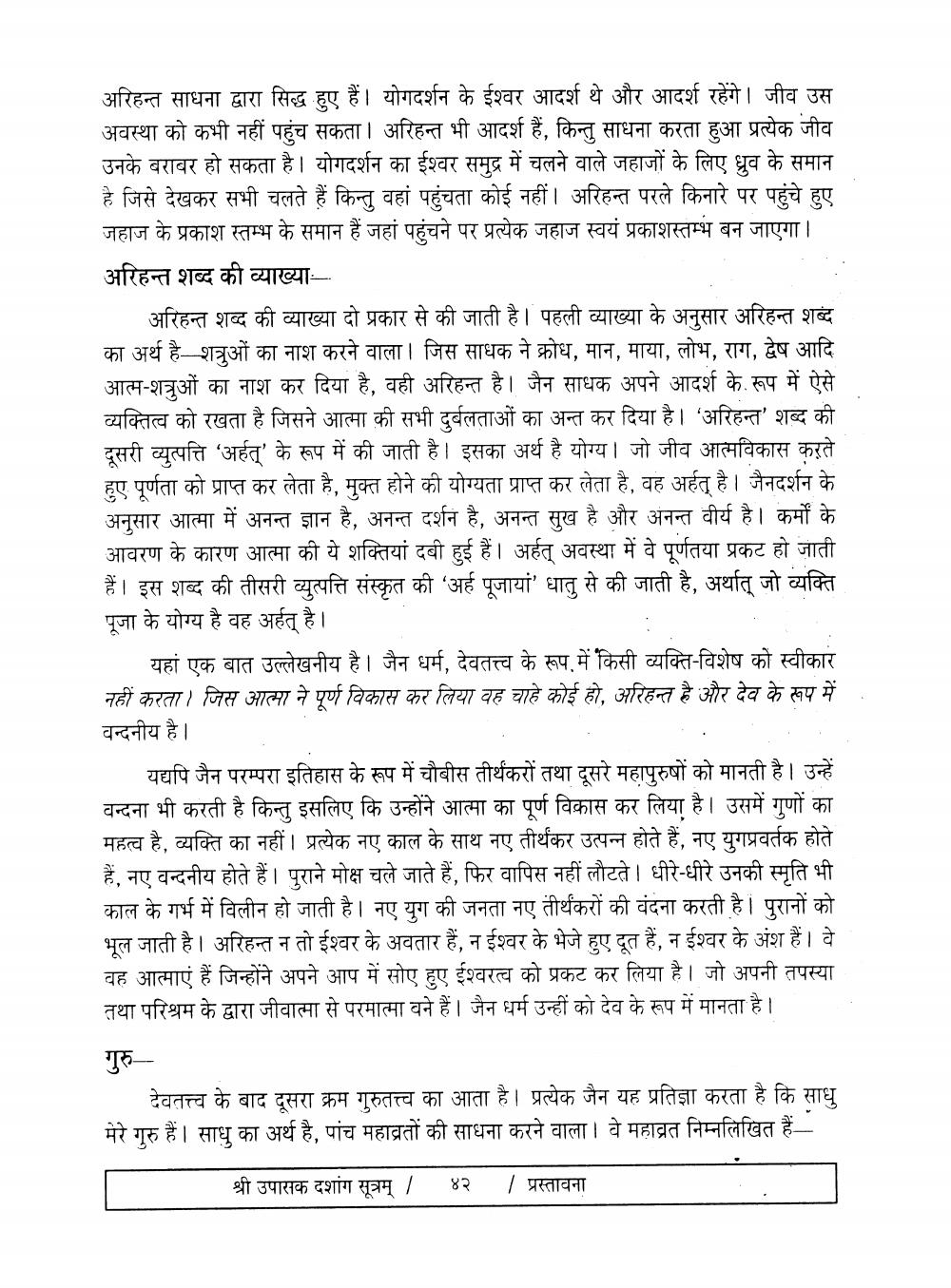________________ अरिहन्त साधना द्वारा सिद्ध हुए हैं। योगदर्शन के ईश्वर आदर्श थे और आदर्श रहेंगे। जीव उस अवस्था को कभी नहीं पहुंच सकता। अरिहन्त भी आदर्श हैं, किन्तु साधना करता हुआ प्रत्येक जीव उनके बराबर हो सकता है। योगदर्शन का ईश्वर समुद्र में चलने वाले जहाजों के लिए ध्रुव के समान है जिसे देखकर सभी चलते हैं किन्तु वहां पहुंचता कोई नहीं। अरिहन्त परले किनारे पर पहुंचे हुए जहाज के प्रकाश स्तम्भ के समान हैं जहां पहुंचने पर प्रत्येक जहाज स्वयं प्रकाशस्तम्भ बन जाएगा। अरिहन्त शब्द की व्याख्या अरिहन्त शब्द की व्याख्या दो प्रकार से की जाती है। पहली व्याख्या के अनुसार अरिहन्त शब्द का अर्थ है—शत्रुओं का नाश करने वाला। जिस साधक ने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि आत्म-शत्रुओं का नाश कर दिया है, वही अरिहन्त है। जैन साधक अपने आदर्श के रूप में ऐसे व्यक्तित्व को रखता है जिसने आत्मा की सभी दुर्बलताओं का अन्त कर दिया है। 'अरिहन्त' शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति 'अर्हत्' के रूप में की जाती है। इसका अर्थ है योग्य / जो जीव आत्मविकास करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, मुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, वह अर्हत् है / जैनदर्शन के अनुसार आत्मा में अनन्त ज्ञान है, अनन्त दर्शन है, अनन्त सुख है और अनन्त वीर्य है। कर्मों के आवरण के कारण आत्मा की ये शक्तियां दबी हुई हैं। अर्हत् अवस्था में वे पूर्णतया प्रकट हो जाती हैं। इस शब्द की तीसरी व्युत्पत्ति संस्कृत की ‘अर्ह पूजायां' धातु से की जाती है, अर्थात् जो व्यक्ति पूजा के योग्य है वह अर्हत् है। यहां एक बात उल्लेखनीय है। जैन धर्म, देवतत्त्व के रूप में किसी व्यक्ति-विशेष को स्वीकार नहीं करता। जिस आत्मा ने पूर्ण विकास कर लिया वह चाहे कोई हो, अरिहन्त है और देव के रूप में वन्दनीय है। यद्यपि जैन परम्परा इतिहास के रूप में चौबीस तीर्थंकरों तथा दूसरे महापुरुषों को मानती है। उन्हें वन्दना भी करती है किन्तु इसलिए कि उन्होंने आत्मा का पूर्ण विकास कर लिया है। उसमें गुणों का महत्व है. व्यक्ति का नहीं। प्रत्येक नए काल के साथ नए तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं. नए यगप्रवर्तक होते हैं, नए वन्दनीय होते हैं। पुराने मोक्ष चले जाते हैं, फिर वापिस नहीं लौटते / धीरे-धीरे उनकी स्मृति भी काल के गर्भ में विलीन हो जाती है। नए युग की जनता नए तीर्थंकरों की वंदना करती है। पुरानों को भूल जाती है। अरिहन्त न तो ईश्वर के अवतार हैं, न ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, न ईश्वर के अंश हैं। वे वह आत्माएं हैं जिन्होंने अपने आप में सोए हुए ईश्वरत्व को प्रकट कर लिया है। जो अपनी तपस्या तथा परिश्रम के द्वारा जीवात्मा से परमात्मा बने हैं। जैन धर्म उन्हीं को देव के रूप में मानता है। गुरु देवतत्त्व के बाद दूसरा क्रम गुरुतत्त्व का आता है। प्रत्येक जैन यह प्रतिज्ञा करता है कि साधु मेरे गुरु हैं। साधु का अर्थ है, पांच महाव्रतों की साधना करने वाला। वे महाव्रत निम्नलिखित हैं श्री उपासक दशांग सूत्रम् / 42 / प्रस्तावना