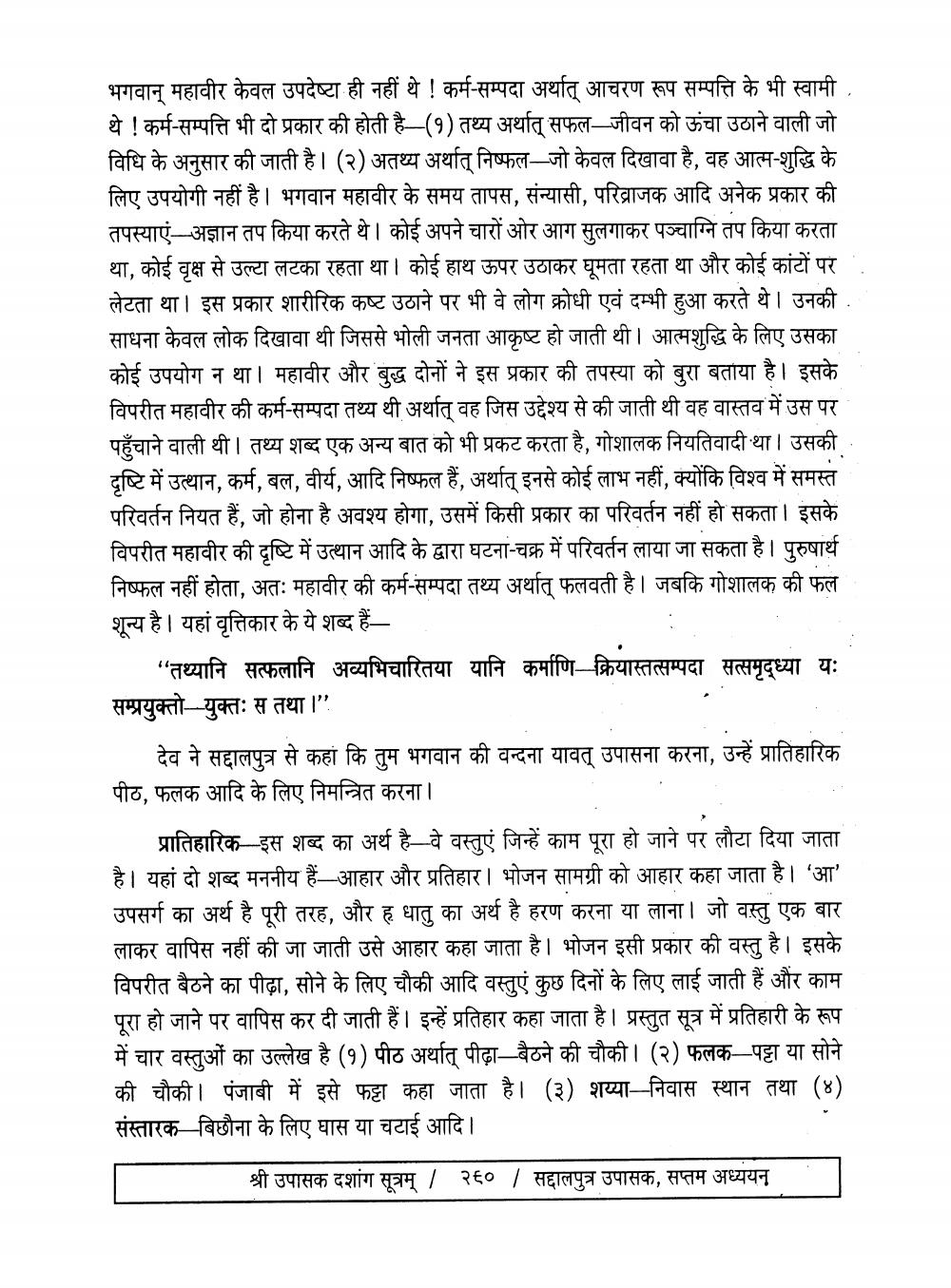________________ भगवान् महावीर केवल उपदेष्टा ही नहीं थे ! कर्म-सम्पदा अर्थात् आचरण रूप सम्पत्ति के भी स्वामी थे ! कर्म-सम्पत्ति भी दो प्रकार की होती है—(१) तथ्य अर्थात् सफल जीवन को ऊंचा उठाने वाली जो विधि के अनुसार की जाती है। (2) अतथ्य अर्थात् निष्फल जो केवल दिखावा है, वह आत्म-शुद्धि के लिए उपयोगी नहीं है। भगवान महावीर के समय तापस, संन्यासी, परिव्राजक आदि अनेक प्रकार की तपस्याएं—अज्ञान तप किया करते थे। कोई अपने चारों ओर आग सुलगाकर पञ्चाग्नि तप किया करता था, कोई वृक्ष से उल्टा लटका रहता था। कोई हाथ ऊपर उठाकर घूमता रहता था और कोई कांटों पर लेटता था। इस प्रकार शारीरिक कष्ट उठाने पर भी वे लोग क्रोधी एवं दम्भी हुआ करते थे। उनकी साधना केवल लोक दिखावा थी जिससे भोली जनता आकृष्ट हो जाती थी। आत्मशुद्धि के लिए उसका कोई उपयोग न था। महावीर और बद्ध दोनों ने इस प्रकार की तपस्या को बुरा बताया है। इसके विपरीत महावीर की कर्म-सम्पदा तथ्य थी अर्थात् वह जिस उद्देश्य से की जाती थी वह वास्तव में उस पर पहुँचाने वाली थी। तथ्य शब्द एक अन्य बात को भी प्रकट करता है, गोशालक नियतिवादी था। उसकी दृष्टि में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, आदि निष्फल हैं, अर्थात् इनसे कोई लाभ नहीं, क्योंकि विश्व में समस्त परिवर्तन नियत हैं, जो होना है अवश्य होगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके विपरीत महावीर की दृष्टि में उत्थान आदि के द्वारा घटना-चक्र में परिवर्तन लाया जा सकता है। पुरुषार्थ निष्फल नहीं होता, अतः महावीर की कर्म-सम्पदा तथ्य अर्थात् फलवती है। जबकि गोशालक की फल शून्य है। यहां वृत्तिकार के ये शब्द हैं "तथ्यानि सत्फलानि अव्यभिचारितया यानि कर्माणि क्रियास्तत्सम्पदा सत्समृद्ध्या यः सम्प्रयुक्तो—युक्तः स तथा / " ___देव ने सद्दालपुत्र से कहा कि तुम भगवान की वन्दना यावत् उपासना करना, उन्हें प्रातिहारिक पीठ, फलक आदि के लिए निमन्त्रित करना / प्रातिहारिक इस शब्द का अर्थ है—वे वस्तुएं जिन्हें काम पूरा हो जाने पर लौटा दिया जाता है। यहां दो शब्द मननीय हैं—आहार और प्रतिहार / भोजन सामग्री को आहार कहा जाता है। 'आ' उपसर्ग का अर्थ है पूरी तरह, और ह धातु का अर्थ है हरण करना या लाना। जो वस्तु एक बार लाकर वापिस नहीं की जा जाती उसे आहार कहा जाता है। भोजन इसी प्रकार की वस्तु है। इसके विपरीत बैठने का पीढ़ा, सोने के लिए चौकी आदि वस्तुएं कुछ दिनों के लिए लाई जाती हैं और काम पूरा हो जाने पर वापिस कर दी जाती हैं। इन्हें प्रतिहार कहा जाता है। प्रस्तुत सूत्र में प्रतिहारी के रूप में चार वस्तुओं का उल्लेख है (1) पीठ अर्थात् पीढ़ा बैठने की चौकी। (2) फलक—पट्टा या सोने की चौकी। पंजाबी में इसे फट्टा कहा जाता है। (3) शय्या निवास स्थान तथा (4) संस्तारक बिछौना के लिए घास या चटाई आदि। श्री उपासक दशांग सूत्रम् / 260 / सद्दालपुत्र उपासक, सप्तम अध्ययन |