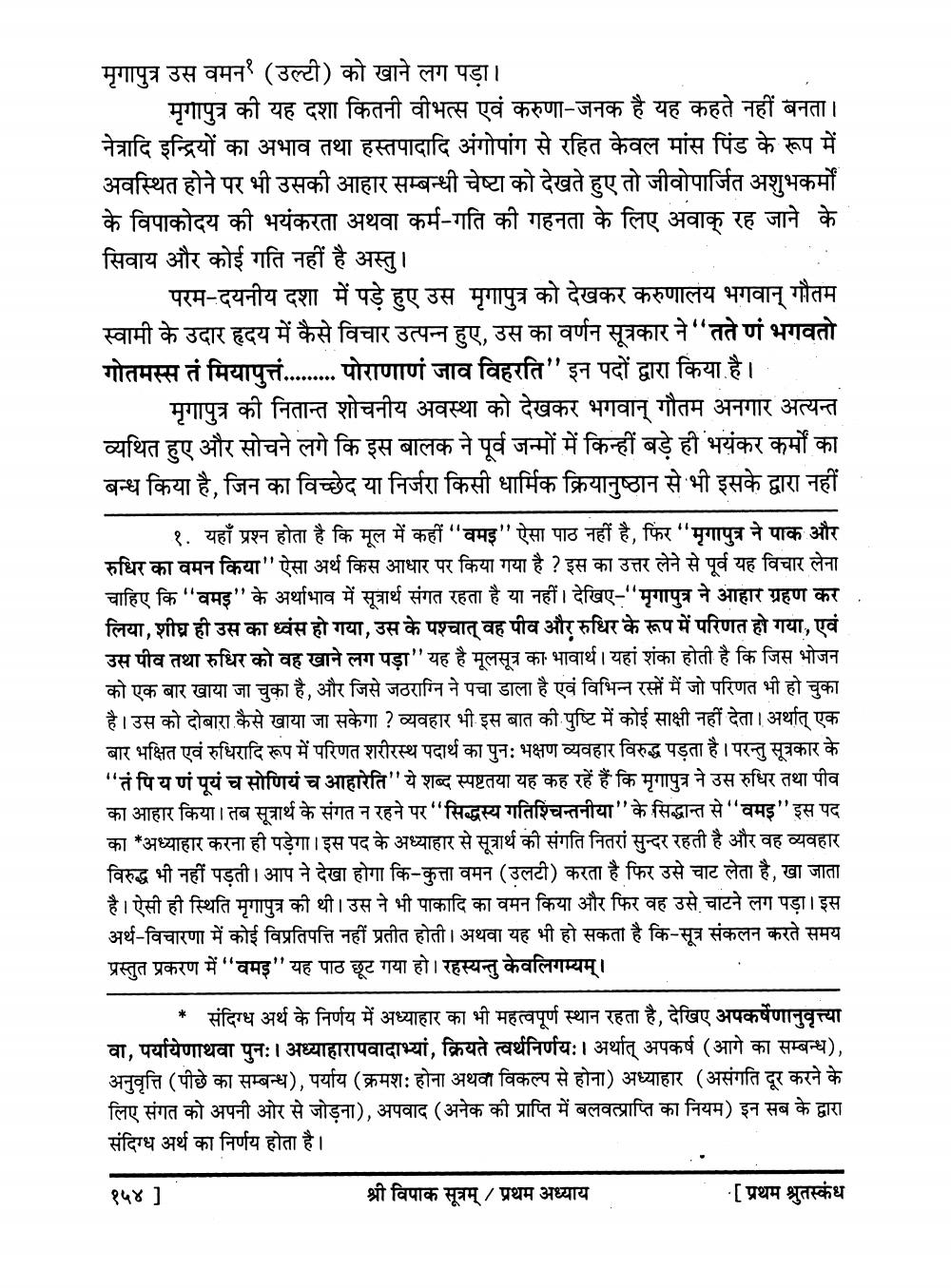________________ मृगापुत्र उस वमन (उल्टी) को खाने लग पड़ा। मृगापुत्र की यह दशा कितनी वीभत्स एवं करुणा-जनक है यह कहते नहीं बनता। नेत्रादि इन्द्रियों का अभाव तथा हस्तपादादि अंगोपांग से रहित केवल मांस पिंड के रूप में अवस्थित होने पर भी उसकी आहार सम्बन्धी चेष्टा को देखते हुए तो जीवोपार्जित अशुभकर्मों के विपाकोदय की भयंकरता अथवा कर्म-गति की गहनता के लिए अवाक् रह जाने के सिवाय और कोई गति नहीं है अस्तु / परम-दयनीय दशा में पड़े हुए उस मृगापुत्र को देखकर करुणालय भगवान् गौतम स्वामी के उदार हृदय में कैसे विचार उत्पन्न हुए, उस का वर्णन सूत्रकार ने "तते णं भगवतो गोतमस्स तं मियापुत्तं........ पोराणाणं जाव विहरति" इन पदों द्वारा किया है। ___मृगापुत्र की नितान्त शोचनीय अवस्था को देखकर भगवान् गौतम अनगार अत्यन्त व्यथित हुए और सोचने लगे कि इस बालक ने पूर्व जन्मों में किन्हीं बड़े ही भयंकर कर्मों का बन्ध किया है, जिन का विच्छेद या निर्जरा किसी धार्मिक क्रियानुष्ठान से भी इसके द्वारा नहीं 1. यहाँ प्रश्न होता है कि मूल में कहीं "वमइ" ऐसा पाठ नहीं है, फिर "मृगापुत्र ने पाक और रुधिर का वमन किया" ऐसा अर्थ किस आधार पर किया गया है ? इस का उत्तर लेने से पूर्व यह विचार लेना चाहिए कि "वमइ" के अभाव में सूत्रार्थ संगत रहता है या नहीं। देखिए-"मृगापुत्र ने आहार ग्रहण कर लिया, शीघ्र ही उस का ध्वंस हो गया, उस के पश्चात् वह पीव और रुधिर के रूप में परिणत हो गया, एवं उस पीव तथा रुधिर को वह खाने लग पड़ा" यह है मूलसूत्र का भावार्थ / यहां शंका होती है कि जिस भोजन को एक बार खाया जा चुका है, और जिसे जठराग्नि ने पचा डाला है एवं विभिन्न रसों में जो परिणत भी हो चुका है। उस को दोबारा कैसे खाया जा सकेगा? व्यवहार भी इस बात की पुष्टि में कोई साक्षी नहीं देता। अर्थात् एक बार भक्षित एवं रुधिरादि रूप में परिणत शरीरस्थ पदार्थ का पुनः भक्षण व्यवहार विरुद्ध पड़ता है। परन्तु सूत्रकार के "तं पि य णं पूयं च सोणियं च आहारेति" ये शब्द स्पष्टतया यह कह रहें हैं कि मृगापुत्र ने उस रुधिर तथा पीव का आहार किया। तब सूत्रार्थ के संगत न रहने पर "सिद्धस्य गतिश्चिन्तनीया" के सिद्धान्त से "वमइ" इस पद का *अध्याहार करना ही पड़ेगा। इस पद के अध्याहार से सूत्रार्थ की संगति नितरां सुन्दर रहती है और वह व्यवहार विरुद्ध भी नहीं पड़ती। आप ने देखा होगा कि-कुत्ता वमन (उलटी) करता है फिर उसे चाट लेता है, खा जाता है। ऐसी ही स्थिति मृगापुत्र की थी। उस ने भी पाकादि का वमन किया और फिर वह उसे चाटने लग पड़ा। इस अर्थ-विचारणा में कोई विप्रतिपत्ति नहीं प्रतीत होती। अथवा यह भी हो सकता है कि-सूत्र संकलन करते समय प्रस्तुत प्रकरण में "वमइ" यह पाठ छूट गया हो। रहस्यन्तु केवलिगम्यम्। * संदिग्ध अर्थ के निर्णय में अध्याहार का भी महत्वपूर्ण स्थान रहता है, देखिए अपकर्षणानुवृत्त्या वा, पर्यायेणाथवा पुनः। अध्याहारापवादाभ्यां, क्रियते त्वर्थनिर्णयः। अर्थात् अपकर्ष (आगे का सम्बन्ध), अनुवृत्ति (पीछे का सम्बन्ध), पर्याय (क्रमशः होना अथवा विकल्प से होना) अध्याहार (असंगति दूर करने के लिए संगत को अपनी ओर से जोड़ना), अपवाद (अनेक की प्राप्ति में बलवत्प्राप्ति का नियम) इन सब के द्वारा संदिग्ध अर्थ का निर्णय होता है। 154 ] श्री विपाक सूत्रम् / प्रथम अध्याय [प्रथम श्रुतस्कंध