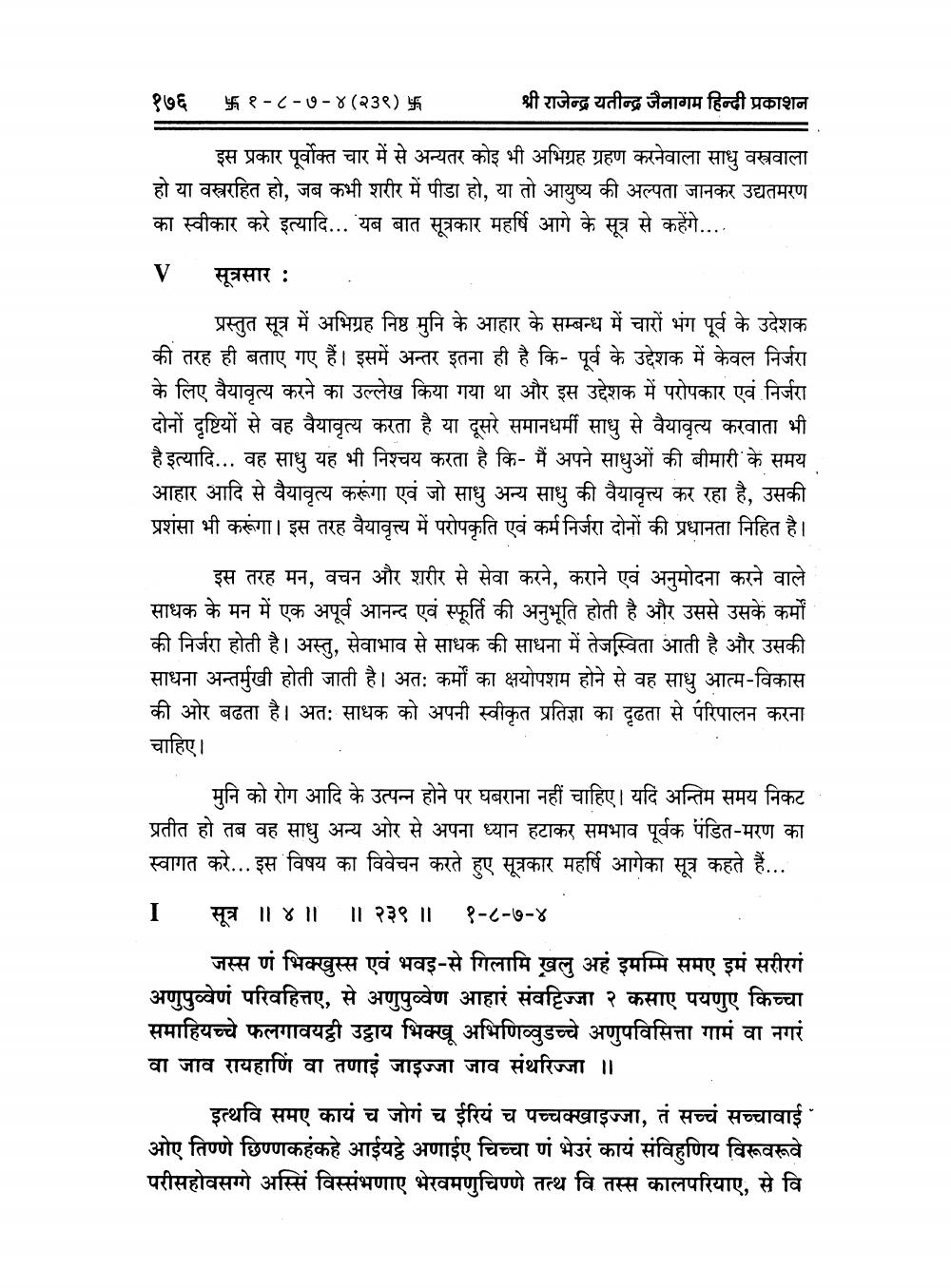________________ 176 // 1-8-7-4 (२३९)卐 श्री राजेन्द्र यतीन्द्र जैनागम हिन्दी प्रकाशन इस प्रकार पूर्वोक्त चार में से अन्यतर कोइ भी अभिग्रह ग्रहण करनेवाला साधु वस्त्रवाला हो या वस्त्ररहित हो, जब कभी शरीर में पीडा हो, या तो आयुष्य की अल्पता जानकर उद्यतमरण का स्वीकार करे इत्यादि... यब बात सूत्रकार महर्षि आगे के सूत्र से कहेंगे... v सूत्रसार : प्रस्तुत सूत्र में अभिग्रह निष्ठ मुनि के आहार के सम्बन्ध में चारों भंग पूर्व के उदेशक की तरह ही बताए गए हैं। इसमें अन्तर इतना ही है कि- पूर्व के उद्देशक में केवल निर्जरा के लिए वैयावृत्य करने का उल्लेख किया गया था और इस उद्देशक में परोपकार एवं निर्जरा दोनों दृष्टियों से वह वैयावृत्य करता है या दूसरे समानधर्मी साधु से वैयावृत्य करवाता भी है इत्यादि... वह साधु यह भी निश्चय करता है कि- मैं अपने साधुओं की बीमारी के समय आहार आदि से वैयावृत्य करूंगा एवं जो साधु अन्य साधु की वैयावृत्त्य कर रहा है, उसकी प्रशंसा भी करूंगा। इस तरह वैयावृत्त्य में परोपकृति एवं कर्म निर्जरा दोनों की प्रधानता निहित है। __ इस तरह मन, वचन और शरीर से सेवा करने, कराने एवं अनुमोदना करने वाले साधक के मन में एक अपूर्व आनन्द एवं स्फूर्ति की अनुभूति होती है और उससे उसके कर्मों की निर्जरा होती है। अस्तु, सेवाभाव से साधक की साधना में तेजस्विता आती है और उसकी साधना अन्तर्मुखी होती जाती है। अतः कर्मों का क्षयोपशम होने से वह साधु आत्म-विकास की ओर बढ़ता है। अतः साधक को अपनी स्वीकृत प्रतिज्ञा का दृढता से परिपालन करना चाहिए। मुनि को रोग आदि के उत्पन्न होने पर घबराना नहीं चाहिए। यदि अन्तिम समय निकट प्रतीत हो तब वह साधु अन्य ओर से अपना ध्यान हटाकर समभाव पूर्वक पंडित-मरण का स्वागत करे... इस विषय का विवेचन करते हुए सूत्रकार महर्षि आगेका सूत्र कहते हैं... I सूत्र // 4 // // 239 // 1-8-7-4 जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ-से गिलामि खलु अहं इमम्मि समए इमं सरीरगं अणुपुव्वेणं परिवहित्तए, से अणुपुव्वेण आहारं संवट्टिज्जा 2 कसाए पयणुए किच्चा समाहियच्चे फलगावयट्ठी उट्ठाय भिक्खू अभिणिव्वुडच्चे अणुपविसित्ता गामं वा नगरं वा जाव रायहाणिं वा तणाई जाइज्जा जाव संथरिज्जा // इत्थवि समए कायं च जोगं च ईरियं च पच्चक्खाइज्जा, तं सच्चं सच्चावाई ओए तिण्णे छिण्णकहकहे आईयढे अणाईए चिच्चा णं भेउरं कायं संविहुणिय विरूवरूवे परीसहोवसग्गे अस्सिं विस्संभणाए भेरवमणुचिण्णे तत्थ वि तस्स कालपरियाए, से वि