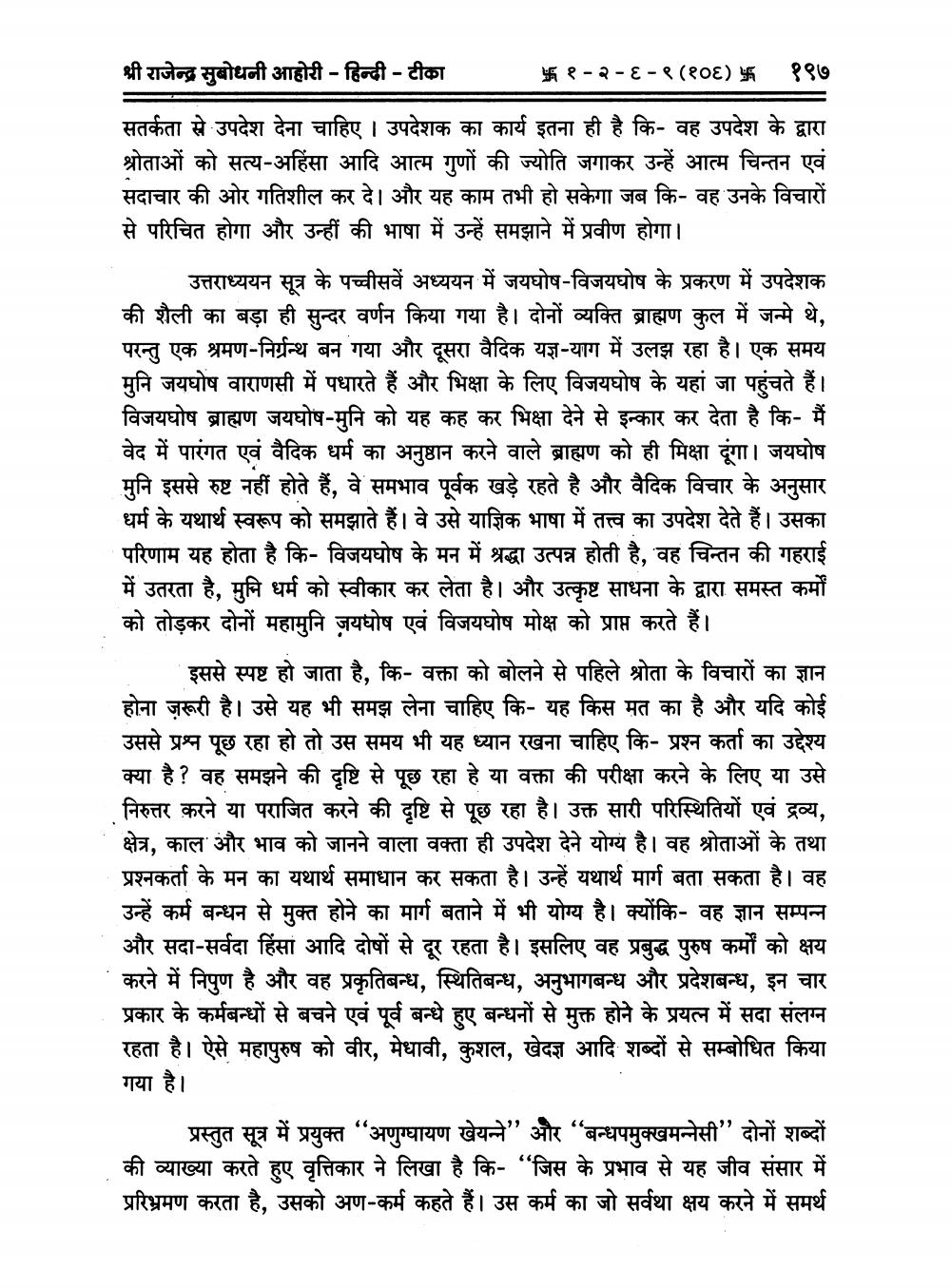________________ श्री राजेन्द्र सुबोधनी आहोरी - हिन्दी - टीका // 1-2-6-9 (108) 197 सतर्कता से उपदेश देना चाहिए / उपदेशक का कार्य इतना ही है कि- वह उपदेश के द्वारा श्रोताओं को सत्य-अहिंसा आदि आत्म गुणों की ज्योति जगाकर उन्हें आत्म चिन्तन एवं सदाचार की ओर गतिशील कर दे। और यह काम तभी हो सकेगा जब कि- वह उनके विचारों से परिचित होगा और उन्हीं की भाषा में उन्हें समझाने में प्रवीण होगा। उत्तराध्ययन सूत्र के पच्चीसवें अध्ययन में जयघोष-विजयघोष के प्रकरण में उपदेशक की शैली का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है। दोनों व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, परन्तु एक श्रमण-निर्ग्रन्थ बन गया और दूसरा वैदिक यज्ञ-याग में उलझ रहा है। एक समय मुनि जयघोष वाराणसी में पधारते हैं और भिक्षा के लिए विजयघोष के यहां जा पहुंचते हैं। विजयघोष ब्राह्मण जयघोष-मुनि को यह कह कर भिक्षा देने से इन्कार कर देता है कि- मैं वेद में पारंगत एवं वैदिक धर्म का अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण को ही मिक्षा दूंगा। जयघोष मुनि इससे रुष्ट नहीं होते हैं, वे समभाव पूर्वक खड़े रहते है और वैदिक विचार के अनुसार धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझाते हैं। वे उसे याज्ञिक भाषा में तत्त्व का उपदेश देते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि- विजयघोष के मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह चिन्तन की गहराई में उतरता है, मुनि धर्म को स्वीकार कर लेता है। और उत्कृष्ट साधना के द्वारा समस्त कर्मों को तोड़कर दोनों महामुनि जयघोष एवं विजयघोष मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है, कि- वक्ता को बोलने से पहिले श्रोता के विचारों का ज्ञान होना ज़रूरी है। उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि- यह किस मत का है और यदि कोई उससे प्रश्न पूछ रहा हो तो उस समय भी यह ध्यान रखना चाहिए कि- प्रश्न कर्ता का उद्देश्य क्या है ? वह समझने की दृष्टि से पूछ रहा हे या वक्ता की परीक्षा करने के लिए या उसे निरुत्तर करने या पराजित करने की दृष्टि से पूछ रहा है। उक्त सारी परिस्थितियों एवं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को जानने वाला वक्ता ही उपदेश देने योग्य है। वह श्रोताओं के तथा प्रश्नकर्ता के मन का यथार्थ समाधान कर सकता है। उन्हें यथार्थ मार्ग बता सकता है। वह उन्हें कर्म बन्धन से मुक्त होने का मार्ग बताने में भी योग्य है। क्योंकि- वह ज्ञान सम्पन्न और सदा-सर्वदा हिंसा आदि दोषों से दूर रहता है। इसलिए वह प्रबुद्ध पुरुष कर्मों को क्षय करने में निपुण है और वह प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध, इन चार प्रकार के कर्मबन्धों से बचने एवं पूर्व बन्धे हुए बन्धनों से मुक्त होने के प्रयत्न में सदा संलग्न रहता है। ऐसे महापुरुष को वीर, मेधावी, कुशल, खेदज्ञ आदि शब्दों से सम्बोधित किया गया है। प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त “अणुग्घायण खेयन्ने” और “बन्धपमुक्खमन्नेसी" दोनों शब्दों की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है कि- “जिस के प्रभाव से यह जीव संसार में प्ररिभ्रमण करता है, उसको अण-कर्म कहते हैं। उस कर्म का जो सर्वथा क्षय करने में समर्थ