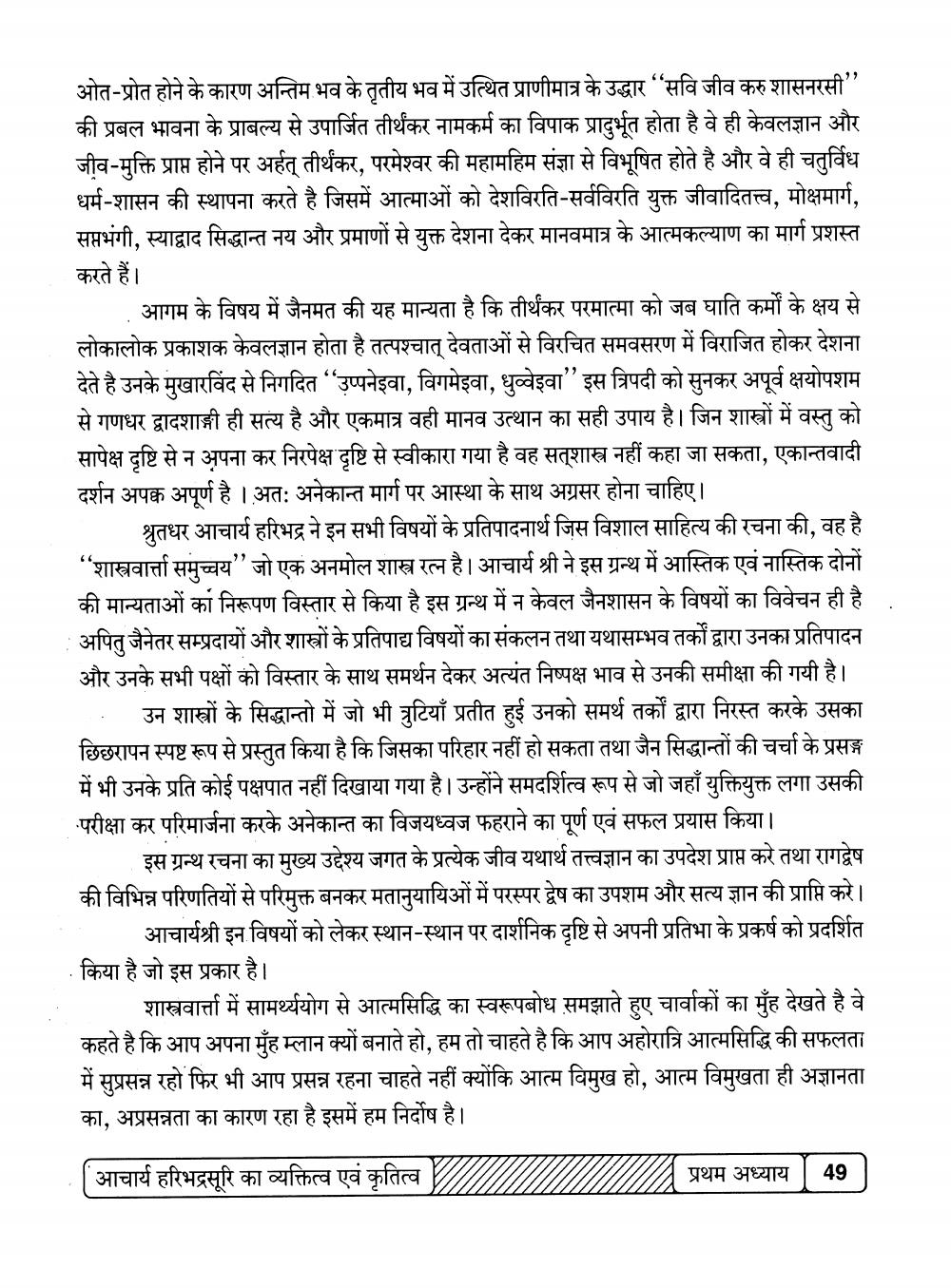________________ ओत-प्रोत होने के कारण अन्तिम भव के तृतीय भव में उत्थित प्राणीमात्र के उद्धार “सवि जीव करु शासनरसी' की प्रबल भावना के प्राबल्य से उपार्जित तीर्थंकर नामकर्म का विपाक प्रादुर्भूत होता है वे ही केवलज्ञान और जीव-मुक्ति प्राप्त होने पर अर्हत् तीर्थंकर, परमेश्वर की महामहिम संज्ञा से विभूषित होते है और वे ही चतुर्विध धर्म-शासन की स्थापना करते है जिसमें आत्माओं को देशविरति-सर्वविरति युक्त जीवादितत्त्व, मोक्षमार्ग, सप्तभंगी, स्याद्वाद सिद्धान्त नय और प्रमाणों से युक्त देशना देकर मानवमात्र के आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। . आगम के विषय में जैनमत की यह मान्यता है कि तीर्थंकर परमात्मा को जब घाति कर्मों के क्षय से लोकालोक प्रकाशक केवलज्ञान होता है तत्पश्चात् देवताओं से विरचित समवसरण में विराजित होकर देशना देते है उनके मुखारविंद से निगदित “उप्पनेइवा, विगमेइवा, धुव्वेइवा” इस त्रिपदी को सुनकर अपूर्व क्षयोपशम से गणधर द्वादशाङ्गी ही सत्य है और एकमात्र वही मानव उत्थान का सही उपाय है। जिन शास्त्रों में वस्तु को सापेक्ष दृष्टि से न अपना कर निरपेक्ष दृष्टि से स्वीकारा गया है वह सत्शास्त्र नहीं कहा जा सकता, एकान्तवादी दर्शन अपक्व अपूर्ण है / अत: अनेकान्त मार्ग पर आस्था के साथ अग्रसर होना चाहिए। श्रुतधर आचार्य हरिभद्र ने इन सभी विषयों के प्रतिपादनार्थ जिस विशाल साहित्य की रचना की, वह है “शास्त्रवार्ता समुच्चय' जो एक अनमोल शास्त्र रत्न है। आचार्य श्री ने इस ग्रन्थ में आस्तिक एवं नास्तिक दोनों की मान्यताओं का निरूपण विस्तार से किया है इस ग्रन्थ में न केवल जैनशासन के विषयों का विवेचन ही है अपितु जैनेतर सम्प्रदायों और शास्त्रों के प्रतिपाद्य विषयों का संकलन तथा यथासम्भव तर्कों द्वारा उनका प्रतिपादन और उनके सभी पक्षों को विस्तार के साथ समर्थन देकर अत्यंत निष्पक्ष भाव से उनकी समीक्षा की गयी है। . उन शास्त्रों के सिद्धान्तो में जो भी त्रुटियाँ प्रतीत हुई उनको समर्थ तर्कों द्वारा निरस्त करके उसका छिछरापन स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है कि जिसका परिहार नहीं हो सकता तथा जैन सिद्धान्तों की चर्चा के प्रसङ्ग में भी उनके प्रति कोई पक्षपात नहीं दिखाया गया है। उन्होंने समदर्शित्व रूप से जो जहाँ युक्तियुक्त लगा उसकी परीक्षा कर परिमार्जना करके अनेकान्त का विजयध्वज फहराने का पूर्ण एवं सफल प्रयास किया। __ इस ग्रन्थ रचना का मुख्य उद्देश्य जगत के प्रत्येक जीव यथार्थ तत्त्वज्ञान का उपदेश प्राप्त करे तथा रागद्वेष की विभिन्न परिणतियों से परिमुक्त बनकर मतानुयायिओं में परस्पर द्वेष का उपशम और सत्य ज्ञान की प्राप्ति करे। आचार्यश्री इन विषयों को लेकर स्थान-स्थान पर दार्शनिक दृष्टि से अपनी प्रतिभा के प्रकर्ष को प्रदर्शित किया है जो इस प्रकार है। शास्त्रवार्ता में सामर्थ्ययोग से आत्मसिद्धि का स्वरूपबोध समझाते हुए चार्वाकों का मुँह देखते है वे कहते है कि आप अपना मुँह म्लान क्यों बनाते हो, हम तो चाहते है कि आप अहोरात्रि आत्मसिद्धि की सफलता में सुप्रसन्न रहो फिर भी आप प्रसन्न रहना चाहते नहीं क्योंकि आत्म विमुख हो, आत्म विमुखता ही अज्ञानता का, अप्रसन्नता का कारण रहा है इसमें हम निर्दोष है। [ आचार्य हरिभद्रसूरि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व VII I प्रथम अध्याय | 49 )