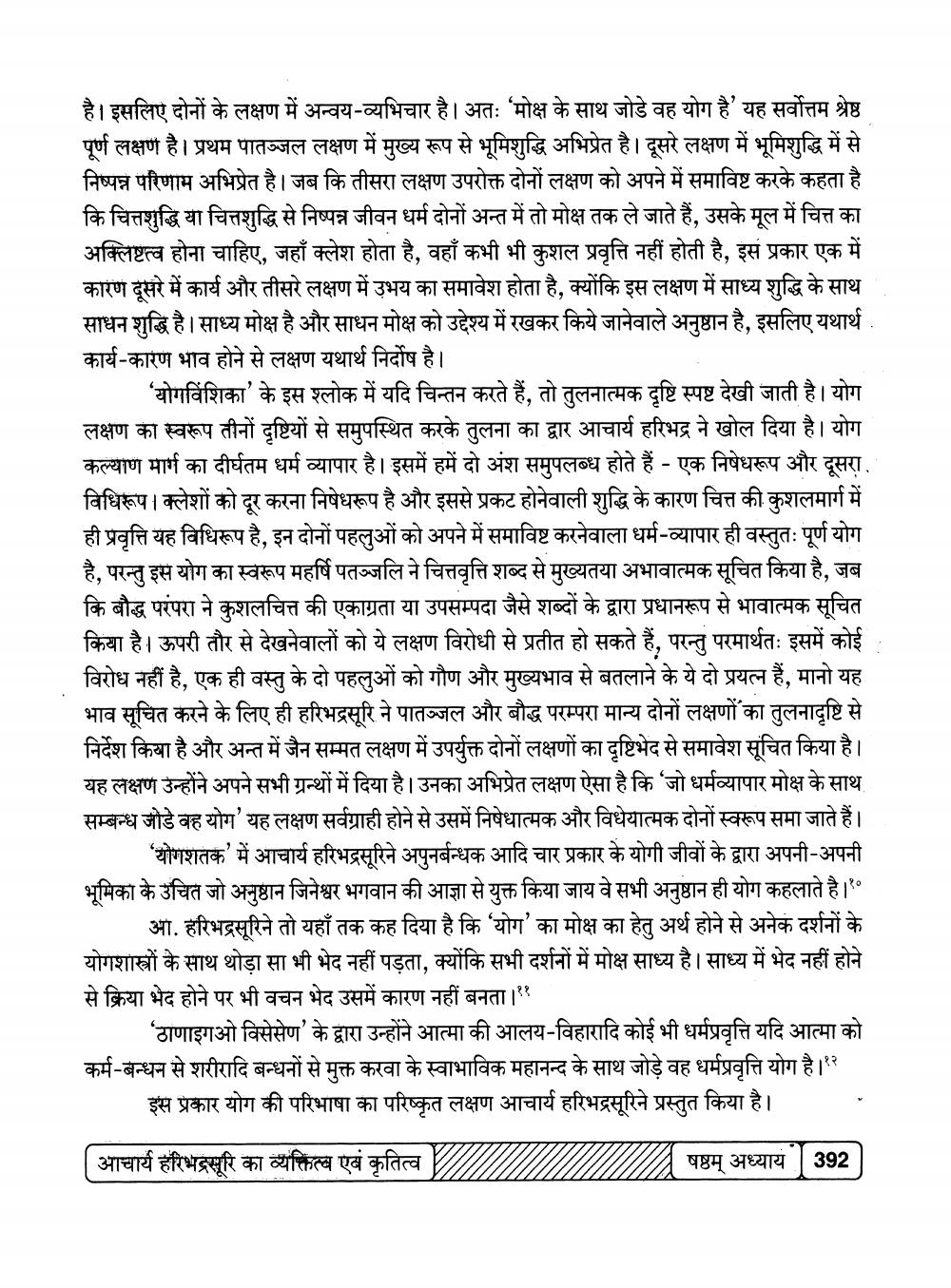________________ है। इसलिए दोनों के लक्षण में अन्वय-व्यभिचार है। अतः ‘मोक्ष के साथ जोडे वह योग है' यह सर्वोत्तम श्रेष्ठ पूर्ण लक्षण है। प्रथम पातञ्जल लक्षण में मुख्य रूप से भूमिशुद्धि अभिप्रेत है। दूसरे लक्षण में भूमिशुद्धि में से निष्पन्न परिणाम अभिप्रेत है। जब कि तीसरा लक्षण उपरोक्त दोनों लक्षण को अपने में समाविष्ट करके कहता है कि चित्तशुद्धि या चित्तशुद्धि से निष्पन्न जीवन धर्म दोनों अन्त में तो मोक्ष तक ले जाते हैं, उसके मूल में चित्त का अक्लिष्टत्व होना चाहिए, जहाँ क्लेश होता है, वहाँ कभी भी कुशल प्रवृत्ति नहीं होती है, इस प्रकार एक में कारण दूसरे में कार्य और तीसरे लक्षण में उभय का समावेश होता है, क्योंकि इस लक्षण में साध्य शुद्धि के साथ साधन शुद्धि है। साध्य मोक्ष है और साधन मोक्ष को उद्देश्य में रखकर किये जानेवाले अनुष्ठान है, इसलिए यथार्थ कार्य-कारण भाव होने से लक्षण यथार्थ निर्दोष है। 'योगविंशिका' के इस श्लोक में यदि चिन्तन करते हैं, तो तुलनात्मक दृष्टि स्पष्ट देखी जाती है। योग लक्षण का स्वरूप तीनों दृष्टियों से समुपस्थित करके तुलना का द्वार आचार्य हरिभद्र ने खोल दिया है। योग कल्याण मार्ग का दीर्घतम धर्म व्यापार है। इसमें हमें दो अंश समुपलब्ध होते हैं - एक निषेधरूप और दूसरा. विधिरूप। क्लेशों को दूर करना निषेधरूप है और इससे प्रकट होनेवाली शुद्धि के कारण चित्त की कुशलमार्ग में ही प्रवृत्ति यह विधिरूप है, इन दोनों पहलुओं को अपने में समाविष्ट करनेवाला धर्म-व्यापार ही वस्तुतः पूर्ण योग है, परन्तु इस योग का स्वरूप महर्षि पतञ्जलि ने चित्तवृत्ति शब्द से मुख्यतया अभावात्मक सूचित किया है, जब कि बौद्ध परंपरा ने कुशलचित्त की एकाग्रता या उपसम्पदा जैसे शब्दों के द्वारा प्रधानरूप से भावात्मक सूचित किया है। ऊपरी तौर से देखनेवालों को ये लक्षण विरोधी से प्रतीत हो सकते हैं, परन्तु परमार्थतः इसमें कोई विरोध नहीं है, एक ही वस्तु के दो पहलुओं को गौण और मुख्यभाव से बतलाने के ये दो प्रयत्न हैं, मानो यह भाव सूचित करने के लिए ही हरिभद्रसूरि ने पातञ्जल और बौद्ध परम्परा मान्य दोनों लक्षणों का तुलनादृष्टि से निर्देश किया है और अन्त में जैन सम्मत लक्षण में उपर्युक्त दोनों लक्षणों का दृष्टिभेद से समावेश सूचित किया है। यह लक्षण उन्होंने अपने सभी ग्रन्थों में दिया है। उनका अभिप्रेत लक्षण ऐसा है कि जो धर्मव्यापार मोक्ष के साथ सम्बन्ध जोडे वह योग' यह लक्षण सर्वग्राही होने से उसमें निषेधात्मक और विधेयात्मक दोनों स्वरूप समा जाते हैं। 'योगशतक' में आचार्य हरिभद्रसूरिने अपुनर्बन्धक आदि चार प्रकार के योगी जीवों के द्वारा अपनी-अपनी भूमिका के उचित जो अनुष्ठान जिनेश्वर भगवान की आज्ञा से युक्त किया जाय वे सभी अनुष्ठान ही योग कहलाते है। ___आ. हरिभद्रसूरिने तो यहाँ तक कह दिया है कि 'योग' का मोक्ष का हेतु अर्थ होने से अनेक दर्शनों के योगशास्त्रों के साथ थोड़ा सा भी भेद नहीं पड़ता, क्योंकि सभी दर्शनों में मोक्ष साध्य है। साध्य में भेद नहीं होने से क्रिया भेद होने पर भी वचन भेद उसमें कारण नहीं बनता।११ 'ठाणाइगओ विसेसेण' के द्वारा उन्होंने आत्मा की आलय-विहारादि कोई भी धर्मप्रवृत्ति यदि आत्मा को कर्म-बन्धन से शरीरादि बन्धनों से मुक्त करवा के स्वाभाविक महानन्द के साथ जोड़े वह धर्मप्रवृत्ति योग है।१२ / इस प्रकार योग की परिभाषा का परिष्कृत लक्षण आचार्य हरिभद्रसूरिने प्रस्तुत किया है। आचार्य हरिभद्रसूरि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIA षष्ठम् अध्याय | 392 |