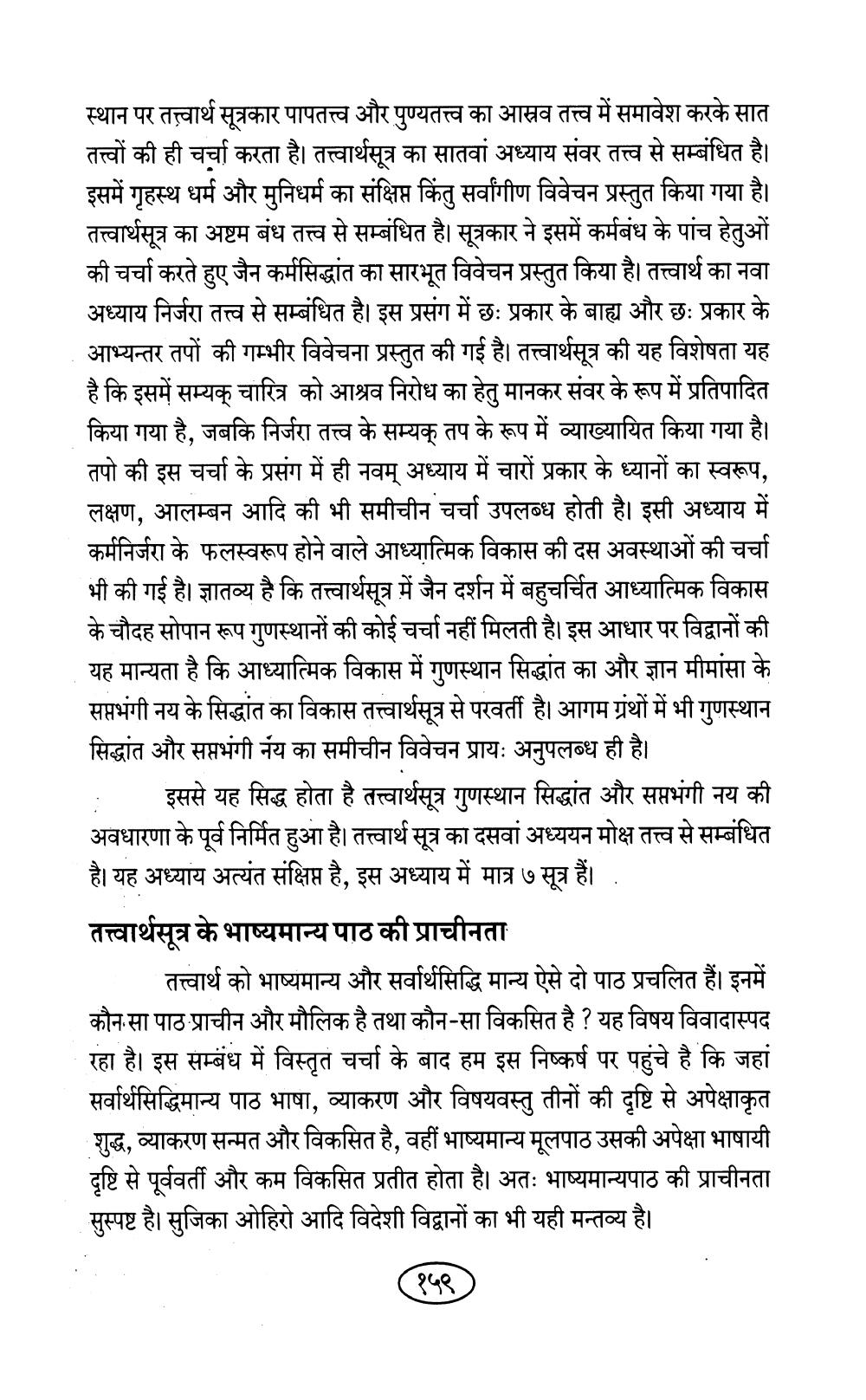________________ स्थान पर तत्त्वार्थ सूत्रकार पापतत्त्व और पुण्यतत्त्व का आस्रव तत्त्व में समावेश करके सात तत्त्वों की ही चर्चा करता है। तत्त्वार्थसूत्र का सातवां अध्याय संवर तत्त्व से सम्बंधित है। इसमें गृहस्थ धर्म और मुनिधर्म का संक्षिप्त किंतु सर्वांगीण विवेचन प्रस्तुत किया गया है। तत्त्वार्थसूत्र का अष्टम बंध तत्त्व से सम्बंधित है। सूत्रकार ने इसमें कर्मबंध के पांच हेतुओं की चर्चा करते हुए जैन कर्मसिद्धांत का सारभूत विवेचन प्रस्तुत किया है। तत्त्वार्थ का नवा अध्याय निर्जरा तत्त्व से सम्बंधित है। इस प्रसंग में छः प्रकार के बाह्य और छः प्रकार के आभ्यन्तर तपों की गम्भीर विवेचना प्रस्तुत की गई है। तत्त्वार्थसूत्र की यह विशेषता यह है कि इसमें सम्यक् चारित्र को आश्रव निरोध का हेतु मानकर संवर के रूप में प्रतिपादित किया गया है, जबकि निर्जरा तत्त्व के सम्यक् तप के रूप में व्याख्यायित किया गया है। तपो की इस चर्चा के प्रसंग में ही नवम् अध्याय में चारों प्रकार के ध्यानों का स्वरूप, लक्षण, आलम्बन आदि की भी समीचीन चर्चा उपलब्ध होती है। इसी अध्याय में कर्मनिर्जरा के फलस्वरूप होने वाले आध्यात्मिक विकास की दस अवस्थाओं की चर्चा भी की गई है। ज्ञातव्य है कि तत्त्वार्थसूत्र में जैन दर्शन में बहुचर्चित आध्यात्मिक विकास के चौदह सोपान रूप गुणस्थानों की कोई चर्चा नहीं मिलती है। इस आधार पर विद्वानों की यह मान्यता है कि आध्यात्मिक विकास में गुणस्थान सिद्धांत का और ज्ञान मीमांसा के सप्तभंगी नय के सिद्धांत का विकास तत्त्वार्थसूत्र से परवर्ती है। आगम ग्रंथों में भी गुणस्थान सिद्धांत और सप्तभंगी नंय का समीचीन विवेचन प्रायः अनुपलब्ध ही है। . इससे यह सिद्ध होता है तत्त्वार्थसूत्र गुणस्थान सिद्धांत और सप्तभंगी नय की अवधारणा के पूर्व निर्मित हुआ है। तत्त्वार्थ सूत्र का दसवां अध्ययन मोक्ष तत्त्व से सम्बंधित है। यह अध्याय अत्यंत संक्षिप्त है, इस अध्याय में मात्र 7 सूत्र हैं। . तत्त्वार्थसूत्र के भाष्यमान्य पाठ की प्राचीनता तत्त्वार्थ को भाष्यमान्य और सर्वार्थसिद्धि मान्य ऐसे दो पाठ प्रचलित हैं। इनमें कौन सा पाठ प्राचीन और मौलिक है तथा कौन-सा विकसित है ? यह विषय विवादास्पद रहा है। इस सम्बंध में विस्तृत चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि जहां सर्वार्थसिद्धिमान्य पाठ भाषा, व्याकरण और विषयवस्तु तीनों की दृष्टि से अपेक्षाकृत शुद्ध, व्याकरण सन्मत और विकसित है, वहीं भाष्यमान्य मूलपाठ उसकी अपेक्षा भाषायी दृष्टि से पूर्ववर्ती और कम विकसित प्रतीत होता है। अतः भाष्यमान्यपाठ की प्राचीनता सुस्पष्ट है। सुजिका ओहिरो आदि विदेशी विद्वानों का भी यही मन्तव्य है।