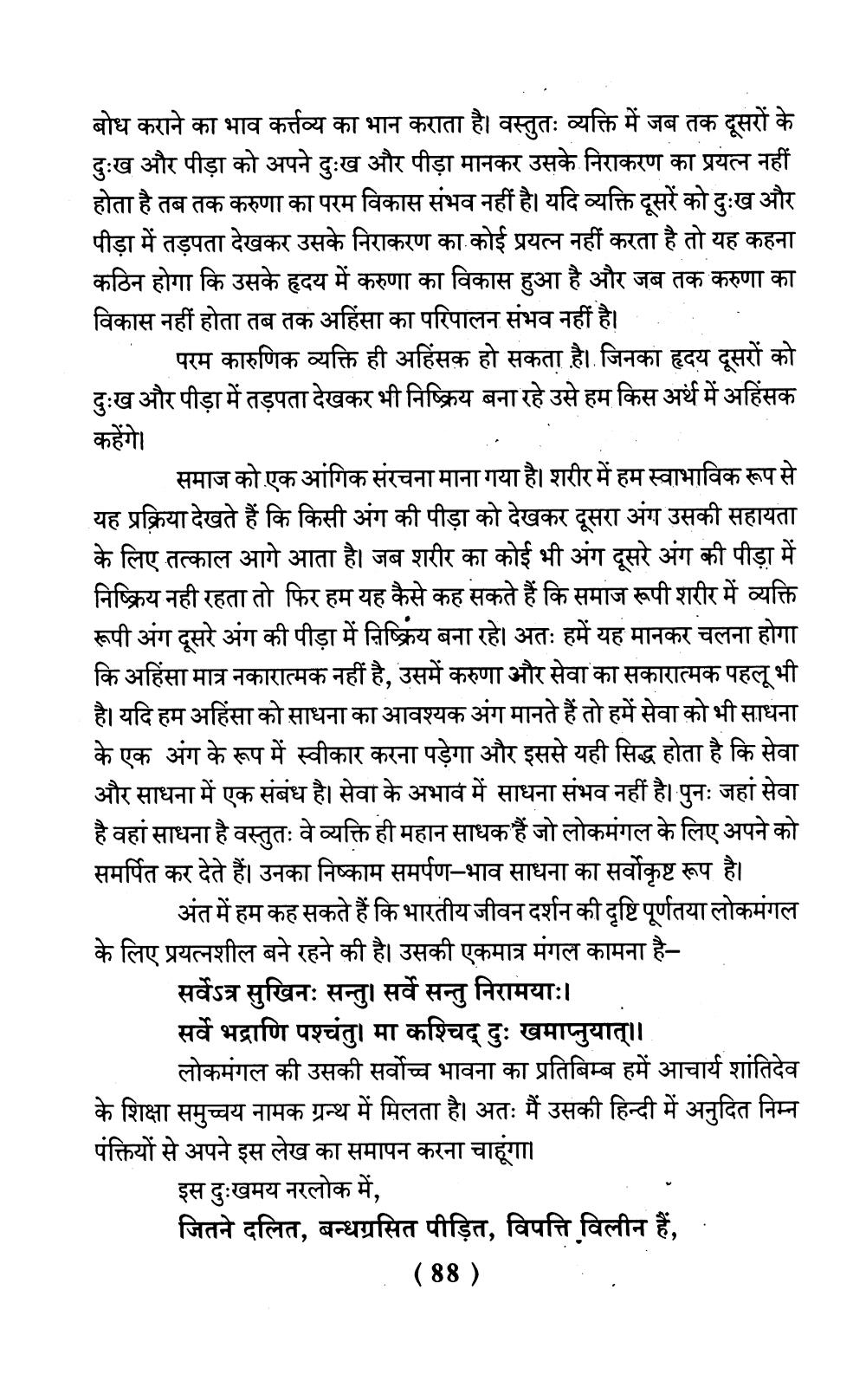________________ बोध कराने का भाव कर्तव्य का भान कराता है। वस्तुतः व्यक्ति में जब तक दूसरों के दुःख और पीड़ा को अपने दुःख और पीड़ा मानकर उसके निराकरण का प्रयत्न नहीं होता है तब तक करुणा का परम विकास संभव नहीं है। यदि व्यक्ति दूसरे को दुःख और पीड़ा में तड़पता देखकर उसके निराकरण का कोई प्रयत्न नहीं करता है तो यह कहना कठिन होगा कि उसके हृदय में करुणा का विकास हुआ है और जब तक करुणा का विकास नहीं होता तब तक अहिंसा का परिपालन संभव नहीं है। परम कारुणिक व्यक्ति ही अहिंसक हो सकता है। जिनका हृदय दूसरों को दुःख और पीड़ा में तड़पता देखकर भी निष्क्रिय बना रहे उसे हम किस अर्थ में अहिंसक कहेंगे। समाज को एक आंगिक संरचना माना गया है। शरीर में हम स्वाभाविक रूप से यह प्रक्रिया देखते हैं कि किसी अंग की पीड़ा को देखकर दूसरा अंग उसकी सहायता के लिए तत्काल आगे आता है। जब शरीर का कोई भी अंग दूसरे अंग की पीड़ा में निष्क्रिय नही रहता तो फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि समाज रूपी शरीर में व्यक्ति रूपी अंग दूसरे अंग की पीड़ा में निष्क्रिय बना रहे। अतः हमें यह मानकर चलना होगा कि अहिंसा मात्र नकारात्मक नहीं है, उसमें करुणा और सेवा का सकारात्मक पहलू भी है। यदि हम अहिंसा को साधना का आवश्यक अंग मानते हैं तो हमें सेवा को भी साधना के एक अंग के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और इससे यही सिद्ध होता है कि सेवा और साधना में एक संबंध है। सेवा के अभाव में साधना संभव नहीं है। पुनः जहां सेवा है वहां साधना है वस्तुतः वे व्यक्ति ही महान साधक हैं जो लोकमंगल के लिए अपने को समर्पित कर देते हैं। उनका निष्काम समर्पण-भाव साधना का सर्वोकृष्ट रूप है। अंत में हम कह सकते हैं कि भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि पूर्णतया लोकमंगल के लिए प्रयत्नशील बने रहने की है। उसकी एकमात्र मंगल कामना है सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु। सर्वे सन्तु निरामयाः। . सर्वे भद्राणि पश्चंतु। मा कश्चिद् दुः खमाप्नुयात्।। लोकमंगल की उसकी सर्वोच्च भावना का प्रतिबिम्ब हमें आचार्य शांतिदेव के शिक्षा समुच्चय नामक ग्रन्थ में मिलता है। अतः मैं उसकी हिन्दी में अनुदित निम्न पंक्तियों से अपने इस लेख का समापन करना चाहूंगा। इस दुःखमय नरलोक में, जितने दलित, बन्धग्रसित पीड़ित, विपत्ति विलीन हैं, . (88)