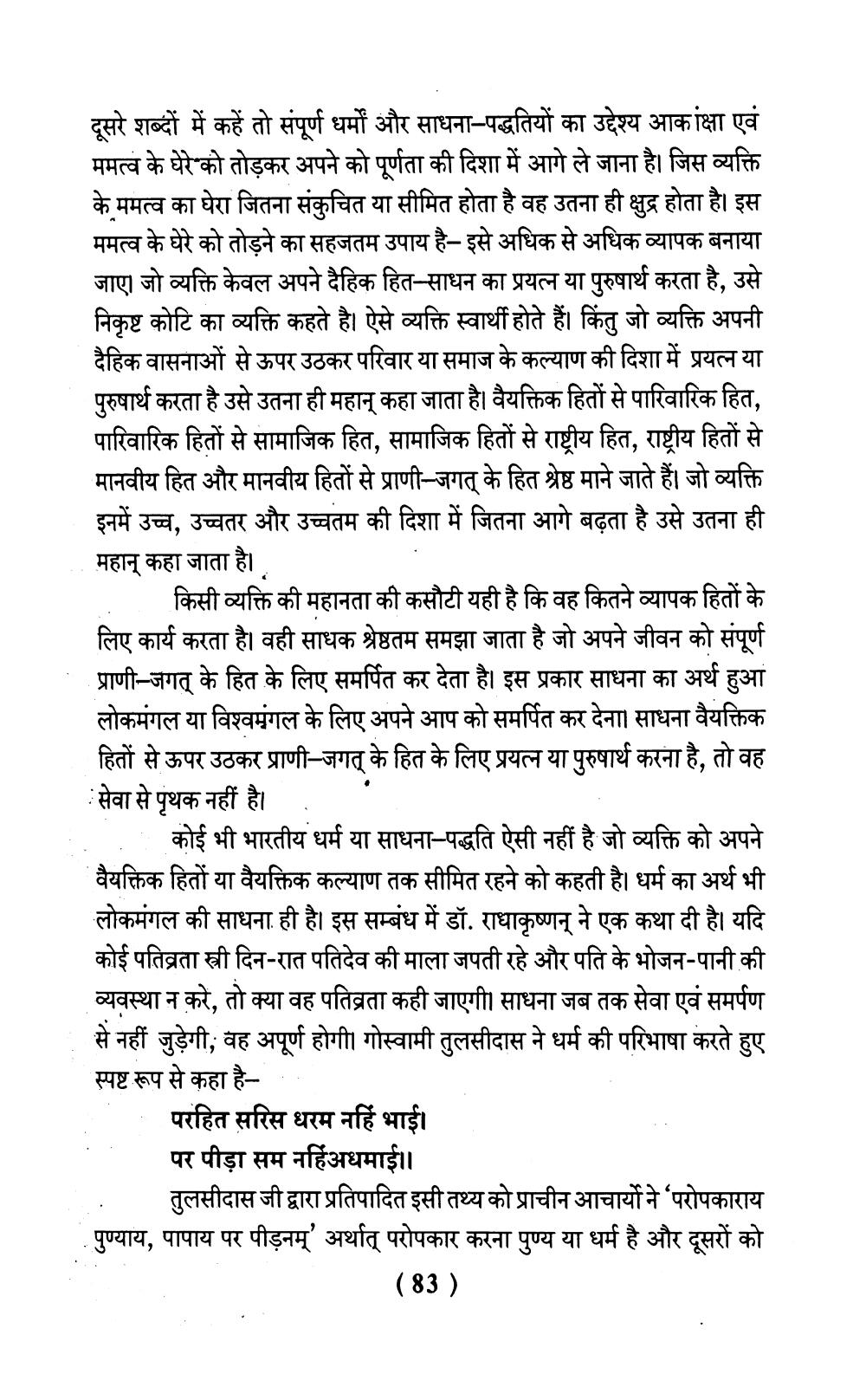________________ दूसरे शब्दों में कहें तो संपूर्ण धर्मों और साधना-पद्धतियों का उद्देश्य आकांक्षा एवं ममत्व के घेरे को तोड़कर अपने को पूर्णता की दिशा में आगे ले जाना है। जिस व्यक्ति के ममत्व का घेरा जितना संकुचित या सीमित होता है वह उतना ही क्षुद्र होता है। इस ममत्व के घेरे को तोड़ने का सहजतम उपाय है- इसे अधिक से अधिक व्यापक बनाया जाए। जो व्यक्ति केवल अपने दैहिक हित-साधन का प्रयत्न या पुरुषार्थ करता है, उसे निकृष्ट कोटि का व्यक्ति कहते है। ऐसे व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। किंतु जो व्यक्ति अपनी दैहिक वासनाओं से ऊपर उठकर परिवार या समाज के कल्याण की दिशा में प्रयत्न या पुरुषार्थ करता है उसे उतना ही महान् कहा जाता है। वैयक्तिक हितों से पारिवारिक हित, पारिवारिक हितों से सामाजिक हित, सामाजिक हितों से राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हितों से मानवीय हित और मानवीय हितों से प्राणी-जगत् के हित श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो व्यक्ति इनमें उच्च, उच्चतर और उच्चतम की दिशा में जितना आगे बढ़ता है उसे उतना ही महान् कहा जाता है। किसी व्यक्ति की महानता की कसौटी यही है कि वह कितने व्यापक हितों के लिए कार्य करता है। वही साधक श्रेष्ठतम समझा जाता है जो अपने जीवन को संपूर्ण प्राणी-जगत् के हित के लिए समर्पित कर देता है। इस प्रकार साधना का अर्थ हुआ लोकमंगल या विश्वमंगल के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। साधना वैयक्तिक हितों से ऊपर उठकर प्राणी-जगत् के हित के लिए प्रयत्न या पुरुषार्थ करना है, तो वह सेवा से पृथक नहीं है। . . कोई भी भारतीय धर्म या साधना-पद्धति ऐसी नहीं है जो व्यक्ति को अपने वैयक्तिक हितों या वैयक्तिक कल्याण तक सीमित रहने को कहती है। धर्म का अर्थ भी लोकमंगल की साधना ही है। इस सम्बंध में डॉ. राधाकृष्णन् ने एक कथा दी है। यदि कोई पतिव्रता स्त्री दिन-रात पतिदेव की माला जपती रहे और पति के भोजन-पानी की व्यवस्था न करे, तो क्या वह पतिव्रता कही जाएगी। साधना जब तक सेवा एवं समर्पण से नहीं जुड़ेगी; वह अपूर्ण होगी। गोस्वामी तुलसीदास ने धर्म की परिभाषा करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है परहित सरिस धरम नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिंअधमाई।। तुलसीदास जी द्वारा प्रतिपादित इसी तथ्य को प्राचीन आचार्यो ने परोपकाराय पुण्याय, पापाय पर पीड़नम्' अर्थात् परोपकार करना पुण्य या धर्म है और दूसरों को (83)