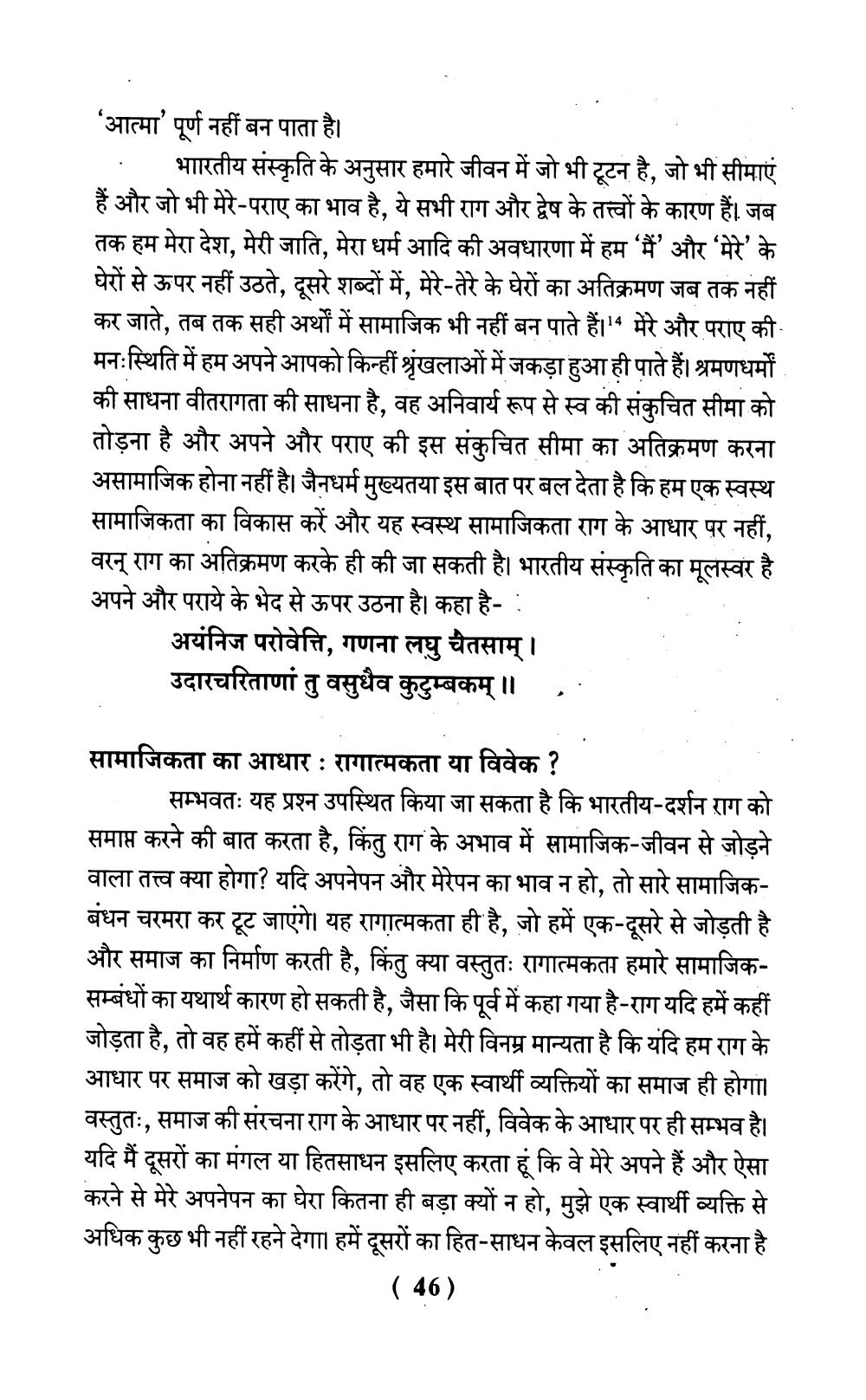________________ 'आत्मा' पूर्ण नहीं बन पाता है। . भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे जीवन में जो भी टूटन है, जो भी सीमाएं हैं और जो भी मेरे-पराए का भाव है, ये सभी राग और द्वेष के तत्त्वों के कारण हैं। जब तक हम मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म आदि की अवधारणा में हम 'मैं' और 'मेरे' के घेरों से ऊपर नहीं उठते, दूसरे शब्दों में, मेरे-तेरे के घेरों का अतिक्रमण जब तक नहीं कर जाते, तब तक सही अर्थों में सामाजिक भी नहीं बन पाते हैं।14 मेरे और पराए की मनःस्थिति में हम अपने आपको किन्हीं श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ ही पाते हैं। श्रमणधर्मों की साधना वीतरागता की साधना है, वह अनिवार्य रूप से स्व की संकुचित सीमा को तोड़ना है और अपने और पराए की इस संकुचित सीमा का अतिक्रमण करना असामाजिक होना नहीं है। जैनधर्म मुख्यतया इस बात पर बल देता है कि हम एक स्वस्थ सामाजिकता का विकास करें और यह स्वस्थ सामाजिकता राग के आधार पर नहीं, वरन् राग का अतिक्रमण करके ही की जा सकती है। भारतीय संस्कृति का मूलस्वर है अपने और पराये के भेद से ऊपर उठना है। कहा है- : अयंनिज परोवेत्ति, गणना लघु चैतसाम्। उदारचरिताणां तु वसुधैव कुटुम्बकम् // , सामाजिकता का आधार : रागात्मकता या विवेक ? सम्भवतः यह प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है कि भारतीय-दर्शन राग को समाप्त करने की बात करता है, किंतु राग के अभाव में सामाजिक-जीवन से जोड़ने वाला तत्त्व क्या होगा? यदि अपनेपन और मेरेपन का भाव न हो, तो सारे सामाजिकबंधन चरमरा कर टूट जाएंगे। यह रागात्मकता ही है, जो हमें एक-दूसरे से जोड़ती है और समाज का निर्माण करती है, किंतु क्या वस्तुतः रागात्मकता हमारे सामाजिकसम्बंधों का यथार्थ कारण हो सकती है, जैसा कि पूर्व में कहा गया है-राग यदि हमें कहीं जोड़ता है, तो वह हमें कहीं से तोड़ता भी है। मेरी विनम्र मान्यता है कि यदि हम राग के आधार पर समाज को खड़ा करेंगे, तो वह एक स्वार्थी व्यक्तियों का समाज ही होगा। वस्तुतः, समाज की संरचना राग के आधार पर नहीं, विवेक के आधार पर ही सम्भव है। यदि मैं दूसरों का मंगल या हितसाधन इसलिए करता हूं कि वे मेरे अपने हैं और ऐसा करने से मेरे अपनेपन का घेरा कितना ही बड़ा क्यों न हो, मुझे एक स्वार्थी व्यक्ति से अधिक कुछ भी नहीं रहने देगा। हमें दूसरों का हित-साधन केवल इसलिए नहीं करना है (46)