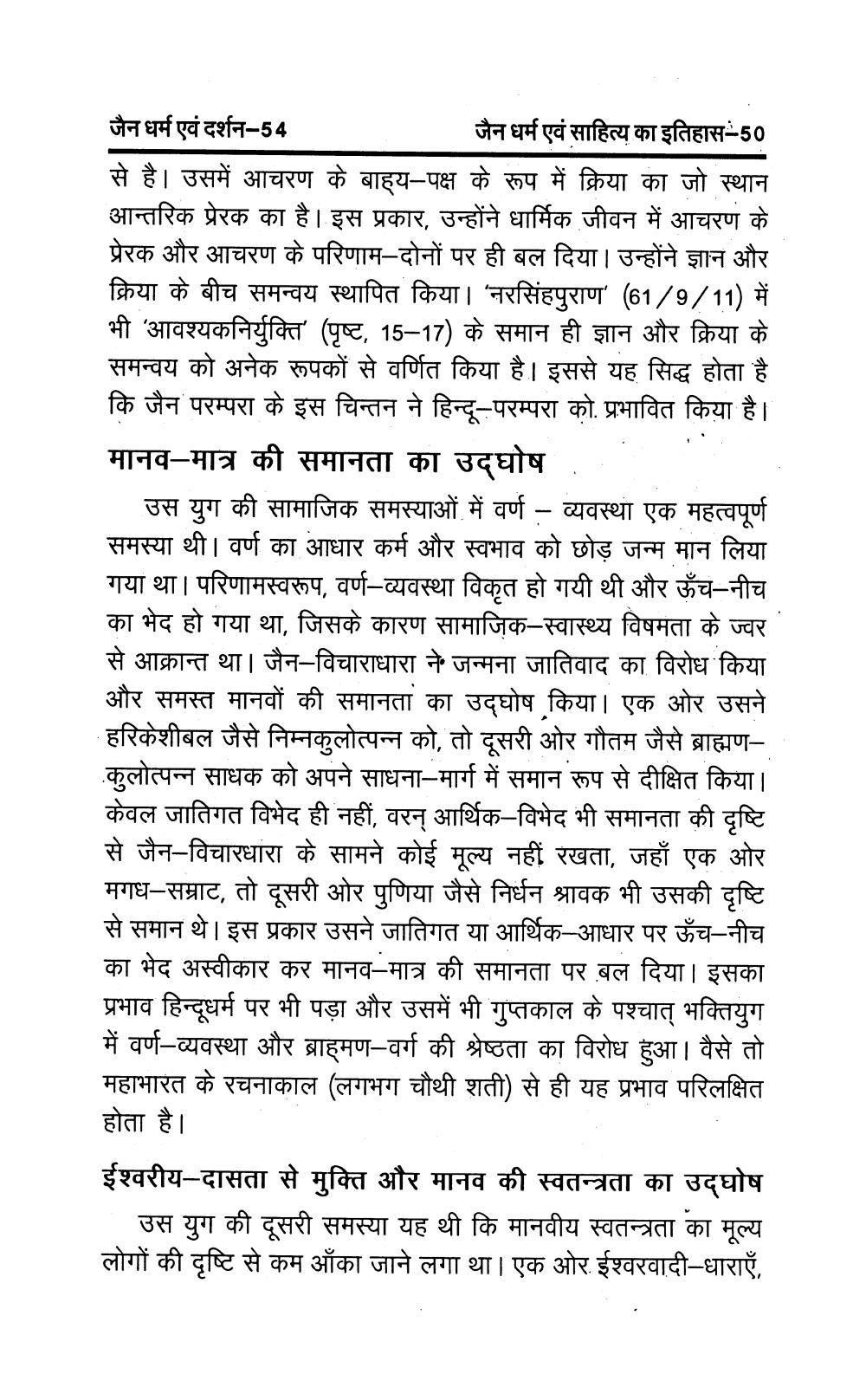________________ जैन धर्म एवं दर्शन-54 जैन धर्म एवं साहित्य का इतिहास-50 से है। उसमें आचरण के बाह्य-पक्ष के रूप में क्रिया का जो स्थान आन्तरिक प्रेरक का है। इस प्रकार, उन्होंने धार्मिक जीवन में आचरण के प्रेरक और आचरण के परिणाम-दोनों पर ही बल दिया। उन्होंने ज्ञान और क्रिया के बीच समन्वय स्थापित किया। 'नरसिंहपुराण' (61/9/11) में भी 'आवश्यकनियुक्ति' (पृष्ट, 15-17) के समान ही ज्ञान और क्रिया के समन्वय को अनेक रूपकों से वर्णित किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जैन परम्परा के इस चिन्तन ने हिन्दू-परम्परा को प्रभावित किया है। मानव-मात्र की समानता का उद्घोष . उस युग की सामाजिक समस्याओं में वर्ण - व्यवस्था एक महत्वपूर्ण समस्या थी। वर्ण का आधार कर्म और स्वभाव को छोड़ जन्म मान लिया गया था। परिणामस्वरूप, वर्ण-व्यवस्था विकृत हो गयी थी और ऊँच-नीच का भेद हो गया था, जिसके कारण सामाजिक-स्वास्थ्य विषमता के ज्वर से आक्रान्त था। जैन-विचाराधारा ने जन्मना जातिवाद का विरोध किया और समस्त मानवों की समानता का उद्घोष किया। एक ओर उसने हरिकेशीबल जैसे निम्नकुलोत्पन्न को, तो दूसरी ओर गौतम जैसे ब्राह्मणकुलोत्पन्न साधक को अपने साधना-मार्ग में समान रूप से दीक्षित किया। केवल जातिगत विभेद ही नहीं, वरन् आर्थिक-विभेद भी समानता की दृष्टि से जैन-विचारधारा के सामने कोई मूल्य नहीं रखता, जहाँ एक ओर मगध-सम्राट, तो दूसरी ओर पुणिया जैसे निर्धन श्रावक भी उसकी दृष्टि से समान थे। इस प्रकार उसने जातिगत या आर्थिक आधार पर ऊँच-नीच का भेद अस्वीकार कर मानव-मात्र की समानता पर बल दिया। इसका प्रभाव हिन्दूधर्म पर भी पड़ा और उसमें भी गुप्तकाल के पश्चात् भक्तियुग में वर्ण-व्यवस्था और ब्राह्मण-वर्ग की श्रेष्ठता का विरोध हुआ। वैसे तो महाभारत के रचनाकाल (लगभग चौथी शती) से ही यह प्रभाव परिलक्षित होता है। ईश्वरीय-दासता से मुक्ति और मानव की स्वतन्त्रता का उद्घोष उस युग की दूसरी समस्या यह थी कि मानवीय स्वतन्त्रता का मूल्य लोगों की दृष्टि से कम आँका जाने लगा था। एक ओर ईश्वरवादी-धाराएँ,