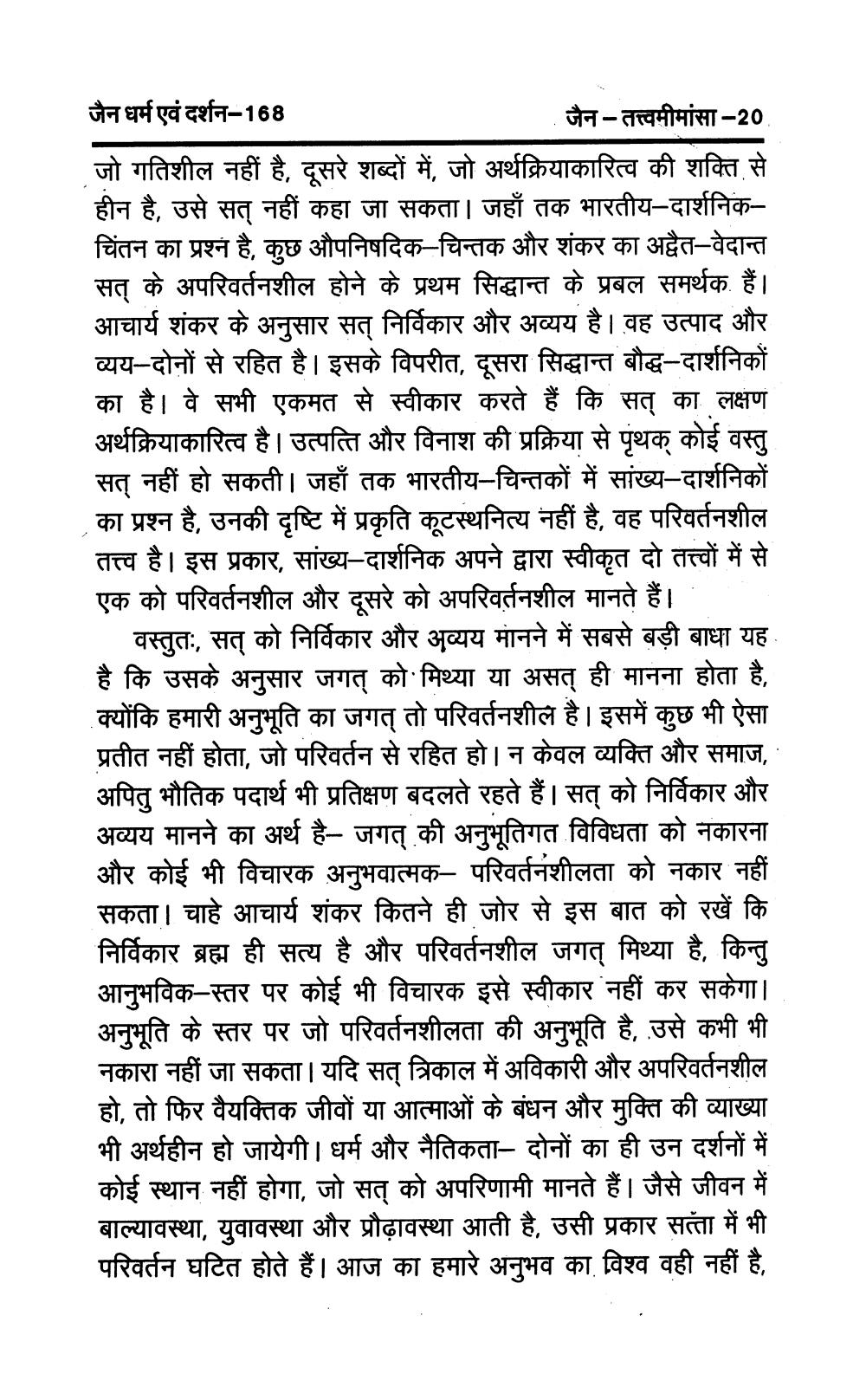________________ जैन धर्म एवं दर्शन-168 जैन-तत्त्वमीमांसा-20 जो गतिशील नहीं है, दूसरे शब्दों में, जो अर्थक्रियाकारित्व की शक्ति से हीन है, उसे सत नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक भारतीय-दार्शनिकचिंतन का प्रश्न है, कुछ औपनिषदिक-चिन्तक और शंकर का अद्वैत-वेदान्त सत् के अपरिवर्तनशील होने के प्रथम सिद्धान्त के प्रबल समर्थक हैं। आचार्य शंकर के अनुसार सत् निर्विकार और अव्यय है। वह उत्पाद और व्यय-दोनों से रहित है। इसके विपरीत, दूसरा सिद्धान्त बौद्ध-दार्शनिकों का है। वे सभी एकमत से स्वीकार करते हैं कि सत् का लक्षण अर्थक्रियाकारित्व है। उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया से पृथक् कोई वस्तु सत् नहीं हो सकती। जहाँ तक भारतीय-चिन्तकों में सांख्य दार्शनिकों का प्रश्न है, उनकी दृष्टि में प्रकृति कूटस्थनित्य नहीं है, वह परिवर्तनशील तत्त्व है। इस प्रकार, सांख्य दार्शनिक अपने द्वारा स्वीकृत दो तत्त्वों में से एक को परिवर्तनशील और दूसरे को अपरिवर्तनशील मानते हैं। ___ वस्तुतः, सत् को निर्विकार और अव्यय मानने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि उसके अनुसार जगत् को मिथ्या या असत् ही मानना होता है, क्योंकि हमारी अनुभूति का जगत् तो परिवर्तनशील है। इसमें कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं होता, जो परिवर्तन से रहित हो। न केवल व्यक्ति और समाज, अपितु भौतिक पदार्थ भी प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। सत् को निर्विकार और अव्यय मानने का अर्थ है- जगत् की अनुभूतिगत विविधता को नकारना और कोई भी विचारक अनुभवात्मक- परिवर्तनशीलता को नकार नहीं सकता। चाहे आचार्य शंकर कितने ही जोर से इस बात को रखें कि निर्विकार ब्रह्म ही सत्य है और परिवर्तनशील जगत् मिथ्या है, किन्तु आनुभविक स्तर पर कोई भी विचारक इसे स्वीकार नहीं कर सकेगा। अनुभूति के स्तर पर जो परिवर्तनशीलता की अनुभूति है, उसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता। यदि सत् त्रिकाल में अविकारी और अपरिवर्तनशील हो, तो फिर वैयक्तिक जीवों या आत्माओं के बंधन और मुक्ति की व्याख्या भी अर्थहीन हो जायेगी। धर्म और नैतिकता- दोनों का ही उन दर्शनों में कोई स्थान नहीं होगा, जो सत् को अपरिणामी मानते हैं। जैसे जीवन में बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था आती है, उसी प्रकार सत्ता में भी परिवर्तन घटित होते हैं। आज का हमारे अनुभव का विश्व वही नहीं है,