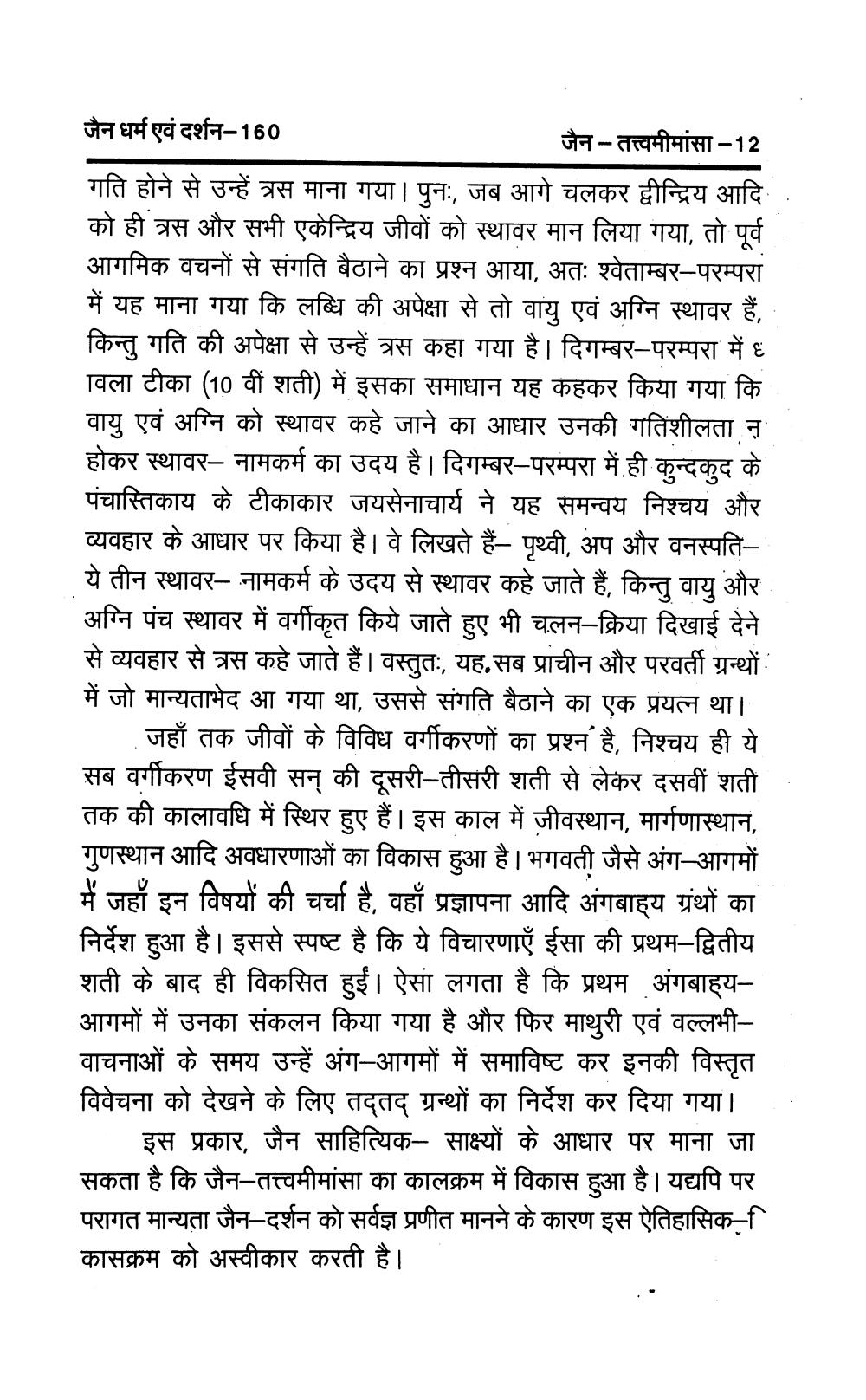________________ जैन धर्म एवं दर्शन-160 जैन-तत्त्वमीमांसा -12 गति होने से उन्हें त्रस माना गया। पुनः, जब आगे चलकर द्वीन्द्रिय आदि को ही त्रस और सभी एकेन्द्रिय जीवों को स्थावर मान लिया गया, तो पूर्व आगमिक वचनों से संगति बैठाने का प्रश्न आया, अतः श्वेताम्बर–परम्परा में यह माना गया कि लब्धि की अपेक्षा से तो वायु एवं अग्नि स्थावर हैं, किन्तु गति की अपेक्षा से उन्हें त्रस कहा गया है। दिगम्बर-परम्परा में विला टीका (10 वीं शती) में इसका समाधान यह कहकर किया गया कि वायु एवं अग्नि को स्थावर कहे जाने का आधार उनकी गतिशीलता न होकर स्थावर- नामकर्म का उदय है। दिगम्बर-परम्परा में ही कुन्दकुद के पंचास्तिकाय के टीकाकार जयसेनाचार्य ने यह समन्वय निश्चय और व्यवहार के आधार पर किया है। वे लिखते हैं- पृथ्वी, अप और वनस्पतिये तीन स्थावर- नामकर्म के उदय से स्थावर कहे जाते हैं, किन्तु वायु और अग्नि पंच स्थावर में वर्गीकृत किये जाते हुए भी चलन-क्रिया दिखाई देने से व्यवहार से त्रस कहे जाते हैं। वस्तुतः, यह.सब प्राचीन और परवर्ती ग्रन्थों में जो मान्यताभेद आ गया था, उससे संगति बैठाने का एक प्रयत्न था। जहाँ तक जीवों के विविध वर्गीकरणों का प्रश्न है, निश्चय ही ये सब वर्गीकरण ईसवी सन् की दूसरी-तीसरी शती से लेकर दसवीं शती तक की कालावधि में स्थिर हुए हैं। इस काल में जीवस्थान, मार्गणास्थान, गुणस्थान आदि अवधारणाओं का विकास हुआ है। भगवती जैसे अंग-आगमों में जहाँ इन विषयों की चर्चा है, वहाँ प्रज्ञापना आदि अंगबाह्य ग्रंथों का निर्देश हुआ है। इससे स्पष्ट है कि ये विचारणाएँ ईसा की प्रथम-द्वितीय शती के बाद ही विकसित हुईं। ऐसा लगता है कि प्रथम अंगबाह्यआगमों में उनका संकलन किया गया है और फिर माथुरी एवं वल्लभीवाचनाओं के समय उन्हें अंग-आगमों में समाविष्ट कर इनकी विस्तृत विवेचना को देखने के लिए तदतद् ग्रन्थों का निर्देश कर दिया गया। इस प्रकार, जैन साहित्यिक- साक्ष्यों के आधार पर माना जा सकता है कि जैन-तत्त्वमीमांसा का कालक्रम में विकास हुआ है। यद्यपि पर परागत मान्यता जैन-दर्शन को सर्वज्ञ प्रणीत मानने के कारण इस ऐतिहासिक कासक्रम को अस्वीकार करती है।