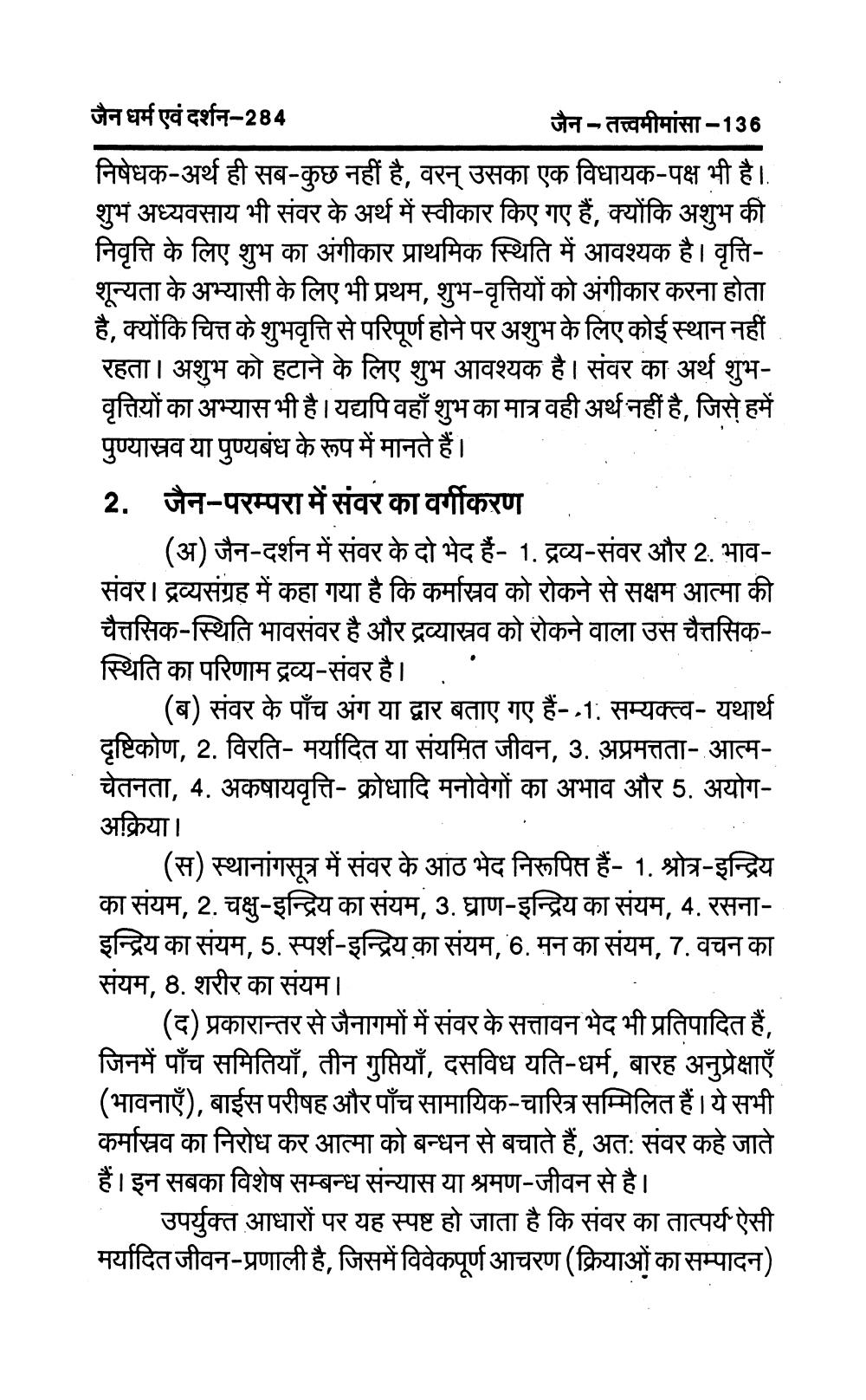________________ जैन धर्म एवं दर्शन-284 जैन- तत्वमीमांसा-136 निषेधक-अर्थ ही सब-कुछ नहीं है, वरन् उसका एक विधायक-पक्ष भी है। शुभ अध्यवसाय भी संवर के अर्थ में स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि अशुभ की निवृत्ति के लिए शुभ का अंगीकार प्राथमिक स्थिति में आवश्यक है। वृत्तिशून्यता के अभ्यासी के लिए भी प्रथम, शुभ-वृत्तियों को अंगीकार करना होता है, क्योंकि चित्त के शुभवृत्ति से परिपूर्ण होने पर अशुभ के लिए कोई स्थान नहीं रहता। अशुभ को हटाने के लिए शुभ आवश्यक है। संवर का अर्थ शुभवृत्तियों का अभ्यास भी है। यद्यपि वहाँ शुभ का मात्र वही अर्थ नहीं है, जिसे हमें पुण्यास्रव या पुण्यबंध के रूप में मानते हैं। 2. जैन-परम्परा में संवर का वर्गीकरण (अ) जैन-दर्शन में संवर के दो भेद हैं- 1. द्रव्य-संवर और 2. भावसंवर। द्रव्यसंग्रह में कहा गया है कि कर्मास्रव को रोकने से सक्षम आत्मा की चैत्तसिक-स्थिति भावसंवर है और द्रव्यास्रव को रोकने वाला उस चैत्तसिकस्थिति का परिणाम द्रव्य-संवर है। .. (ब) संवर के पाँच अंग या द्वार बताए गए हैं-.1: सम्यक्त्व- यथार्थ दृष्टिकोण, 2. विरति- मर्यादित या संयमित जीवन, 3. अप्रमत्तता- आत्मचेतनता, 4. अकषायवृत्ति- क्रोधादि मनोवेगों का अभाव और 5. अयोगअक्रिया। (स) स्थानांगसूत्र में संवर के आंठ भेद निरूपित हैं- 1. श्रोत्र-इन्द्रिय का संयम, 2. चक्षु-इन्द्रिय का संयम, 3. घ्राण-इन्द्रिय का संयम, 4. रसनाइन्द्रिय का संयम, 5. स्पर्श-इन्द्रिय का संयम, 6. मन का संयम, 7. वचन का संयम, 8. शरीर का संयम। (द) प्रकारान्तर से जैनागमों में संवर के सत्तावन भेद भी प्रतिपादित हैं, जिनमें पाँच समितियाँ, तीन गुप्तियाँ, दसविध यति-धर्म, बारह अनुप्रेक्षाएँ (भावनाएँ), बाईस परीषह और पाँच सामायिक-चारित्र सम्मिलित हैं। ये सभी कर्मास्रव का निरोध कर आत्मा को बन्धन से बचाते हैं, अत: संवर कहे जाते हैं। इन सबका विशेष सम्बन्ध संन्यास या श्रमण-जीवन से है। __ उपर्युक्त आधारों पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संवर का तात्पर्य ऐसी मर्यादित जीवन-प्रणाली है, जिसमें विवेकपूर्ण आचरण (क्रियाओं का सम्पादन)