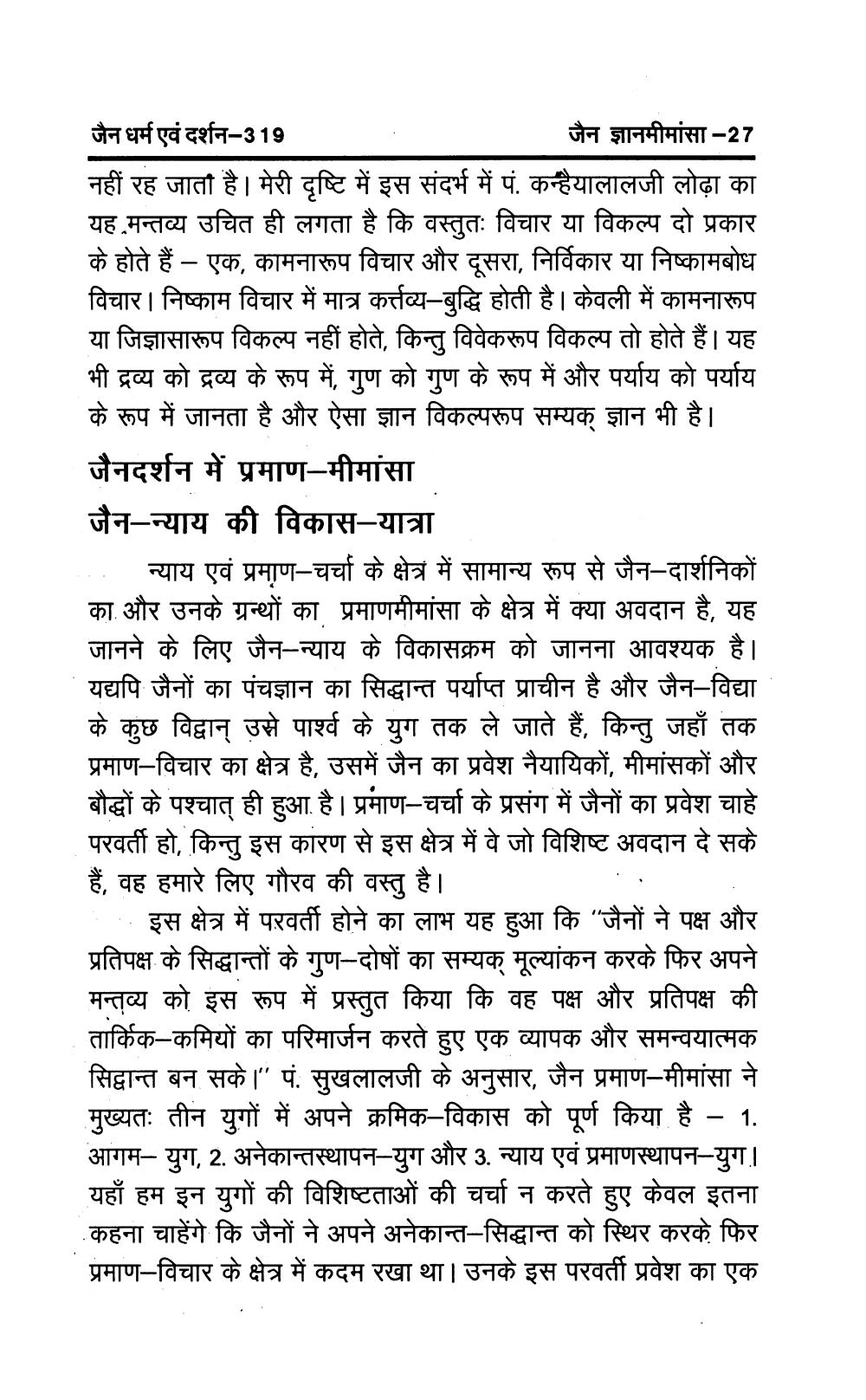________________ जैन धर्म एवं दर्शन-319 जैन ज्ञानमीमांसा -27 नहीं रह जाता है। मेरी दृष्टि में इस संदर्भ में पं. कन्हैयालालजी लोढ़ा का यह मन्तव्य उचित ही लगता है कि वस्तुतः विचार या विकल्प दो प्रकार के होते हैं - एक, कामनारूप विचार और दूसरा, निर्विकार या निष्कामबोध विचार / निष्काम विचार में मात्र कर्तव्य-बुद्धि होती है। केवली में कामनारूप या जिज्ञासारूप विकल्प नहीं होते, किन्तु विवेकरूप विकल्प तो होते हैं। यह भी द्रव्य को द्रव्य के रूप में, गुण को गुण के रूप में और पर्याय को पर्याय के रूप में जानता है और ऐसा ज्ञान विकल्परूप सम्यक् ज्ञान भी है। जैनदर्शन में प्रमाण-मीमांसा जैन-न्याय की विकास यात्रा .... न्याय एवं प्रमाण-चर्चा के क्षेत्र में सामान्य रूप से जैन-दार्शनिकों का और उनके ग्रन्थों का प्रमाणमीमांसा के क्षेत्र में क्या अवदान है, यह जानने के लिए जैन-न्याय के विकासक्रम को जानना आवश्यक है। यद्यपि जैनों का पंचज्ञान का सिद्धान्त पर्याप्त प्राचीन है और जैन-विद्या के कुछ विद्वान् उसे पार्श्व के युग तक ले जाते हैं, किन्तु जहाँ तक प्रमाण-विचार का क्षेत्र है, उसमें जैन का प्रवेश नैयायिकों, मीमांसकों और बौद्धों के पश्चात् ही हुआ है। प्रमाण-चर्चा के प्रसंग में जैनों का प्रवेश चाहे परवर्ती हो, किन्तु इस कारण से इस क्षेत्र में वे जो विशिष्ट अवदान दे सके हैं, वह हमारे लिए गौरव की वस्तु है। .. इस क्षेत्र में परवर्ती होने का लाभ यह हुआ कि "जैनों ने पक्ष और प्रतिपक्ष के सिद्धान्तों के गुण-दोषों का सम्यक मूल्यांकन करके फिर अपने मन्तव्य को इस रूप में प्रस्तुत किया कि वह पक्ष और प्रतिपक्ष की तार्किक-कमियों का परिमार्जन करते हुए एक व्यापक और समन्वयात्मक सिद्वान्त बन सके।" पं. सुखलालजी के अनुसार, जैन प्रमाण-मीमांसा ने मुख्यतः तीन युगों में अपने क्रमिक-विकास को पूर्ण किया है - 1. आगम- युग, 2. अनेकान्तस्थापन-युग और 3. न्याय एवं प्रमाणस्थापन-युग। यहाँ हम इन युगों की विशिष्टताओं की चर्चा न करते हुए केवल इतना कहना चाहेंगे कि जैनों ने अपने अनेकान्त-सिद्धान्त को स्थिर करके फिर प्रमाण-विचार के क्षेत्र में कदम रखा था। उनके इस परवर्ती प्रवेश का एक