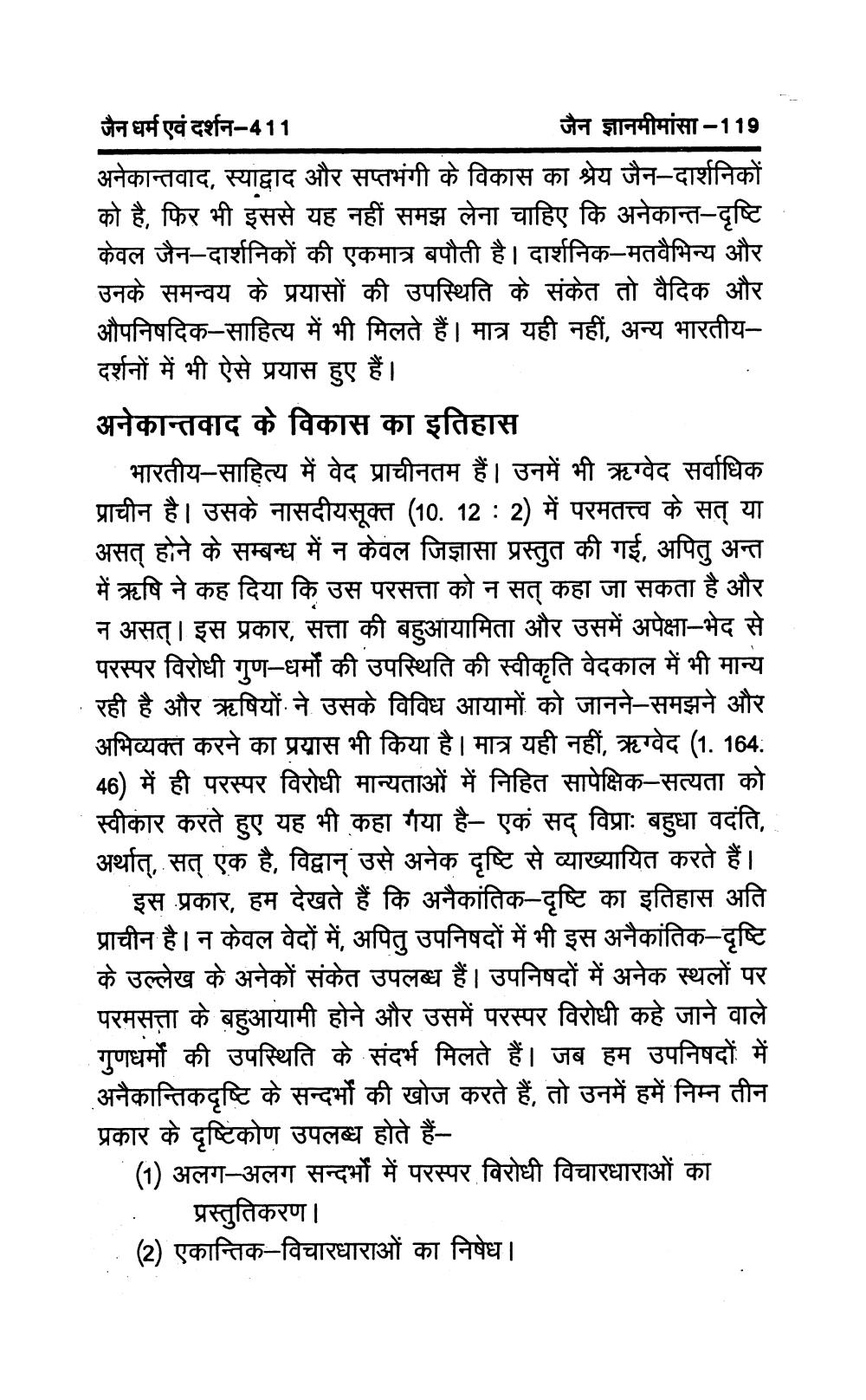________________ जैन धर्म एवं दर्शन-411 जैन ज्ञानमीमांसा-119 अनेकान्तवाद, स्याद्वाद और सप्तभंगी के विकास का श्रेय जैन-दार्शनिकों को है, फिर भी इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अनेकान्त-दृष्टि केवल जैन-दार्शनिकों की एकमात्र बपौती है। दार्शनिक-मतवैभिन्य और उनके समन्वय के प्रयासों की उपस्थिति के संकेत तो वैदिक और औपनिषदिक-साहित्य में भी मिलते हैं। मात्र यही नहीं, अन्य भारतीयदर्शनों में भी ऐसे प्रयास हुए हैं। अनेकान्तवाद के विकास का इतिहास भारतीय साहित्य में वेद प्राचीनतम हैं। उनमें भी ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है। उसके नासदीयसूक्त (10. 12 : 2) में परमतत्त्व के सत् या असत् होने के सम्बन्ध में न केवल जिज्ञासा प्रस्तुत की गई, अपितु अन्त में ऋषि ने कह दिया कि उस परसत्ता को न सत कहा जा सकता है और न असत् / इस प्रकार, सत्ता की बहुआयामिता और उसमें अपेक्षा-भेद से परस्पर विरोधी गुण-धर्मों की उपस्थिति की स्वीकृति वेदकाल में भी मान्य रही है और ऋषियों ने उसके विविध आयामों को जानने-समझने और अभिव्यक्त करने का प्रयास भी किया है। मात्र यही नहीं, ऋग्वेद (1. 164. 46) में ही परस्पर विरोधी मान्यताओं में निहित सापेक्षिक-सत्यता को स्वीकार करते हुए यह भी कहा गया है- एकं सद् विप्राः बहुधा वदंति, अर्थात्, सत् एक है, विद्वान् उसे अनेक दृष्टि से व्याख्यायित करते हैं। इस प्रकार, हम देखते हैं कि अनैकांतिक-दृष्टि का इतिहास अति प्राचीन है। न केवल वेदों में, अपितु उपनिषदों में भी इस अनैकांतिक-दृष्टि के उल्लेख के अनेकों संकेत उपलब्ध हैं। उपनिषदों में अनेक स्थलों पर परमसत्ता के बहुआयामी होने और उसमें परस्पर विरोधी कहे जाने वाले गुणधर्मों की उपस्थिति के संदर्भ मिलते हैं। जब हम उपनिषदों में अनैकान्तिकदृष्टि के सन्दर्भो की खोज करते हैं, तो उनमें हमें निम्न तीन प्रकार के दृष्टिकोण उपलब्ध होते हैं (1) अलग-अलग सन्दर्भो में परस्पर विरोधी विचारधाराओं का . प्रस्तुतिकरण। . (2) एकान्तिक-विचारधाराओं का निषेध /