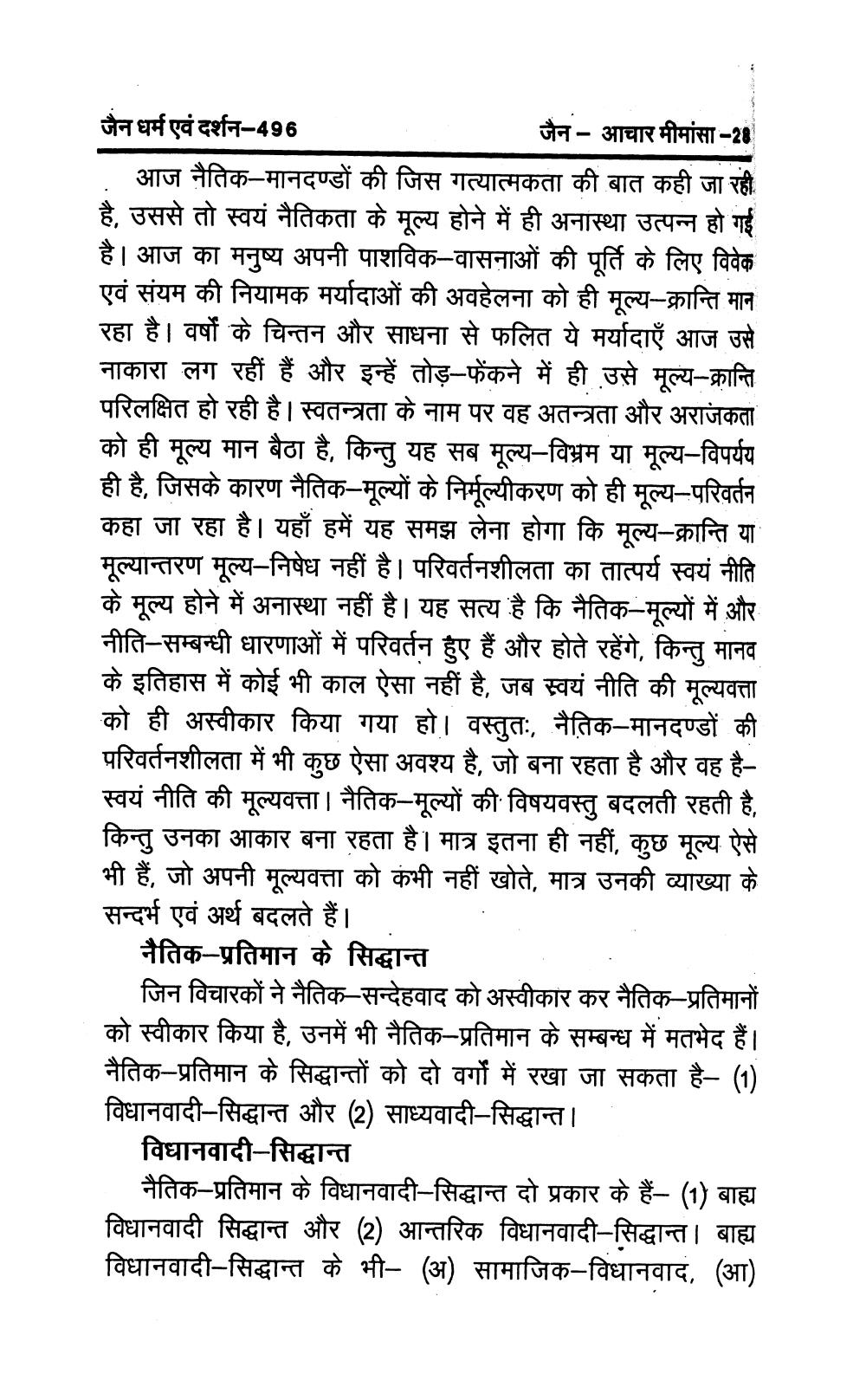________________ जैन धर्म एवं दर्शन-496 जैन - आचार मीमांसा-20 आज नैतिक-मानदण्डों की जिस गत्यात्मकता की बात कही जा रही है, उससे तो स्वयं नैतिकता के मूल्य होने में ही अनास्था उत्पन्न हो गई है। आज का मनुष्य अपनी पाशविक-वासनाओं की पूर्ति के लिए विवेक एवं संयम की नियामक मर्यादाओं की अवहेलना को ही मूल्य-क्रान्ति मान रहा है। वर्षों के चिन्तन और साधना से फलित ये मर्यादाएँ आज उसे नाकारा लग रही हैं और इन्हें तोड़-फेंकने में ही उसे मूल्य-क्रान्ति परिलक्षित हो रही है। स्वतन्त्रता के नाम पर वह अतन्त्रता और अराजकता को ही मूल्य मान बैठा है, किन्तु यह सब मूल्य-विभ्रम या मूल्य–विपर्यय ही है, जिसके कारण नैतिक मूल्यों के निर्मूल्यीकरण को ही मूल्य-परिवर्तन कहा जा रहा है। यहाँ हमें यह समझ लेना होगा कि मूल्य-क्रान्ति या मूल्यान्तरण मूल्य-निषेध नहीं है। परिवर्तनशीलता का तात्पर्य स्वयं नीति के मूल्य होने में अनास्था नहीं है। यह सत्य है कि नैतिक मूल्यों में और नीति-सम्बन्धी धारणाओं में परिवर्तन हुए हैं और होते रहेंगे, किन्तु मानव के इतिहास में कोई भी काल ऐसा नहीं है, जब स्वयं नीति की मूल्यवत्ता को ही अस्वीकार किया गया हो। वस्तुतः, नैतिक-मानदण्डों की परिवर्तनशीलता में भी कुछ ऐसा अवश्य है, जो बना रहता है और वह हैस्वयं नीति की मूल्यवत्ता / नैतिक मूल्यों की विषयवस्तु बदलती रहती है, किन्तु उनका आकार बना रहता है। मात्र इतना ही नहीं, कुछ मूल्य ऐसे भी हैं, जो अपनी मूल्यवत्ता को कभी नहीं खोते, मात्र उनकी व्याख्या के सन्दर्भ एवं अर्थ बदलते हैं। नैतिक-प्रतिमान के सिद्धान्त जिन विचारकों ने नैतिक-सन्देहवाद को अस्वीकार कर नैतिक-प्रतिमानों को स्वीकार किया है, उनमें भी नैतिक-प्रतिमान के सम्बन्ध में मतभेद हैं। नैतिक-प्रतिमान के सिद्धान्तों को दो वर्गों में रखा जा सकता है- (1) विधानवादी-सिद्धान्त और (2) साध्यवादी-सिद्धान्त। विधानवादी सिद्धान्त नैतिक-प्रतिमान के विधानवादी-सिद्धान्त दो प्रकार के हैं- (1) बाह्य विधानवादी सिद्धान्त और (2) आन्तरिक विधानवादी-सिद्धान्त। बाह्य विधानवादी-सिद्धान्त के भी- (अ) सामाजिक-विधानवाद, (आ)