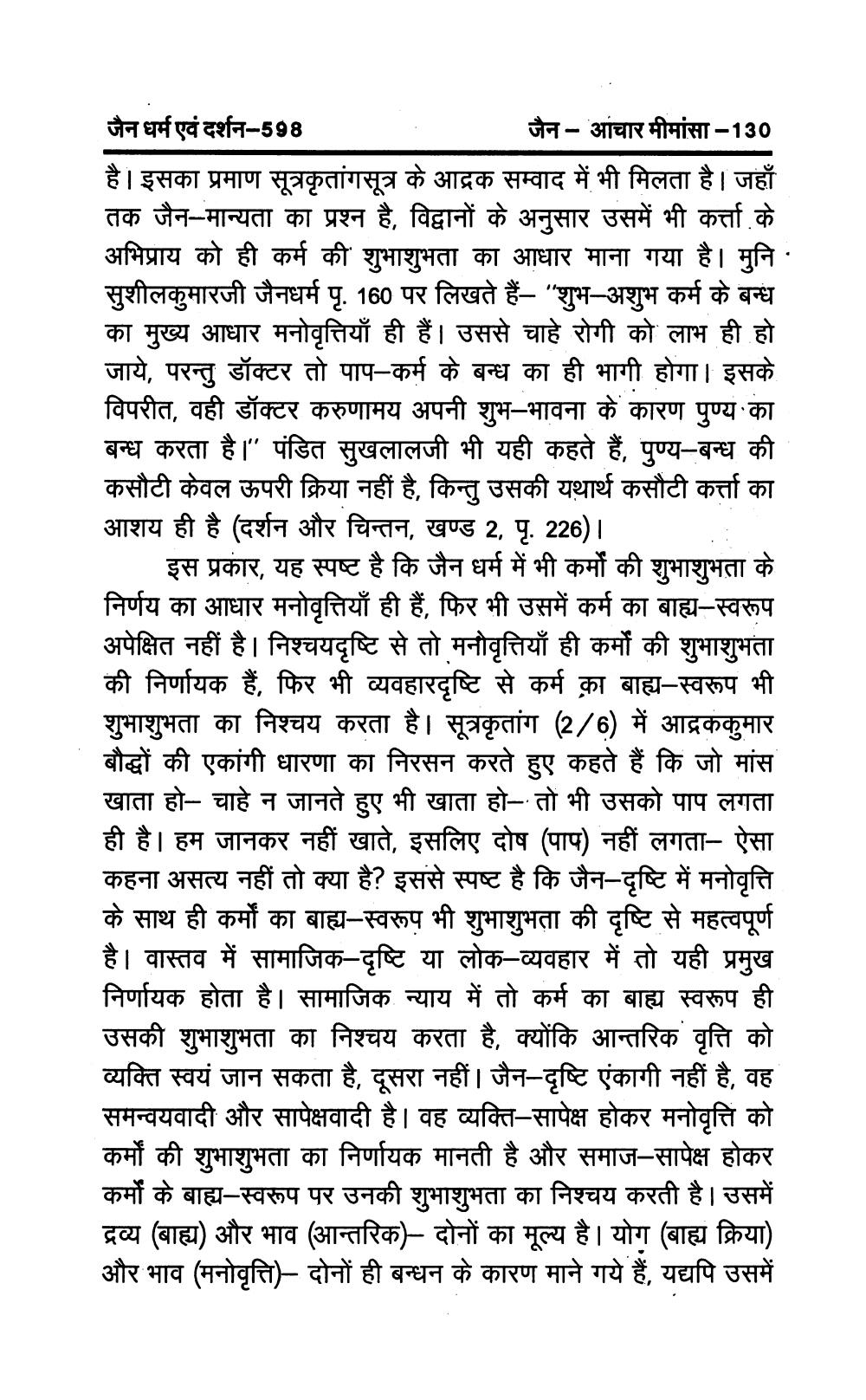________________ जैन धर्म एवं दर्शन-598 जैन- आचार मीमांसा-130 है। इसका प्रमाण सूत्रकृतांगसूत्र के आद्रक सम्वाद में भी मिलता है। जहाँ तक जैन-मान्यता का प्रश्न है, विद्वानों के अनुसार उसमें भी कर्ता के अभिप्राय को ही कर्म की शुभाशुभता का आधार माना गया है। मुनि / सुशीलकुमारजी जैनधर्म पृ. 160 पर लिखते हैं- "शुभ-अशुभ कर्म के बन्ध का मुख्य आधार मनोवृत्तियाँ ही हैं। उससे चाहे रोगी को लाभ ही हो जाये, परन्तु डॉक्टर तो पाप-कर्म के बन्ध का ही भागी होगा। इसके विपरीत, वही डॉक्टर करुणामय अपनी शुभ-भावना के कारण पुण्य का बन्ध करता है।" पंडित सुखलालजी भी यही कहते हैं, पुण्य-बन्ध की कसौटी केवल ऊपरी क्रिया नहीं है, किन्तु उसकी यथार्थ कसौटी कर्ता का आशय ही है (दर्शन और चिन्तन, खण्ड 2, पृ. 226) / इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जैन धर्म में भी कर्मों की शुभाशुभता के निर्णय का आधार मनोवृत्तियाँ ही हैं, फिर भी उसमें कर्म का बाह्य-स्वरूप अपेक्षित नहीं है। निश्चयदृष्टि से तो मनोवृत्तियाँ ही कर्मों की शुभाशुभता की निर्णायक हैं, फिर भी व्यवहारदृष्टि से कर्म का बाह्य-स्वरूप भी शुभाशुभता का निश्चय करता है। सूत्रकृतांग (2/6) में आद्रककुमार बौद्धों की एकांगी धारणा का निरसन करते हुए कहते हैं कि जो मांस खाता हो- चाहे न जानते हुए भी खाता हो- तो भी उसको पाप लगता ही है। हम जानकर नहीं खाते, इसलिए दोष (पाप) नहीं लगता- ऐसा कहना असत्य नहीं तो क्या है? इससे स्पष्ट है कि जैन-दृष्टि में मनोवृत्ति के साथ ही कर्मों का बाह्य-स्वरूप भी शुभाशुभता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वास्तव में सामाजिक-दृष्टि या लोक-व्यवहार में तो यही प्रमुख निर्णायक होता है। सामाजिक न्याय में तो कर्म का बाह्य स्वरूप ही उसकी शुभाशुभता का निश्चय करता है, क्योंकि आन्तरिक वृत्ति को व्यक्ति स्वयं जान सकता है, दूसरा नहीं। जैन-दृष्टि एकागी नहीं है, वह समन्वयवादी और सापेक्षवादी है। वह व्यक्ति-सापेक्ष होकर मनोवृत्ति को कर्मों की शुभाशुभता का निर्णायक मानती है और समाज-सापेक्ष होकर कर्मों के बाह्य-स्वरूप पर उनकी शुभाशुभता का निश्चय करती है। उसमें द्रव्य (बाह्य) और भाव (आन्तरिक)- दोनों का मूल्य है। योग (बाह्य क्रिया) और भाव (मनोवृत्ति)- दोनों ही बन्धन के कारण माने गये हैं, यद्यपि उसमें