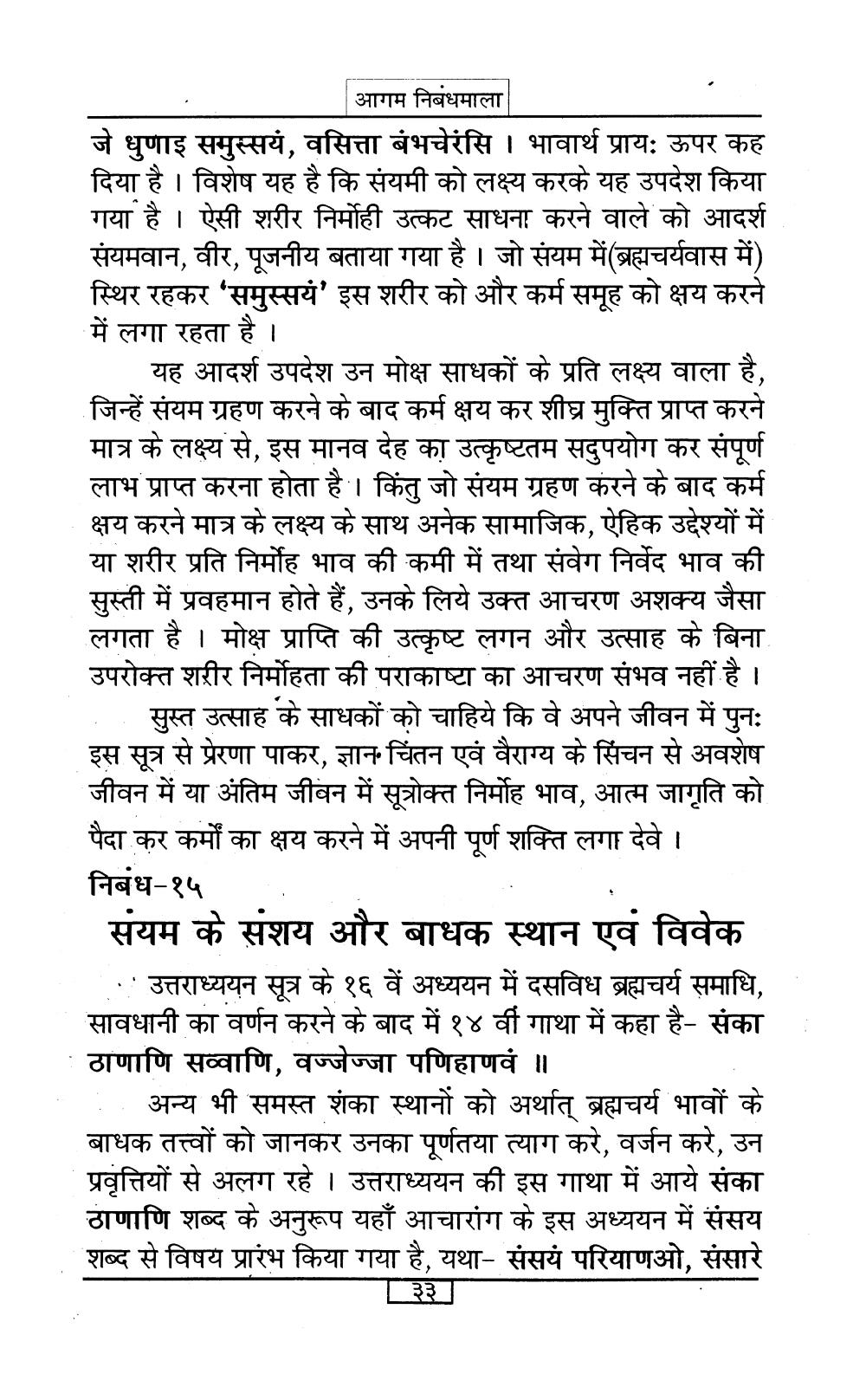________________ आगम निबंधमाला जे धुणाइ समुस्सयं, वसित्ता बंभचेरंसि / भावार्थ प्रायः ऊपर कह दिया है / विशेष यह है कि संयमी को लक्ष्य करके यह उपदेश किया गया है / ऐसी शरीर निर्मोही उत्कट साधना करने वाले को आदर्श संयमवान, वीर, पूजनीय बताया गया है / जो संयम में(ब्रह्मचर्यवास में) स्थिर रहकर 'समुस्सयं' इस शरीर को और कर्म समूह को क्षय करने में लगा रहता है। ___ यह आदर्श उपदेश उन मोक्ष साधकों के प्रति लक्ष्य वाला है, जिन्हें संयम ग्रहण करने के बाद कर्म क्षय कर शीघ्र मुक्ति प्राप्त करने मात्र के लक्ष्य से, इस मानव देह का उत्कृष्टतम सदुपयोग कर संपूर्ण लाभ प्राप्त करना होता है। किंतु जो संयम ग्रहण करने के बाद कर्म क्षय करने मात्र के लक्ष्य के साथ अनेक सामाजिक, ऐहिक उद्देश्यों में या शरीर प्रति निर्मोह भाव की कमी में तथा संवेग निर्वेद भाव की सुस्ती में प्रवहमान होते हैं, उनके लिये उक्त आचरण अशक्य जैसा लगता है / मोक्ष प्राप्ति की उत्कृष्ट लगन और उत्साह के बिना उपरोक्त शरीर निर्मोहता की पराकाष्टा का आचरण संभव नहीं है / . सुस्त उत्साह के साधकों को चाहिये कि वे अपने जीवन में पुनः इस सूत्र से प्रेरणा पाकर, ज्ञान चिंतन एवं वैराग्य के सिंचन से अवशेष जीवन में या अंतिम जीवन में सूत्रोक्त निर्मोह भाव, आत्म जागृति को पैदा कर कर्मों का क्षय करने में अपनी पूर्ण शक्ति लगा देवे / निबंध-१५ संयम के संशय और बाधक स्थान एवं विवेक * * उत्तराध्ययन सूत्र के 16 वें अध्ययन में दसविध ब्रह्मचर्य समाधि, सावधानी का वर्णन करने के बाद में 14 वीं गाथा में कहा है- संका ठाणाणि सव्वाणि, वज्जेज्जा पणिहाणवं // . अन्य भी समस्त शंका स्थानों को अर्थात् ब्रह्मचर्य भावों के बाधक तत्त्वों को जानकर उनका पूर्णतया त्याग करे, वर्जन करे, उन प्रवृत्तियों से अलग रहे / उत्तराध्ययन की इस गाथा में आये संका ठाणाणि शब्द के अनुरूप यहाँ आचारांग के इस अध्ययन में संसय शब्द से विषय प्रारंभ किया गया है, यथा- संसयं परियाणओ, संसारे