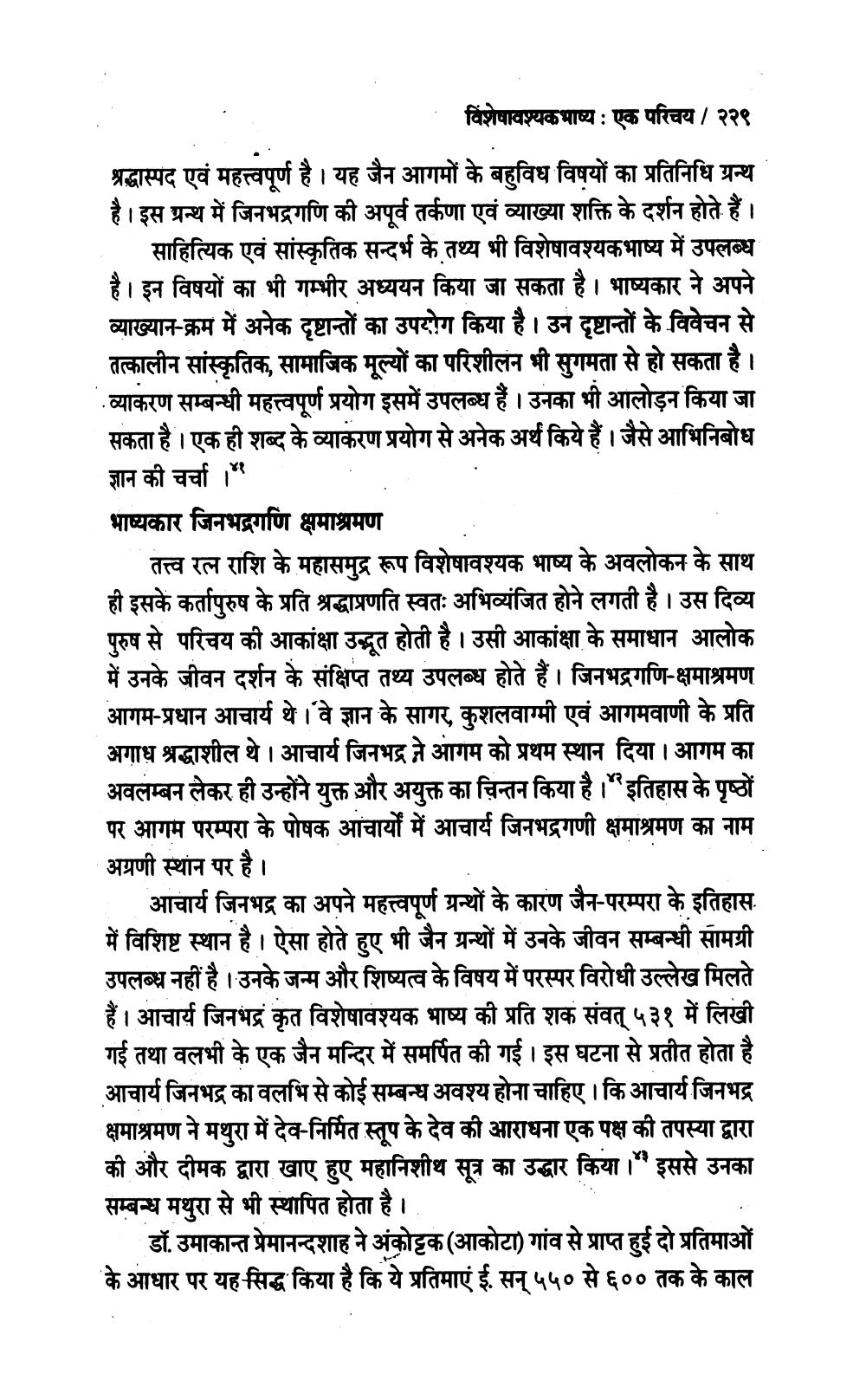________________ विशेषावश्यकभाष्य : एक परिचय | 229 श्रद्धास्पद एवं महत्त्वपूर्ण है। यह जैन आगमों के बहुविध विषयों का प्रतिनिधि ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में जिनभद्रगणि की अपूर्व तर्कणा एवं व्याख्या शक्ति के दर्शन होते हैं। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सन्दर्भ के तथ्य भी विशेषावश्यकभाष्य में उपलब्ध है। इन विषयों का भी गम्भीर अध्ययन किया जा सकता है। भाष्यकार ने अपने व्याख्यान-क्रम में अनेक दृष्टान्तों का उपयोग किया है। उन दृष्टान्तों के विवेचन से तत्कालीन सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्यों का परिशीलन भी सुगमता से हो सकता है। व्याकरण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रयोग इसमें उपलब्ध हैं / उनका भी आलोड़न किया जा सकता है / एक ही शब्द के व्याकरण प्रयोग से अनेक अर्थ किये हैं। जैसे आभिनिबोध ज्ञान की चर्चा / " भाष्यकार जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण तत्त्व रत्न राशि के महासमुद्र रूप विशेषावश्यक भाष्य के अवलोकन के साथ ही इसके कर्तापुरुष के प्रति श्रद्धाप्रणति स्वतः अभिव्यंजित होने लगती है। उस दिव्य पुरुष से परिचय की आकांक्षा उद्भूत होती है / उसी आकांक्षा के समाधान आलोक में उनके जीवन दर्शन के संक्षिप्त तथ्य उपलब्ध होते हैं। जिनभद्रगणि-क्षमाश्रमण आगम-प्रधान आचार्य थे। वे ज्ञान के सागर, कशलवाग्मी एवं आगमवाणी के प्रति अगाध श्रद्धाशील थे। आचार्य जिनभद्र ने आगम को प्रथम स्थान दिया। आगम का अवलम्बन लेकर ही उन्होंने युक्त और अयुक्त का चिन्तन किया है।" इतिहास के पृष्ठों पर आगम परम्परा के पोषक आचार्यों में आचार्य जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण का नाम अग्रणी स्थान पर है। ___ आचार्य जिनभद्र का अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के कारण जैन-परम्परा के इतिहास. में विशिष्ट स्थान है। ऐसा होते हुए भी जैन ग्रन्थों में उनके जीवन सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध नहीं है। उनके जन्म और शिष्यत्व के विषय में परस्पर विरोधी उल्लेख मिलते हैं। आचार्य जिनभद्रं कृत विशेषावश्यक भाष्य की प्रति शक संवत् 531 में लिखी गई तथा वलभी के एक जैन मन्दिर में समर्पित की गई। इस घटना से प्रतीत होता है आचार्य जिनभद्र का वलभि से कोई सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए। कि आचार्य जिनभद्र क्षमाश्रमण ने मथुरा में देव-निर्मित स्तूप के देव की आराधना एक पक्ष की तपस्या द्वारा की और दीमक द्वारा खाए हुए महानिशीथ सूत्र का उद्धार किया। इससे उनका सम्बन्ध मथुरा से भी स्थापित होता है। डॉ. उमाकान्त प्रेमानन्दशाह ने अंकोट्टक(आकोटा) गांव से प्राप्त हुई दो प्रतिमाओं के आधार पर यह सिद्ध किया है कि ये प्रतिमाएं ई. सन् 550 से 600 तक के काल