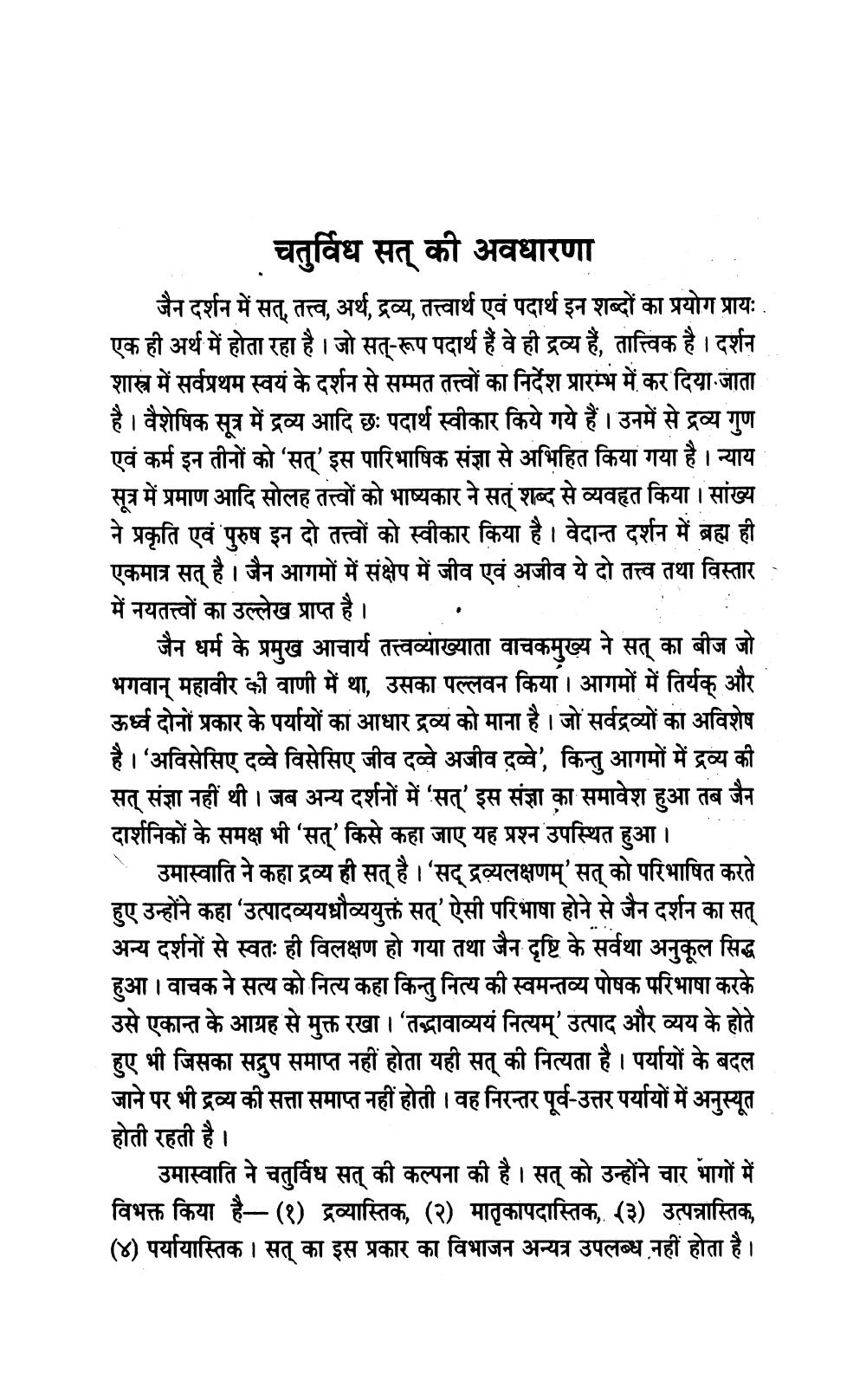________________ चतुर्विध सत् की अवधारणा जैन दर्शन में सत्, तत्त्व, अर्थ, द्रव्य, तत्त्वार्थ एवं पदार्थ इन शब्दों का प्रयोग प्रायः . एक ही अर्थ में होता रहा है / जो सत्-रूप पदार्थ हैं वे ही द्रव्य हैं, तात्त्विक है / दर्शन शास्त्र में सर्वप्रथम स्वयं के दर्शन से सम्मत तत्त्वों का निर्देश प्रारम्भ में कर दिया जाता है। वैशेषिक सूत्र में द्रव्य आदि छः पदार्थ स्वीकार किये गये हैं। उनमें से द्रव्य गुण एवं कर्म इन तीनों को 'सत्' इस पारिभाषिक संज्ञा से अभिहित किया गया है। न्याय सूत्र में प्रमाण आदि सोलह तत्त्वों को भाष्यकार ने सत् शब्द से व्यवहृत किया। सांख्य ने प्रकृति एवं पुरुष इन दो तत्त्वों को स्वीकार किया है। वेदान्त दर्शन में ब्रह्म ही एकमात्र सत् है / जैन आगमों में संक्षेप में जीव एवं अजीव ये दो तत्त्व तथा विस्तार में नयतत्त्वों का उल्लेख प्राप्त है। . जैन धर्म के प्रमुख आचार्य तत्त्वव्याख्याता वाचकमुख्य ने सत् का बीज जो भगवान् महावीर की वाणी में था, उसका पल्लवन किया। आगमों में तिर्यक् और ऊर्ध्व दोनों प्रकार के पर्यायों का आधार द्रव्य को माना है / जो सर्वद्रव्यों का अविशेष है। 'अविसेसिए दव्वे विसेसिए जीव दवे अजीव दवे, किन्तु आगमों में द्रव्य की सत् संज्ञा नहीं थी। जब अन्य दर्शनों में 'सत्' इस संज्ञा का समावेश हआ तब जैन दार्शनिकों के समक्ष भी 'सत्' किसे कहा जाए यह प्रश्न उपस्थित हुआ। उमास्वाति ने कहा द्रव्य ही सत् है / 'सद् द्रव्यलक्षणम्' सत् को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्' ऐसी परिभाषा होने से जैन दर्शन का सत् अन्य दर्शनों से स्वतः ही विलक्षण हो गया तथा जैन दृष्टि के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ। वाचक ने सत्य को नित्य कहा किन्तु नित्य की स्वमन्तव्य पोषक परिभाषा करके उसे एकान्त के आग्रह से मुक्त रखा। तद्भावाव्ययं नित्यम्' उत्पाद और व्यय के होते हुए भी जिसका सद्रुप समाप्त नहीं होता यही सत् की नित्यता है / पर्यायों के बदल जाने पर भी द्रव्य की सत्ता समाप्त नहीं होती / वह निरन्तर पूर्व-उत्तर पर्यायों में अनुस्यूत होती रहती है। उमास्वाति ने चतुर्विध सत् की कल्पना की है। सत् को उन्होंने चार भागों में विभक्त किया है- (1) द्रव्यास्तिक, (2) मातृकापदास्तिक, (3) उत्पन्नास्तिक, (4) पर्यायास्तिक / सत् का इस प्रकार का विभाजन अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता है।