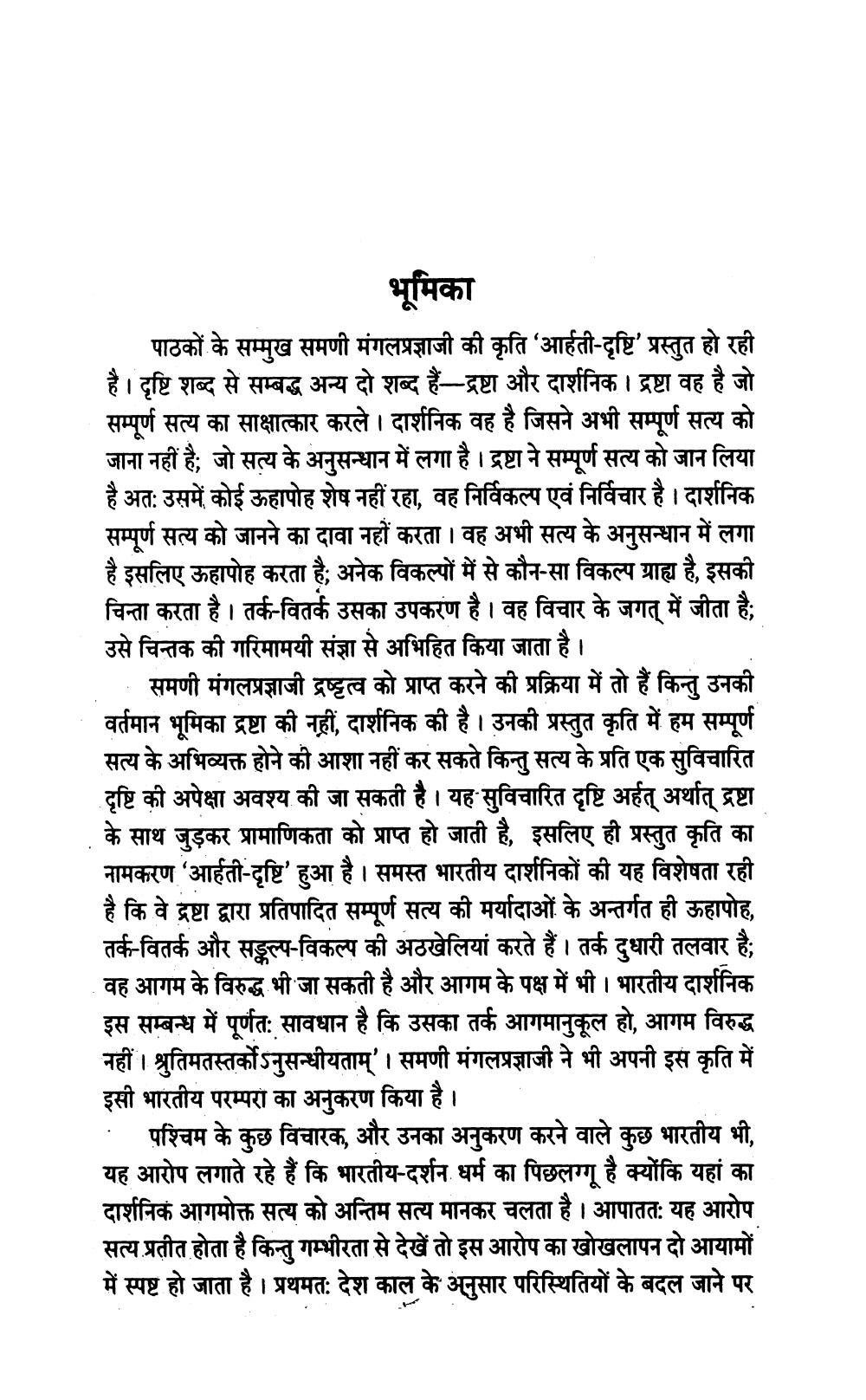________________ भूमिका पाठकों के सम्मुख समणी मंगलप्रज्ञाजी की कृति 'आर्हती-दृष्टि' प्रस्तुत हो रही है। दृष्टि शब्द से सम्बद्ध अन्य दो शब्द हैं-द्रष्टा और दार्शनिक / द्रष्टा वह है जो सम्पूर्ण सत्य का साक्षात्कार करले। दार्शनिक वह है जिसने अभी सम्पूर्ण सत्य को जाना नहीं है; जो सत्य के अनुसन्धान में लगा है / द्रष्टा ने सम्पूर्ण सत्य को जान लिया है अत: उसमें कोई ऊहापोह शेष नहीं रहा, वह निर्विकल्प एवं निर्विचार है / दार्शनिक सम्पूर्ण सत्य को जानने का दावा नहीं करता। वह अभी सत्य के अनुसन्धान में लगा है इसलिए ऊहापोह करता है; अनेक विकल्पों में से कौन-सा विकल्प ग्राह्य है, इसकी चिन्ता करता है। तर्क-वितर्क उसका उपकरण है / वह विचार के जगत् में जीता है; उसे चिन्तक की गरिमामयी संज्ञा से अभिहित किया जाता है। - समणी मंगलप्रज्ञाजी द्रष्टुत्व को प्राप्त करने की प्रक्रिया में तो हैं किन्तु उनकी वर्तमान भूमिका द्रष्टा की नहीं, दार्शनिक की है। उनकी प्रस्तुत कृति में हम सम्पूर्ण सत्य के अभिव्यक्त होने की आशा नहीं कर सकते किन्तु सत्य के प्रति एक सुविचारित दृष्टि की अपेक्षा अवश्य की जा सकती है। यह सुविचारित दृष्टि अर्हत् अर्थात् द्रष्टा के साथ जुड़कर प्रामाणिकता को प्राप्त हो जाती है, इसलिए ही प्रस्तुत कृति का नामकरण 'आर्हती-दृष्टि' हुआ है। समस्त भारतीय दार्शनिकों की यह विशेषता रही है कि वे द्रष्टा द्वारा प्रतिपादित सम्पूर्ण सत्य की मर्यादाओं के अन्तर्गत ही ऊहापोह, तर्क-वितर्क और सङ्कल्प-विकल्प की अठखेलियां करते हैं। तर्क दुधारी तलवार है; वह आगम के विरुद्ध भी जा सकती है और आगम के पक्ष में भी। भारतीय दार्शनिक इस सम्बन्ध में पूर्णत: सावधान है कि उसका तर्क आगमानुकूल हो, आगम विरुद्ध नहीं। श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम्' / समणी मंगलप्रज्ञाजी ने भी अपनी इस कृति में इसी भारतीय परम्परा का अनुकरण किया है। - पश्चिम के कुछ विचारक, और उनका अनुकरण करने वाले कुछ भारतीय भी, यह आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय-दर्शन धर्म का पिछलग्गू है क्योंकि यहां का दार्शनिकं आगमोक्त सत्य को अन्तिम सत्य मानकर चलता है। आपातत: यह आरोप सत्य प्रतीत होता है किन्तु गम्भीरता से देखें तो इस आरोप का खोखलापन दो आयामों में स्पष्ट हो जाता है। प्रथमत: देश काल के अनुसार परिस्थितियों के बदल जाने पर