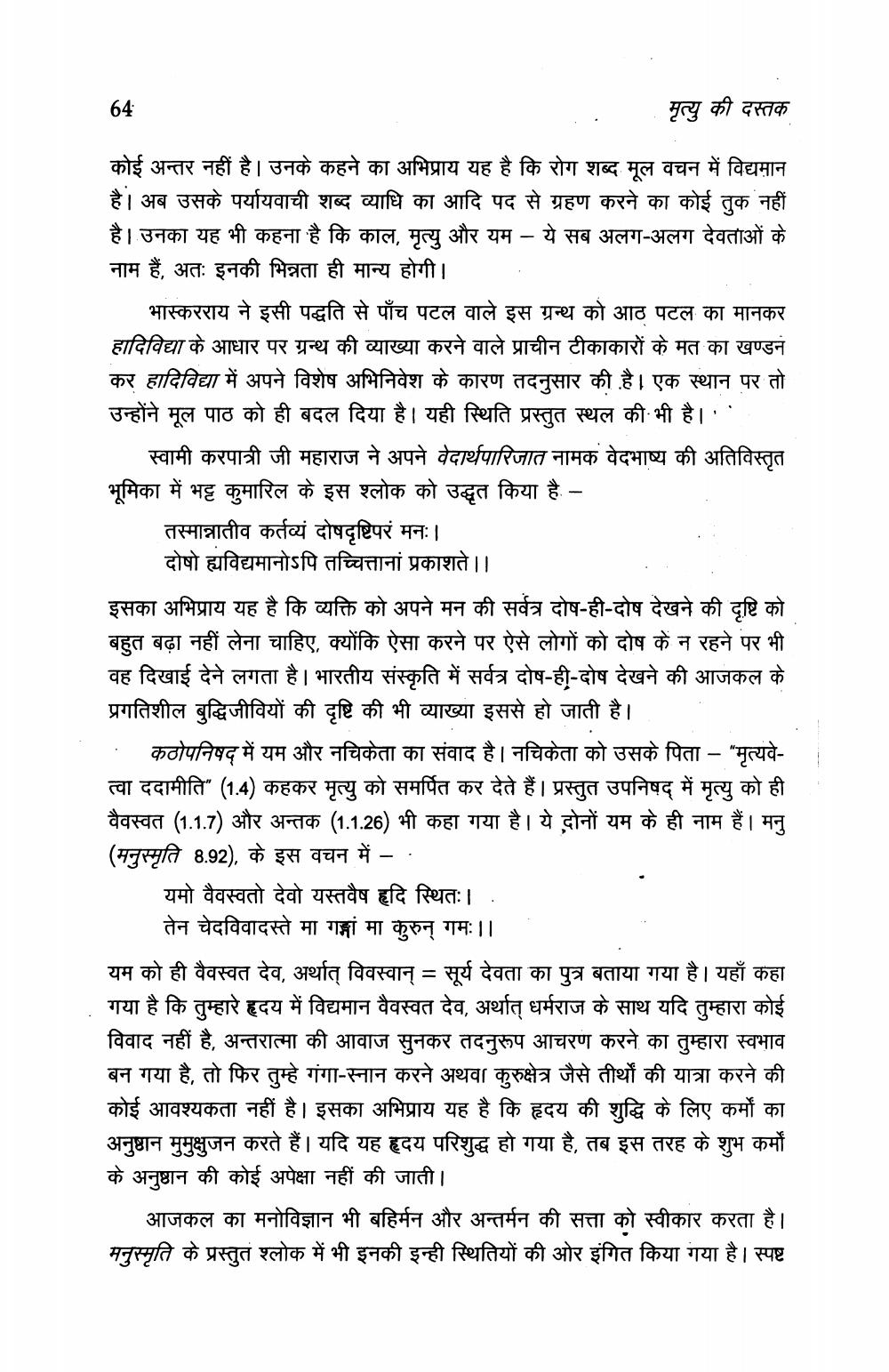________________ . मृत्यु की दस्तक कोई अन्तर नहीं है। उनके कहने का अभिप्राय यह है कि रोग शब्द मूल वचन में विद्यमान है। अब उसके पर्यायवाची शब्द व्याधि का आदि पद से ग्रहण करने का कोई तुक नहीं है। उनका यह भी कहना है कि काल, मृत्यु और यम - ये सब अलग-अलग देवताओं के नाम हैं, अतः इनकी भिन्नता ही मान्य होगी। भास्करराय ने इसी पद्धति से पाँच पटल वाले इस ग्रन्थ को आठ पटल का मानकर हादिविद्या के आधार पर ग्रन्थ की व्याख्या करने वाले प्राचीन टीकाकारों के मत का खण्डन कर हादिविद्या में अपने विशेष अभिनिवेश के कारण तदनुसार की है। एक स्थान पर तो उन्होंने मूल पाठ को ही बदल दिया है। यही स्थिति प्रस्तुत स्थल की भी है। '' स्वामी करपात्री जी महाराज ने अपने वेदार्थपारिजात नामक वेदभाष्य की अतिविस्तृत भूमिका में भट्ट कुमारिल के इस श्लोक को उद्धृत किया है - तस्मान्नातीव कर्तव्यं दोषदृष्टिपरं मनः / दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशते / / इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को अपने मन की सर्वत्र दोष-ही-दोष देखने की दृष्टि को बहुत बढ़ा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ऐसे लोगों को दोष के न रहने पर भी वह दिखाई देने लगता है। भारतीय संस्कृति में सर्वत्र दोष-ही-दोष देखने की आजकल के प्रगतिशील बुद्धिजीवियों की दृष्टि की भी व्याख्या इससे हो जाती है। कठोपनिषद् में यम और नचिकेता का संवाद है। नचिकेता को उसके पिता - “मृत्यवेत्वा ददामीति” (1.4) कहकर मृत्यु को समर्पित कर देते हैं। प्रस्तुत उपनिषद् में मृत्यु को ही वैवस्वत (1.1.7) और अन्तक (1.1.26) भी कहा गया है। ये दोनों यम के ही नाम हैं। मनु (मनुस्मृति 8.92), के इस वचन में - . यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः। . तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरुन् गमः / / यम को ही वैवस्वत देव, अर्थात् विवस्वान् = सूर्य देवता का पुत्र बताया गया है। यहाँ कहा गया है कि तुम्हारे हृदय में विद्यमान वैवस्वत देव, अर्थात् धर्मराज के साथ यदि तुम्हारा कोई विवाद नहीं है, अन्तरात्मा की आवाज सुनकर तदनुरूप आचरण करने का तुम्हारा स्वभाव बन गया है, तो फिर तुम्हे गंगा-स्नान करने अथवा कुरुक्षेत्र जैसे तीर्थों की यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि हृदय की शुद्धि के लिए कर्मों का अनुष्ठान मुमुक्षुजन करते हैं। यदि यह हृदय परिशुद्ध हो गया है, तब इस तरह के शुभ कर्मों के अनुष्ठान की कोई अपेक्षा नहीं की जाती। ___ आजकल का मनोविज्ञान भी बहिर्मन और अन्तर्मन की सत्ता को स्वीकार करता है। मनुस्मृति के प्रस्तुत श्लोक में भी इनकी इन्ही स्थितियों की ओर इंगित किया गया है। स्पष्ट