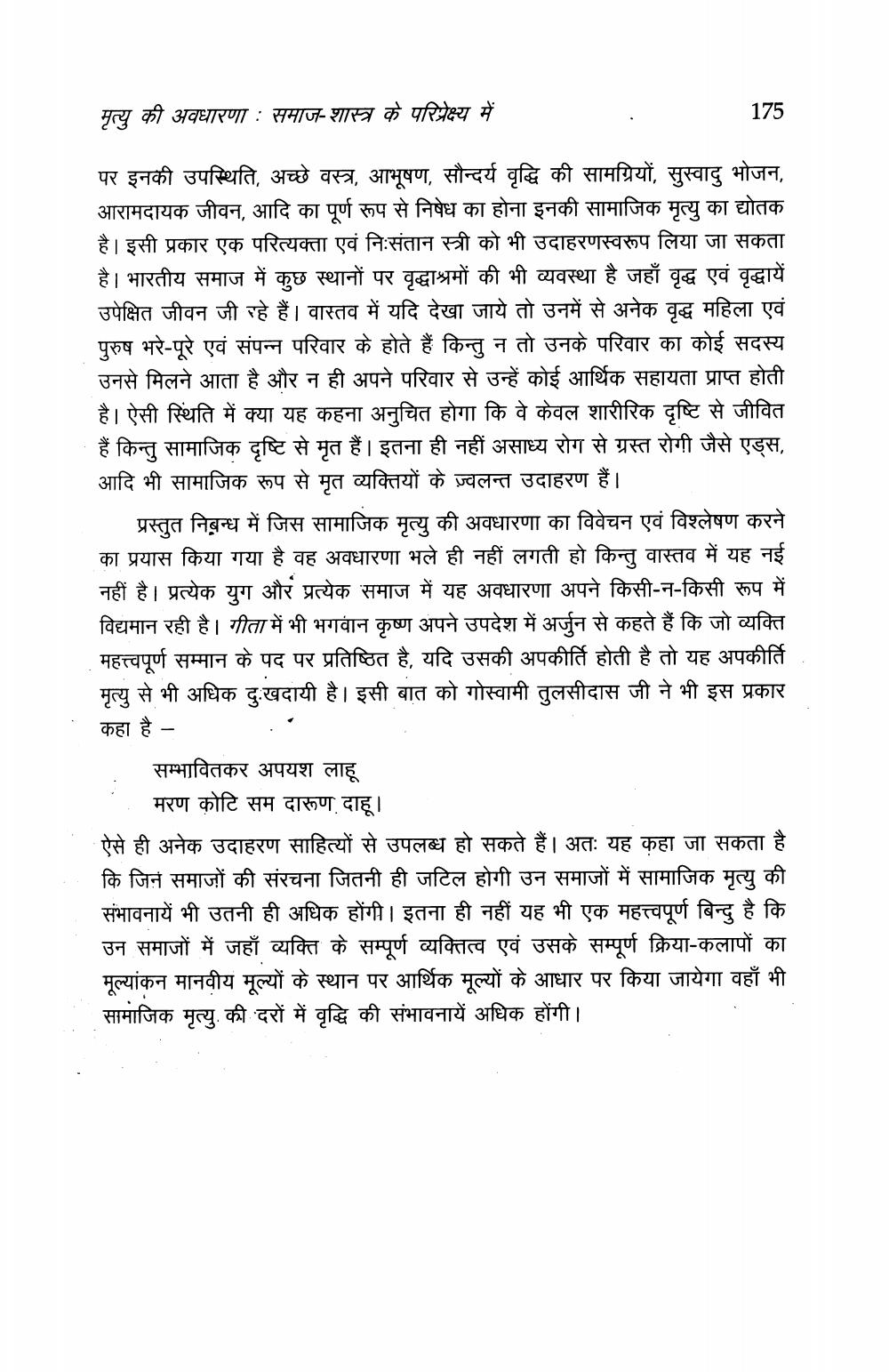________________ मृत्यु की अवधारणा : समाज-शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में 175 पर इनकी उपस्थिति, अच्छे वस्त्र, आभूषण, सौन्दर्य वृद्धि की सामग्रियों, सुस्वादु भोजन, आरामदायक जीवन, आदि का पूर्ण रूप से निषेध का होना इनकी सामाजिक मृत्यु का द्योतक है। इसी प्रकार एक परित्यक्ता एवं निःसंतान स्त्री को भी उदाहरणस्वरूप लिया जा सकता है। भारतीय समाज में कुछ स्थानों पर वृद्धाश्रमों की भी व्यवस्था है जहाँ वृद्ध एवं वृद्धायें उपेक्षित जीवन जी रहे हैं। वास्तव में यदि देखा जाये तो उनमें से अनेक वृद्ध महिला एवं पुरुष भरे-पूरे एवं संपन्न परिवार के होते हैं किन्तु न तो उनके परिवार का कोई सदस्य उनसे मिलने आता है और न ही अपने परिवार से उन्हें कोई आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में क्या यह कहना अनुचित होगा कि वे केवल शारीरिक दृष्टि से जीवित हैं किन्तु सामाजिक दृष्टि से मृत हैं। इतना ही नहीं असाध्य रोग से ग्रस्त रोगी जैसे एड्स, आदि भी सामाजिक रूप से मृत व्यक्तियों के ज्वलन्त उदाहरण हैं। प्रस्तुत निबन्ध में जिस सामाजिक मृत्यु की अवधारणा का विवेचन एवं विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है वह अवधारणा भले ही नहीं लगती हो किन्तु वास्तव में यह नई नहीं है। प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में यह अवधारणा अपने किसी-न-किसी रूप में विद्यमान रही है। गीता में भी भगवान कृष्ण अपने उपदेश में अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति महत्त्वपूर्ण सम्मान के पद पर प्रतिष्ठित है, यदि उसकी अपकीर्ति होती है तो यह अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक दुःखदायी है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस प्रकार कहा है - सम्भावितकर अपयश लाहू मरण कोटि सम दारूण दाहू। ऐसे ही अनेक उदाहरण साहित्यों से उपलब्ध हो सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि जिन समाजों की संरचना जितनी ही जटिल होगी उन समाजों में सामाजिक मृत्यु की संभावनायें भी उतनी ही अधिक होंगी। इतना ही नहीं यह भी एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु है कि उन समाजों में जहाँ व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं उसके सम्पूर्ण क्रिया-कलापों का मूल्यांकन मानवीय मूल्यों के स्थान पर आर्थिक मूल्यों के आधार पर किया जायेगा वहाँ भी सामाजिक मृत्यु. की दरों में वृद्धि की संभावनायें अधिक होंगी।