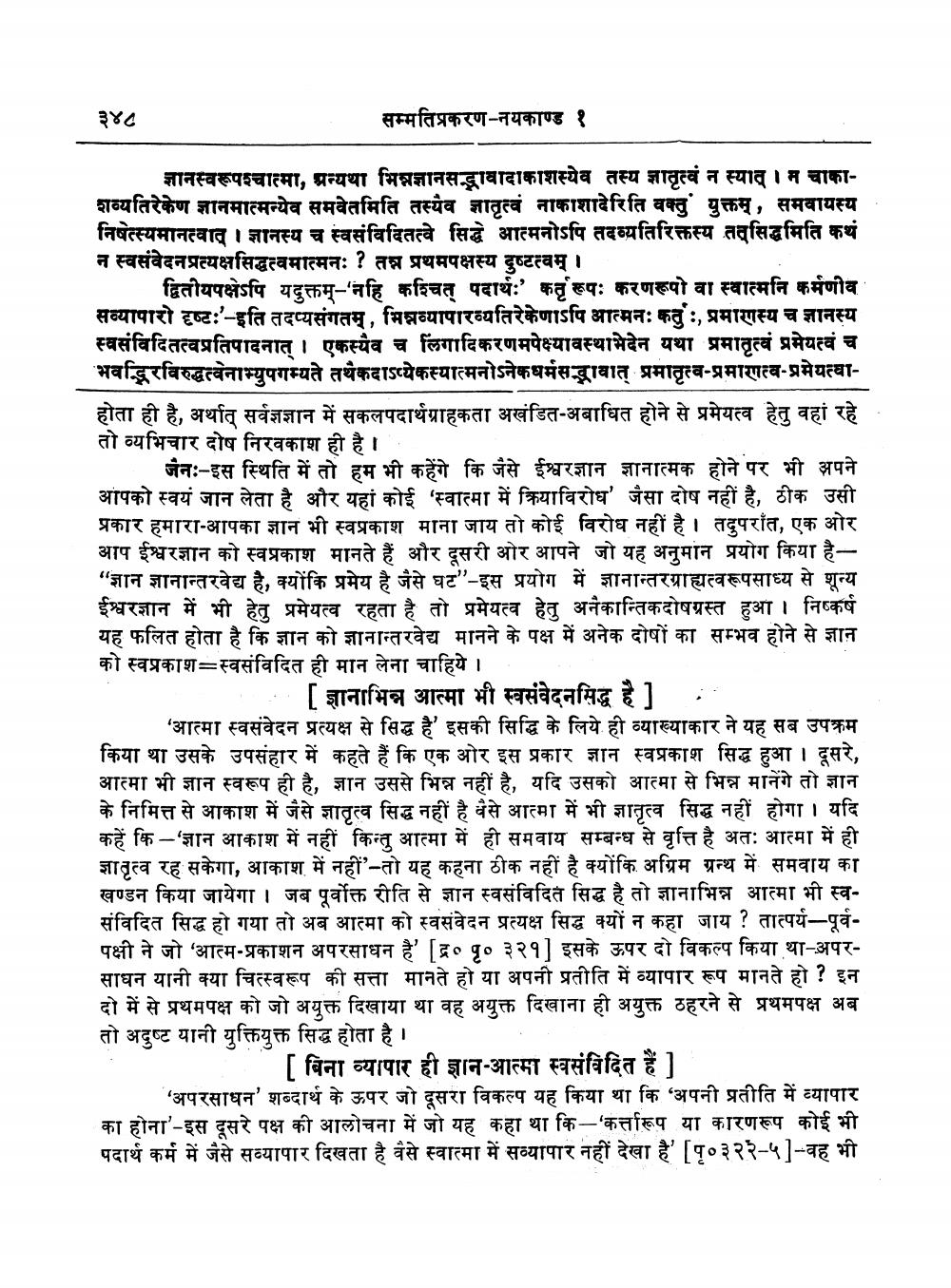________________ 348 सम्मतिप्रकरण-नयकाण्ड 1 ज्ञानस्वरूपश्चात्मा, अन्यथा भिन्नज्ञानसद्भावादाकाशस्येव तस्य ज्ञातृत्वं न स्यात् / म चाकाशव्यतिरेकेण ज्ञानमात्मन्येव समवेतमिति तस्यैव ज्ञातृत्वं नाकाशादेरिति वक्तु युक्तम् , समवायस्य निषेत्स्यमानत्वात् / ज्ञानस्य च स्वसंविदितत्वे सिद्धे आत्मनोऽपि तदव्यतिरिक्तस्य तदसिद्धमिति कथं न स्वसंवेदनप्रत्यक्षसिद्धत्वमात्मनः ? तन्न प्रथमपक्षस्य दुष्टत्वम्। द्वितीयपक्षेऽपि यदुक्तम्-'नहि कश्चित् पदार्थः' कर्तृरूपः करणरूपो वा स्वात्मनि कर्मणीव सव्यापारो दृष्टः' इति तदप्यसंगतम् , भिन्नव्यापारव्यतिरेकेणाऽपि आत्मनः कर्तुः, प्रमारणस्य च ज्ञानस्य स्वसंविदितत्वप्रतिपादनात् / एकस्यैव च लिंगादिकरणमपेक्ष्यावस्थाभेदेन यथा प्रमातृत्वं प्रमेयत्वं च भवद्भिरविरुद्धत्वेनाभ्युपगम्यते तथैकदाऽप्येकस्यात्मनोऽनेकधर्मसद्भावात् प्रमातृत्व-प्रमाणत्व-प्रमेयत्वाहोता ही है, अर्थात् सर्वज्ञज्ञान में सकलपदार्थग्राहकता अखंडित-अबाधित होने से प्रमेयत्व हेतु वहां रहे तो व्यभिचार दोष निरवकाश ही है। जैनः-इस स्थिति में तो हम भी कहेंगे कि जैसे ईश्वरज्ञान ज्ञानात्मक होने पर भी अपने आपको स्वयं जान लेता है और यहां कोई 'स्वात्मा में क्रियाविरोध' जैसा दोष नहीं है, ठीक उसी प्रकार हमारा-आपका ज्ञान भी स्वप्रकाश माना जाय तो कोई विरोध नहीं है। तदुपराँत, एक ओर आप ईश्वरज्ञान को स्वप्रकाश मानते हैं और दूसरी ओर आपने जो यह अनुमान प्रयोग किया है"ज्ञान ज्ञानान्तरवेद्य है, क्योंकि प्रमेय है जैसे घट"-इस प्रयोग में ज्ञानान्तरग्राह्यत्वरूपसाध्य से शून्य ईश्वरज्ञान में भी हेतु प्रमेयत्व रहता है तो प्रमेयत्व हेतु अनैकान्तिकदोषग्रस्त हुआ। निष्कर्ष यह फलित होता है कि ज्ञान को ज्ञानान्तरवेद्य मानने के पक्ष में अनेक दोषों का सम्भव होने से ज्ञान को स्वप्रकाश स्वसंविदित ही मान लेना चाहिये। . [ ज्ञानाभिन्न आत्मा भी स्वसंवेदनसिद्ध है ] 'आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से सिद्ध है' इसकी सिद्धि के लिये ही व्याख्याकार ने यह सब उपक्रम किया था उसके उपसंहार में कहते हैं कि एक ओर इस प्रकार ज्ञान स्वप्रकाश सिद्ध हुआ। दूसरे, आत्मा भी ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान उससे भिन्न नहीं है, यदि उसको आत्मा से भिन्न मानेंगे तो ज्ञान के निमित्त से आकाश में जैसे ज्ञातृत्व सिद्ध नहीं है वैसे आत्मा में भी ज्ञातृत्व सिद्ध नहीं होगा। यदि कहें कि - 'ज्ञान आकाश में नहीं किन्तु आत्मा में ही समवाय सम्बन्ध से वृत्ति है अत: आत्मा में ही ज्ञातृत्व रह सकेगा, आकाश में नहीं'-तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि अग्रिम ग्रन्थ में समवाय का खण्डन किया जायेगा। जब पूर्वोक्त रीति से ज्ञान स्वसंविदित सिद्ध है तो ज्ञानाभिन्न आत्मा भी स्वसंविदित सिद्ध हो गया तो अब आत्मा को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष सिद्ध क्यों न कहा जाय ? तात्पर्य-पूर्वपक्षी ने जो 'आत्म-प्रकाशन अपरसाधन है' [द्र०१० 321] इसके ऊपर दो विकल्प किया था-अपरसाधन यानी क्या चित्स्वरूप की सत्ता मानते हो या अपनी प्रतीति में व्यापार रूप मानते हो? इन दो में से प्रथमपक्ष को जो अयुक्त दिखाया था वह अयुक्त दिखाना ही अयुक्त ठहरने से प्रथमपक्ष अब तो अदुष्ट यानी युक्तियुक्त सिद्ध होता है / [विना व्यापार ही ज्ञान-आत्मा स्वसंविदित हैं ] 'अपरसाधन' शब्दार्थ के ऊपर जो दूसरा विकल्प यह किया था कि 'अपनी प्रतीति में व्यापार का होना'-इस दूसरे पक्ष की आलोचना में जो यह कहा था कि-'कर्त्तारूप या कारणरूप कोई भी पदार्थ कर्म में जैसे सव्यापार दिखता है वैसे स्वात्मा में सव्यापार नहीं देखा है' [पृ०३२२-५]-वह भी