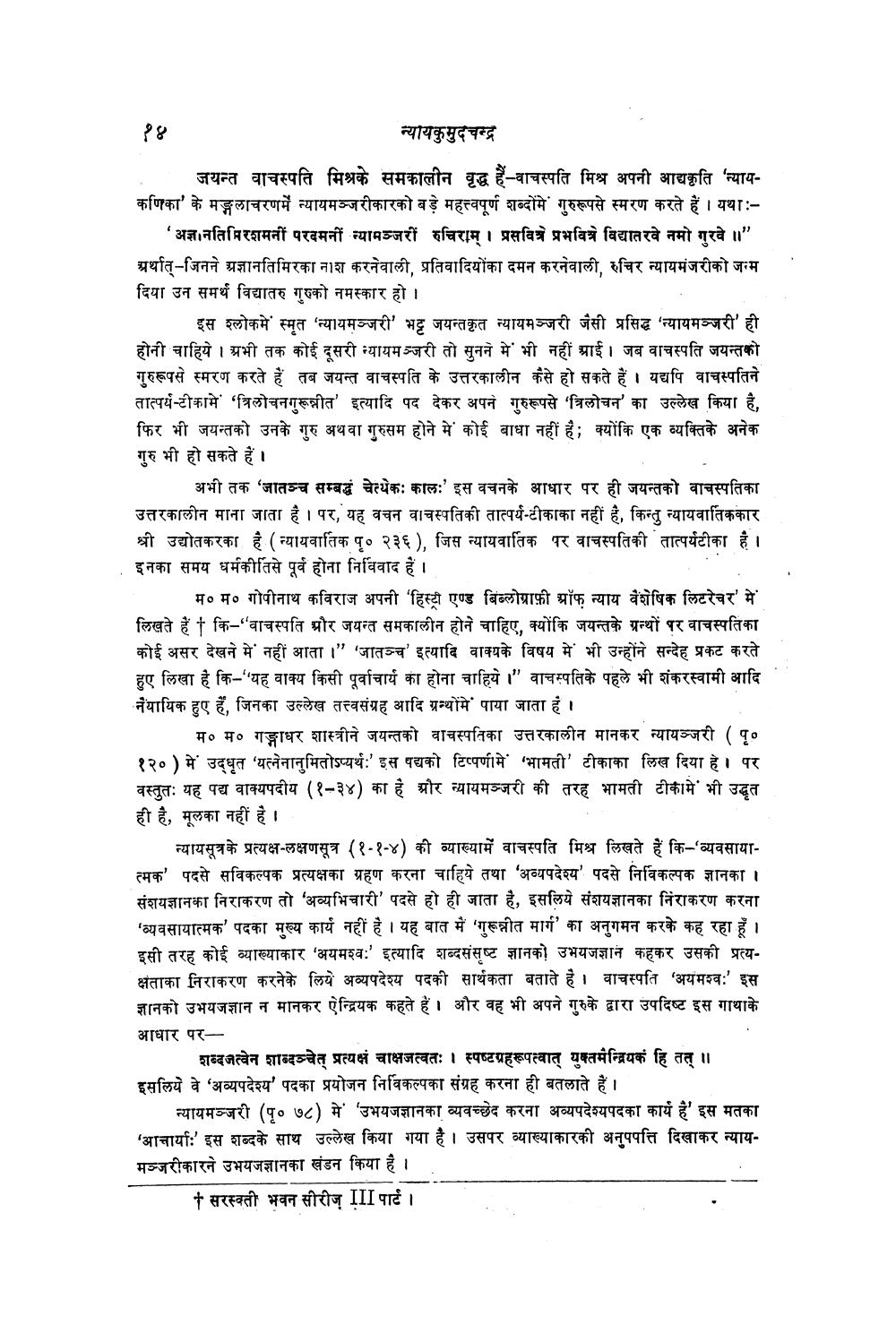________________ न्यायकुमुदचन्द्र जयन्त वाचस्पति मिश्रके समकालीन वृद्ध हैं-वाचस्पति मिश्र अपनी आद्यकृति 'न्यायकणिका' के मङ्गलाचरणमें न्यायमञ्जरीकारको बड़े महत्त्वपूर्ण शब्दोंमे गुरुरूपसे स्मरण करते हैं / यथा: 'अज्ञानतिमिरशमनी परदमनी न्यामञ्जरी रुचिराम / प्रसवित्रे प्रभवित्र विद्यातरवे नमो गुरवे // " अर्थात्-जिनने अज्ञानतिमिरका नाश करनेवाली, प्रतिवादियोंका दमन करनेवाली, रुचिर न्यायमंजरीको जन्म दिया उन समर्थ विद्यातरु गुरुको नमस्कार हो। इस श्लोकमे स्मृत 'न्यायमञ्जरी' भट्ट जयन्तकृत न्यायमञ्जरी जैसी प्रसिद्ध 'न्यायमञ्जरी' ही होनी चाहिये / अभी तक कोई दूसरी न्यायमञ्जरी तो सुनने में भी नहीं आई। जब वाचस्पति जयन्तको गुरुरूपसे स्मरण करते हैं तब जयन्त वाचस्पति के उत्तरकालीन कैसे हो सकते हैं। यद्यपि वाचस्पतिने तात्पर्य-टीकामे 'त्रिलोचनगुरून्नीत' इत्यादि पद देकर अपने गुरुरूपसे 'त्रिलोचन' का उल्लेख किया है, फिर भी जयन्तको उनके गुरु अथवा गुरुसम होने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि एक व्यक्तिके अनेक गुरु भी हो सकते हैं। अभी तक 'जातञ्च सम्बद्धं चेत्येकः कालः' इस वचनके आधार पर ही जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकालीन माना जाता है। पर, यह वचन वाचस्पतिकी तात्पर्य-टीकाका नहीं है, किन्तु न्यायवार्तिककार श्री उद्योतकरका है (न्यायवार्तिक पृ० 236 ), जिस न्यायवार्तिक पर वाचस्पतिकी तात्पर्यटीका है। इनका समय धर्मकीतिसे पूर्व होना निर्विवाद हैं / म०म० गोपीनाथ कविराज अपनी 'हिस्टी एण्ड बिब्लोग्राफ़ी ऑफ न्याय वैशेषिक लिटरेचर' में लिखते हैं कि-"वाचस्पति और जयन्त समकालीन होने चाहिए, क्योंकि जयन्तके ग्रन्थों पर वाचस्पतिका कोई असर देखने में नहीं आता।" 'जातञ्च' इत्यादि वाक्यके विषय में भी उन्होंने सन्देह प्रकट करते हए लिखा है कि-'यह वाक्य किसी पूर्वाचार्य का होना चाहिये।" वाचस्पतिके पहले भी शंकरस्वामी आदि नैयायिक हुए हैं, जिनका उल्लेख तत्त्वसंग्रह आदि ग्रन्थोंमें पाया जाता है। म. म. गङ्गाधर शास्त्रीने जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकालीन मानकर न्यायञ्जरी ( 10 120) में उद्धृत 'यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः' इस पद्यको टिप्पणीमें भामती' टीकाका लिख दिया है। पर वस्तुतः यह पद्य वाक्यपदीय (1-34) का है और न्यायमञ्जरी की तरह भामती टीकामे भी उद्धृत ही है, मूलका नहीं है। न्यायसूत्र के प्रत्यक्ष-लक्षणसूत्र (1-1-4) की व्याख्यामें वाचस्पति मिश्र लिखते हैं कि-'व्यवसायात्मक' पदसे सविकल्पक प्रत्यक्षका ग्रहण करना चाहिये तथा 'अव्यपदेश्य' पदसे निर्विकल्पक ज्ञानका / संशयज्ञानका निराकरण तो 'अव्यभिचारी' पदसे हो ही जाता है, इसलिये संशयज्ञानका निराकरण करना 'व्यवसायात्मक' पदका मुख्य कार्य नहीं है / यह बात मैं 'गुरून्नीत मार्ग' का अनुगमन करके कह रहा हूँ। इसी तरह कोई व्याख्याकार 'अयमश्वः' इत्यादि शब्दसंसष्ट ज्ञानको उभयजज्ञान कहकर उसकी प्रत्यक्षताका निराकरण करनेके लिये अव्यपदेश्य पदकी सार्थकता बताते है। वाचस्पति 'अयमश्व:' इस ज्ञानको उभयजज्ञान न मानकर ऐन्द्रियक कहते हैं। और वह भी अपने गुरुके द्वारा उपदिष्ट इस गाथाके आधार पर शब्दजत्वेन शाब्दञ्चेत् प्रत्यक्षं चाक्षजत्वतः / स्पष्टग्रहरूपत्वात् युक्तमन्द्रियकं हि तत् / / इसलिये वे 'अव्यपदेश्य पदका प्रयोजन निर्विकल्पका संग्रह करना ही बतलाते हैं। न्यायमञ्जरी (पृ० 78) में 'उभयजज्ञानका व्यवच्छेद करना अव्यपदेश्यपदका कार्य है' इस मतका 'आचार्याः' इस शब्दके साथ उल्लेख किया गया है। उसपर व्याख्याकारकी अनुपपत्ति दिखाकर न्यायमञ्जरीकारने उभयजज्ञानका खंडन किया है। + सरस्वती भवन सीरीज़ III पार्ट /