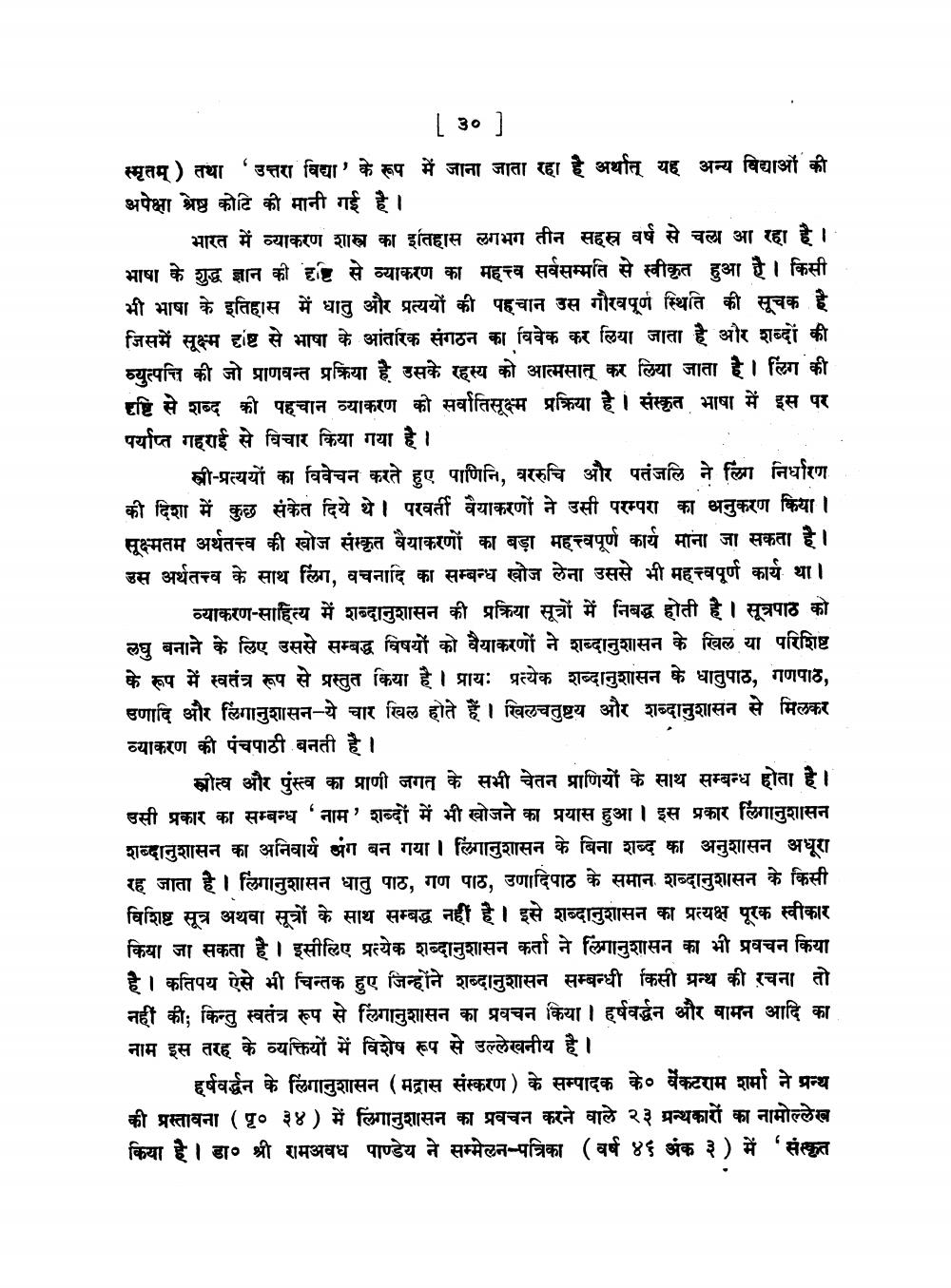________________ [ 30 ] स्मृतम्) तथा 'उत्तरा विद्या' के रूप में जाना जाता रहा है अर्थात् यह अन्य विद्याओं की अपेक्षा श्रेष्ठ कोटि की मानी गई है। भारत में व्याकरण शास्त्र का इतिहास लगभग तीन सहस्र वर्ष से चला आ रहा है। भाषा के शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से व्याकरण का महत्त्व सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ है। किसी भी भाषा के इतिहास में धातु और प्रत्ययों की पहचान उस गौरवपूर्ण स्थिति की सूचक है जिसमें सूक्ष्म दृष्टि से भाषा के आंतरिक संगठन का विवेक कर लिया जाता है और शब्दों की व्युत्पत्ति की जो प्राणवन्त प्रक्रिया है उसके रहस्य को आत्मसात् कर लिया जाता है। लिंग की दृष्टि से शब्द को पहचान व्याकरण को सर्वातिसूक्ष्म प्रक्रिया है। संस्कृत भाषा में इस पर पर्याप्त गहराई से विचार किया गया है। स्त्री-प्रत्ययों का विवेचन करते हुए पाणिनि, वररुचि और पतंजलि ने लिंग निर्धारण की दिशा में कुछ संकेत दिये थे। परवर्ती वैयाकरणों ने उसी परम्परा का अनुकरण किया / सूक्ष्मतम अर्थतत्त्व की खोज संस्कृत वैयाकरणों का बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य माना जा सकता है। उस अर्थतत्व के साथ लिंग, वचनादि का सम्बन्ध खोज लेना उससे भी महत्त्वपूर्ण कार्य था। व्याकरण-साहित्य में शब्दानुशासन की प्रक्रिया सूत्रों में निबद्ध होती है। सूत्रपाठ को लघु बनाने के लिए उससे सम्बद्ध विषयों को वैयाकरणों ने शब्दानुशासन के खिल या परिशिष्ट के रूप में स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया है। प्रायः प्रत्येक शब्दानुशासन के धातुपाठ, गणपाठ, उणादि और लिंगानुशासन-ये चार खिल होते हैं। खिलचतुष्टय और शब्दानुशासन से मिलकर व्याकरण की पंचपाठी बनती है। स्रीत्व और पुंस्त्व का प्राणी जगत के सभी चेतन प्राणियों के साथ सम्बन्ध होता है। उसी प्रकार का सम्बन्ध 'नाम' शब्दों में भी खोजने का प्रयास हुआ। इस प्रकार लिंगानुशासन शब्दानुशासन का अनिवार्य अंग बन गया। लिंगानुशासन के बिना शब्द का अनुशासन अधूरा रह जाता है / लिंगानुशासन धातु पाठ, गण पाठ, उणादिपाठ के समान शब्दानुशासन के किसी विशिष्ट सूत्र अथवा सूत्रों के साथ सम्बद्ध नहीं है। इसे शब्दानुशासन का प्रत्यक्ष पूरक स्वीकार किया जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक शब्दानुशासन कर्ता ने लिंगानुशासन का भी प्रवचन किया है। कतिपय ऐसे भी चिन्तक हुए जिन्होंने शब्दानुशासन सम्बन्धी किसी ग्रन्थ की रचना तो नहीं की; किन्तु स्वतंत्र रूप से लिंगानुशासन का प्रवचन किया। हर्षवर्धन और वामन आदि का नाम इस तरह के व्यक्तियों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हर्षवर्द्धन के लिंगानुशासन (मद्रास संस्करण ) के सम्पादक के० वेंकटराम शर्मा ने प्रन्थ की प्रस्तावना (पृ० 34) में लिंगानुशासन का प्रवचन करने वाले 23 ग्रन्थकारों का नामोल्लेख किया है। डा. श्री रामअवध पाण्डेय ने सम्मेलन-पत्रिका (वर्ष 46 अंक 3) में 'संस्कृत