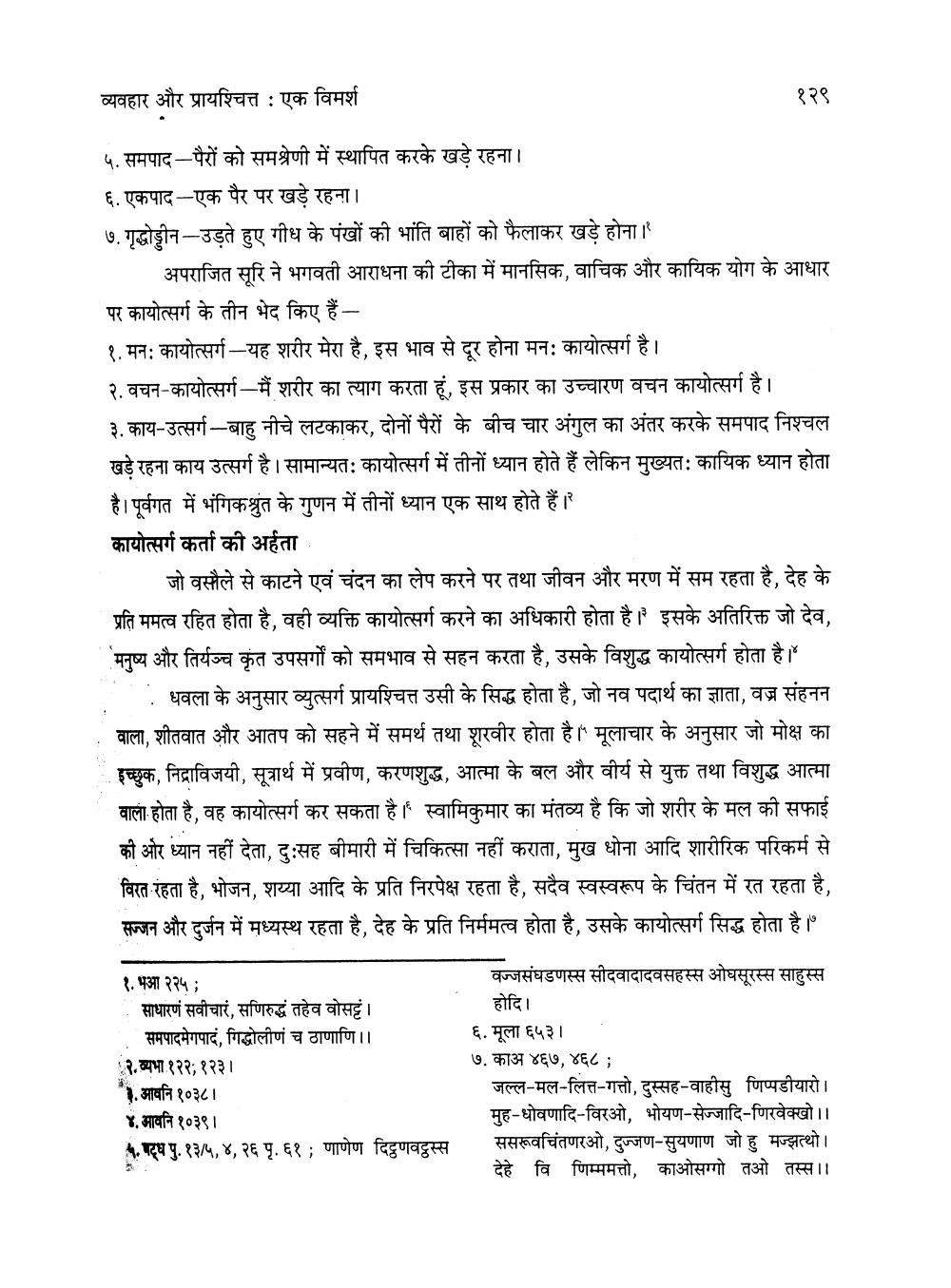________________ व्यवहार और प्रायश्चित्त : एक विमर्श 129 5. समपाद-पैरों को समश्रेणी में स्थापित करके खड़े रहना। 6. एकपाद -एक पैर पर खड़े रहना। 7. गृद्धोड्डीन-उड़ते हुए गीध के पंखों की भांति बाहों को फैलाकर खड़े होना। अपराजित सूरि ने भगवती आराधना की टीका में मानसिक, वाचिक और कायिक योग के आधार पर कायोत्सर्ग के तीन भेद किए हैं - 1. मनः कायोत्सर्ग-यह शरीर मेरा है, इस भाव से दूर होना मनः कायोत्सर्ग है। 2. वचन-कायोत्सर्ग-मैं शरीर का त्याग करता हूं, इस प्रकार का उच्चारण वचन कायोत्सर्ग है। 3. काय-उत्सर्ग-बाहु नीचे लटकाकर, दोनों पैरों के बीच चार अंगुल का अंतर करके समपाद निश्चल खड़े रहना काय उत्सर्ग है। सामान्यतः कायोत्सर्ग में तीनों ध्यान होते हैं लेकिन मुख्यतः कायिक ध्यान होता है। पूर्वगत में भंगिकश्रृंत के गुणन में तीनों ध्यान एक साथ होते हैं। कायोत्सर्ग कर्ता की अर्हता जो वसौले से काटने एवं चंदन का लेप करने पर तथा जीवन और मरण में सम रहता है, देह के प्रति ममत्व रहित होता है, वही व्यक्ति कायोत्सर्ग करने का अधिकारी होता है। इसके अतिरिक्त जो देव, मनुष्य और तिर्यञ्च कृत उपसर्गों को समभाव से सहन करता है, उसके विशुद्ध कायोत्सर्ग होता है।' . धवला के अनुसार व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त उसी के सिद्ध होता है, जो नव पदार्थ का ज्ञाता, वज्र संहनन वाला, शीतवात और आतप को सहने में समर्थ तथा शूरवीर होता है। मूलाचार के अनुसार जो मोक्ष का इच्छुक, निद्राविजयी, सूत्रार्थ में प्रवीण, करणशुद्ध, आत्मा के बल और वीर्य से युक्त तथा विशुद्ध आत्मा वाला होता है, वह कायोत्सर्ग कर सकता है। स्वामिकुमार का मंतव्य है कि जो शरीर के मल की सफाई की ओर ध्यान नहीं देता, दुःसह बीमारी में चिकित्सा नहीं कराता, मुख धोना आदि शारीरिक परिकर्म से विरत रहता है, भोजन, शय्या आदि के प्रति निरपेक्ष रहता है, सदैव स्वस्वरूप के चिंतन में रत रहता है, सज्जन और दुर्जन में मध्यस्थ रहता है, देह के प्रति निर्ममत्व होता है, उसके कायोत्सर्ग सिद्ध होता है।' 1. भआ 225%, साधारणं सवीचारं, सणिरुद्धं तहेव वोसट्टं। समपादमेगपाद, गिद्धोलीणं च ठाणाणि।। 22. व्यभा 122; 123 / आवनि 1038 / ४.आवनि 1039 / ६.पट्ध पु. 13/5,4, 26 पृ.६१; णाणेण दिगुणवट्ठस्स वज्जसंघडणस्स सीदवादादवसहस्स ओघसूरस्स साहुस्स होदि। 6. मूला 653 / 7. काअ 467, 468; जल्ल-मल-लित्त-गत्तो, दुस्सह-वाहीसु णिप्पडीयारो। मुह-धोवणादि-विरओ, भोयण-सेज्जादि-णिरवेक्खो।। ससरूवचिंतणरओ, दुज्जण-सुयणाण जो हु मज्झत्थो। देहे वि णिम्ममत्तो, काओसग्गो तओ तस्स / /