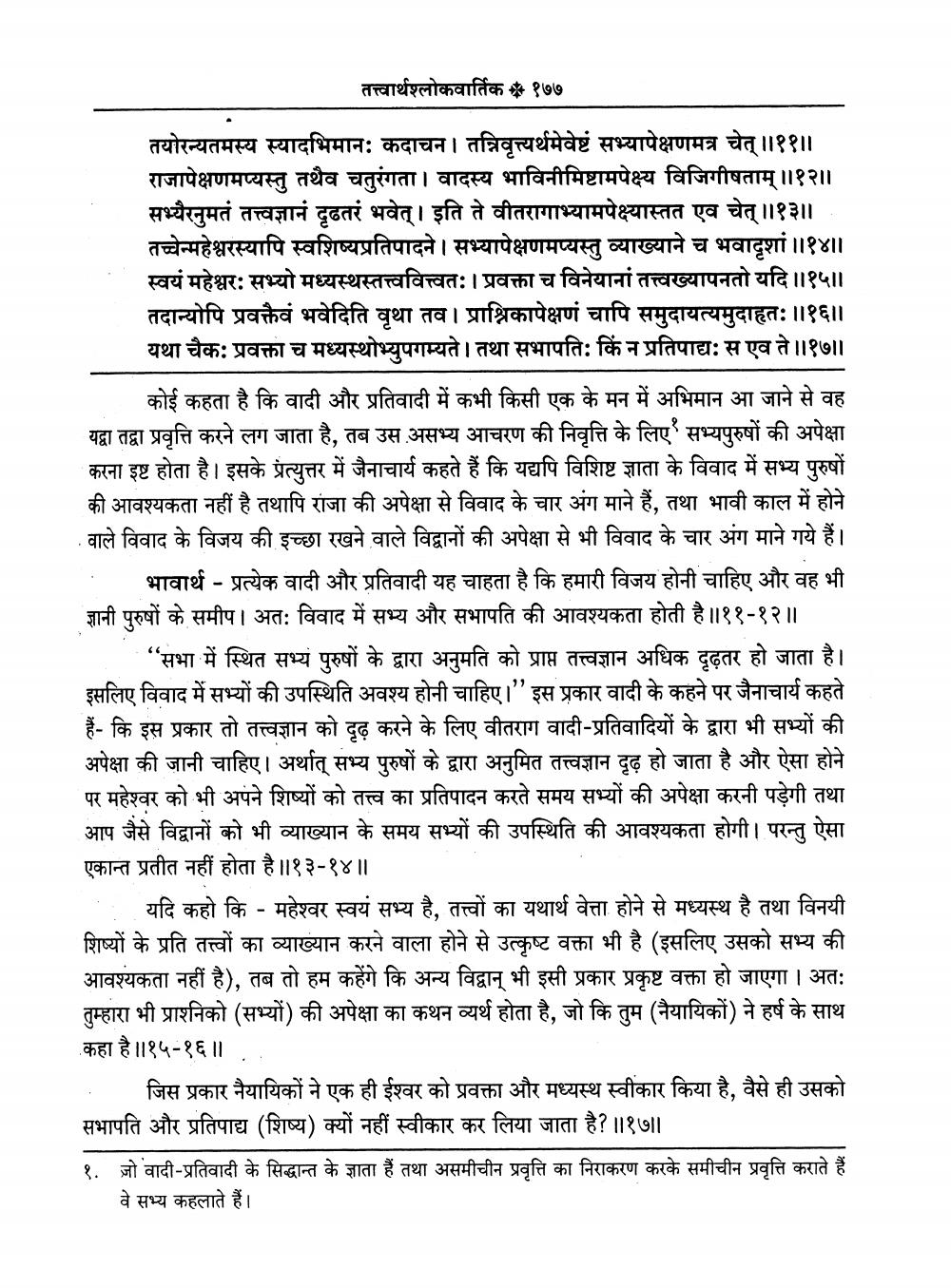________________ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक 177 तयोरन्यतमस्य स्यादभिमानः कदाचन। तन्निवृत्त्यर्थमेवेष्टं सभ्यापेक्षणमत्र चेत् // 11 // राजापेक्षणमप्यस्तु तथैव चतुरंगता। वादस्य भाविनीमिष्टामपेक्ष्य विजिगीषताम् // 12 // सभ्यैरनुमतं तत्त्वज्ञानं दृढतरं भवेत् / इति ते वीतरागाभ्यामपेक्ष्यास्तत एव चेत् // 13 // तच्चेन्महेश्वरस्यापि स्वशिष्यप्रतिपादने / सभ्यापेक्षणमप्यस्तु व्याख्याने च भवादृशां // 14 // स्वयं महेश्वरः सभ्यो मध्यस्थस्तत्त्ववित्त्वतः। प्रवक्ता च विनेयानां तत्त्वख्यापनतो यदि // 15 // तदान्योपि प्रवक्तैवं भवेदिति वृथा तव। प्राश्निकापेक्षणं चापि समुदायत्यमुदाहृतः॥१६॥ यथा चैकः प्रवक्ता च मध्यस्थोभ्युपगम्यते। तथा सभापति: किं न प्रतिपाद्यः स एव ते॥१७॥ कोई कहता है कि वादी और प्रतिवादी में कभी किसी एक के मन में अभिमान आ जाने से वह यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करने लग जाता है, तब उस असभ्य आचरण की निवृत्ति के लिए सभ्यपुरुषों की अपेक्षा करना इष्ट होता है। इसके प्रत्युत्तर में जैनाचार्य कहते हैं कि यद्यपि विशिष्ट ज्ञाता के विवाद में सभ्य पुरुषों की आवश्यकता नहीं है तथापि राजा की अपेक्षा से विवाद के चार अंग माने हैं, तथा भावी काल में होने वाले विवाद के विजय की इच्छा रखने वाले विद्वानों की अपेक्षा से भी विवाद के चार अंग माने गये हैं। - भावार्थ - प्रत्येक वादी और प्रतिवादी यह चाहता है कि हमारी विजय होनी चाहिए और वह भी ज्ञानी पुरुषों के समीप। अतः विवाद में सभ्य और सभापति की आवश्यकता होती है॥११-१२॥ “सभा में स्थित सभ्यं पुरुषों के द्वारा अनुमति को प्राप्त तत्त्वज्ञान अधिक दृढ़तर हो जाता है। इसलिए विवाद में सभ्यों की उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए।" इस प्रकार वादी के कहने पर जैनाचार्य कहते हैं- कि इस प्रकार तो तत्त्वज्ञान को दृढ़ करने के लिए वीतराग वादी-प्रतिवादियों के द्वारा भी सभ्यों की अपेक्षा की जानी चाहिए। अर्थात् सभ्य पुरुषों के द्वारा अनुमित तत्त्वज्ञान दृढ़ हो जाता है और ऐसा होने पर महेश्वर को भी अपने शिष्यों को तत्त्व का प्रतिपादन करते समय सभ्यों की अपेक्षा करनी पड़ेगी तथा आप जैसे विद्वानों को भी व्याख्यान के समय सभ्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होगी। परन्तु ऐसा एकान्त प्रतीत नहीं होता है॥१३-१४ // यदि कहो कि - महेश्वर स्वयं सभ्य है, तत्त्वों का यथार्थ वेत्ता होने से मध्यस्थ है तथा विनयी शिष्यों के प्रति तत्त्वों का व्याख्यान करने वाला होने से उत्कृष्ट वक्ता भी है (इसलिए उसको सभ्य की आवश्यकता नहीं है), तब तो हम कहेंगे कि अन्य विद्वान् भी इसी प्रकार प्रकृष्ट वक्ता हो जाएगा / अत: तुम्हारा भी प्राशनको (सभ्यों) की अपेक्षा का कथन व्यर्थ होता है, जो कि तुम (नैयायिकों) ने हर्ष के साथ कहा है।।१५-१६॥ .. जिस प्रकार नैयायिकों ने एक ही ईश्वर को प्रवक्ता और मध्यस्थ स्वीकार किया है, वैसे ही उसको सभापति और प्रतिपाद्य (शिष्य) क्यों नहीं स्वीकार कर लिया जाता है? // 17 // 1. जो वादी-प्रतिवादी के सिद्धान्त के ज्ञाता हैं तथा असमीचीन प्रवृत्ति का निराकरण करके समीचीन प्रवृत्ति कराते हैं वे सभ्य कहलाते हैं।