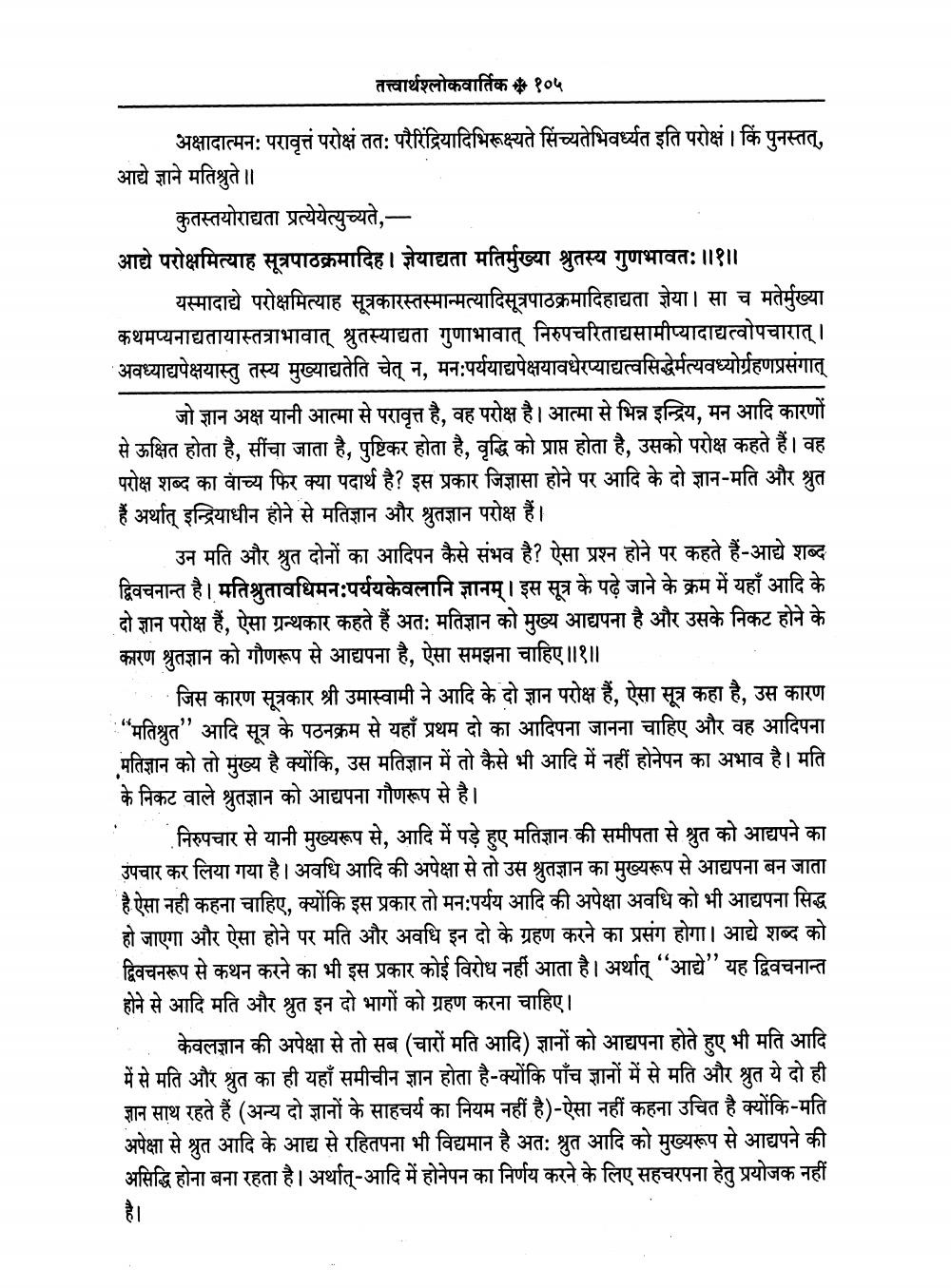________________ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक * 105 अक्षादात्मनः परावृत्तं परोक्षं ततः परैरिंद्रियादिभिरूक्ष्यते सिंच्यतेभिवर्ध्यत इति परोक्षं / किं पुनस्तत्, आद्ये ज्ञाने मतिश्रुते॥ कुतस्तयोराद्यता प्रत्येयेत्युच्यते,आद्ये परोक्षमित्याह सूत्रपाठक्रमादिह। ज्ञेयाद्यता मतिर्मुख्या श्रुतस्य गुणभावतः॥१॥ यस्मादाद्ये परोक्षमित्याह सूत्रकारस्तस्मान्मत्यादिसूत्रपाठक्रमादिहाद्यता ज्ञेया। सा च मतेर्मुख्या कथमप्यनाद्यतायास्तत्राभावात् श्रुतस्याद्यता गुणाभावात् निरुपचरिताद्यसामीप्यादाद्यत्वोपचारात् / अवध्याद्यपेक्षयास्तु तस्य मुख्याद्यतेति चेत् न, मन:पर्ययाद्यपेक्षयावधेरप्याद्यत्वसिद्धर्मत्यवध्योर्ग्रहणप्रसंगात् जो ज्ञान अक्ष यानी आत्मा से परावृत्त है, वह परोक्ष है। आत्मा से भिन्न इन्द्रिय, मन आदि कारणों से ऊक्षित होता है, सींचा जाता है, पुष्टिकर होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, उसको परोक्ष कहते हैं। वह परोक्ष शब्द का वाच्य फिर क्या पदार्थ है? इस प्रकार जिज्ञासा होने पर आदि के दो ज्ञान-मति और श्रुत हैं अर्थात् इन्द्रियाधीन होने से मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष हैं। उन मति और श्रुत दोनों का आदिपन कैसे संभव है? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं-आये शब्द द्विवचनान्त है। मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् / इस सूत्र के पढ़े जाने के क्रम में यहाँ आदि के दो ज्ञान परोक्ष हैं, ऐसा ग्रन्थकार कहते हैं अत: मतिज्ञान को मुख्य आद्यपना है और उसके निकट होने के कारण श्रुतज्ञान को गौणरूप से आद्यपना है, ऐसा समझना चाहिए॥१॥ - जिस कारण सूत्रकार श्री उमास्वामी ने आदि के दो ज्ञान परोक्ष हैं, ऐसा सूत्र कहा है, उस कारण "मतिश्रुत" आदि सूत्र के पठनक्रम से यहाँ प्रथम दो का आदिपना जानना चाहिए और वह आदिपना मतिज्ञान को तो मुख्य है क्योंकि, उस मतिज्ञान में तो कैसे भी आदि में नहीं होनेपन का अभाव है। मति के निकट वाले श्रुतज्ञान को आद्यपना गौणरूप से है। निरुपचार से यानी मुख्यरूप से, आदि में पड़े हुए मतिज्ञान की समीपता से श्रुत को आद्यपने का उपचार कर लिया गया है। अवधि आदि की अपेक्षा से तो उस श्रुतज्ञान का मुख्यरूप से आद्यपना बन जाता है ऐसा नही कहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार तो मनःपर्यय आदि की अपेक्षा अवधि को भी आद्यपना सिद्ध हो जाएगा और ऐसा होने पर मति और अवधि इन दो के ग्रहण करने का प्रसंग होगा। आद्ये शब्द को द्विवचनरूप से कथन करने का भी इस प्रकार कोई विरोध नहीं आता है। अर्थात् “आद्ये" यह द्विवचनान्त होने से आदि मति और श्रुत इन दो भागों को ग्रहण करना चाहिए। केवलज्ञान की अपेक्षा से तो सब (चारों मति आदि) ज्ञानों को आद्यपना होते हुए भी मति आदि में से मति और श्रुत का ही यहाँ समीचीन ज्ञान होता है क्योंकि पाँच ज्ञानों में से मति और श्रुत ये दो ही ज्ञान साथ रहते हैं (अन्य दो ज्ञानों के साहचर्य का नियम नहीं है)-ऐसा नहीं कहना उचित है क्योंकि-मति अपेक्षा से श्रुत आदि के आद्य से रहितपना भी विद्यमान है अतः श्रुत आदि को मुख्यरूप से आद्यपने की असिद्धि होना बना रहता है। अर्थात्-आदि में होनेपन का निर्णय करने के लिए सहचरपना हेतु प्रयोजक नहीं