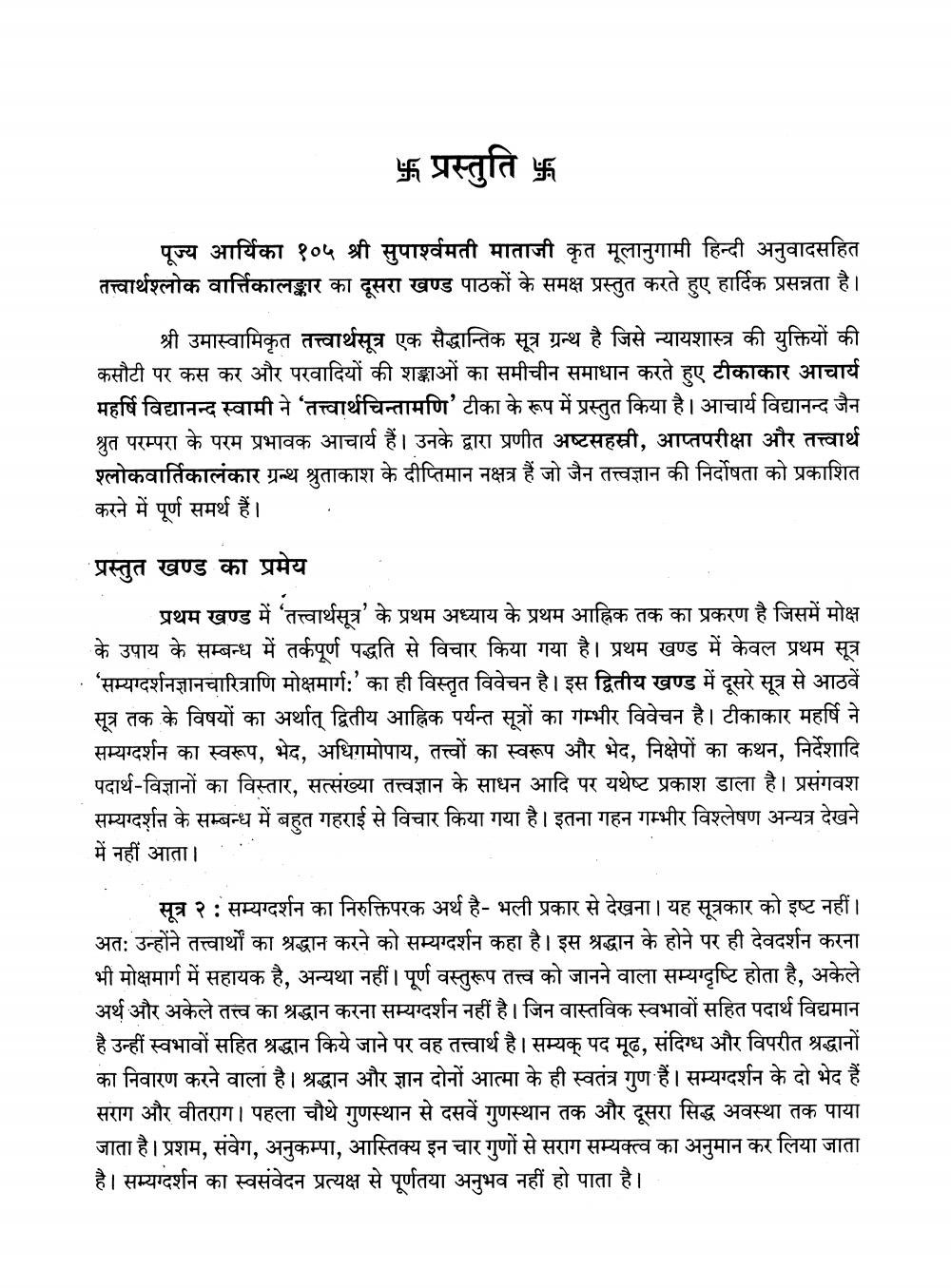________________ म प्रस्तुति पूज्य आर्यिका 105 श्री सुपार्श्वमती माताजी कृत मूलानुगामी हिन्दी अनुवादसहित तत्त्वार्थश्लोक वार्त्तिकालङ्कार का दूसरा खण्ड पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता है। श्री उमास्वामिकृत तत्त्वार्थसूत्र एक सैद्धान्तिक सूत्र ग्रन्थ है जिसे न्यायशास्त्र की युक्तियों की कसौटी पर कस कर और परवादियों की शङ्काओं का समीचीन समाधान करते हुए टीकाकार आचार्य महर्षि विद्यानन्द स्वामी ने 'तत्त्वार्थचिन्तामणि' टीका के रूप में प्रस्तुत किया है। आचार्य विद्यानन्द जैन श्रुत परम्परा के परम प्रभावक आचार्य हैं। उनके द्वारा प्रणीत अष्टसहस्री, आप्तपरीक्षा और तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिकालंकार ग्रन्थ श्रुताकाश के दीप्तिमान नक्षत्र हैं जो जैन तत्त्वज्ञान की निर्दोषता को प्रकाशित करने में पूर्ण समर्थ हैं। प्रस्तुत खण्ड का प्रमेय प्रथम खण्ड में 'तत्त्वार्थसूत्र' के प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक तक का प्रकरण है जिसमें मोक्ष के उपाय के सम्बन्ध में तर्कपूर्ण पद्धति से विचार किया गया है। प्रथम खण्ड में केवल प्रथम सूत्र 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' का ही विस्तृत विवेचन है। इस द्वितीय खण्ड में दूसरे सूत्र से आठवें सूत्र तक के विषयों का अर्थात् द्वितीय आह्निक पर्यन्त सूत्रों का गम्भीर विवेचन है। टीकाकार महर्षि ने सम्यग्दर्शन का स्वरूप, भेद, अधिगमोपाय, तत्त्वों का स्वरूप और भेद, निक्षेपों का कथन, निर्देशादि पदार्थ-विज्ञानों का विस्तार, सत्संख्या तत्त्वज्ञान के साधन आदि पर यथेष्ट प्रकाश डाला है। प्रसंगवश सम्यग्दर्शन के सम्बन्ध में बहुत गहराई से विचार किया गया है। इतना गहन गम्भीर विश्लेषण अन्यत्र देखने में नहीं आता। सूत्र 2 : सम्यग्दर्शन का निरुक्तिपरक अर्थ है- भली प्रकार से देखना / यह सूत्रकार को इष्ट नहीं। अतः उन्होंने तत्त्वार्थों का श्रद्धान करने को सम्यग्दर्शन कहा है। इस श्रद्धान के होने पर ही देवदर्शन करना भी मोक्षमार्ग में सहायक है, अन्यथा नहीं। पूर्ण वस्तुरूप तत्त्व को जानने वाला सम्यग्दृष्टि होता है, अकेले अर्थ और अकेले तत्त्व का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन नहीं है। जिन वास्तविक स्वभावों सहित पदार्थ विद्यमान है उन्हीं स्वभावों सहित श्रद्धान किये जाने पर वह तत्त्वार्थ है। सम्यक् पद मूढ, संदिग्ध और विपरीत श्रद्धानों का निवारण करने वाला है। श्रद्धान और ज्ञान दोनों आत्मा के ही स्वतंत्र गुण हैं। सम्यग्दर्शन के दो भेद हैं सराग और वीतराग। पहला चौथे गुणस्थान से दसवें गुणस्थान तक और दूसरा सिद्ध अवस्था तक पाया जाता है। प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, आस्तिक्य इन चार गुणों से सराग सम्यक्त्व का अनुमान कर लिया जाता है। सम्यग्दर्शन का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से पूर्णतया अनुभव नहीं हो पाता है।