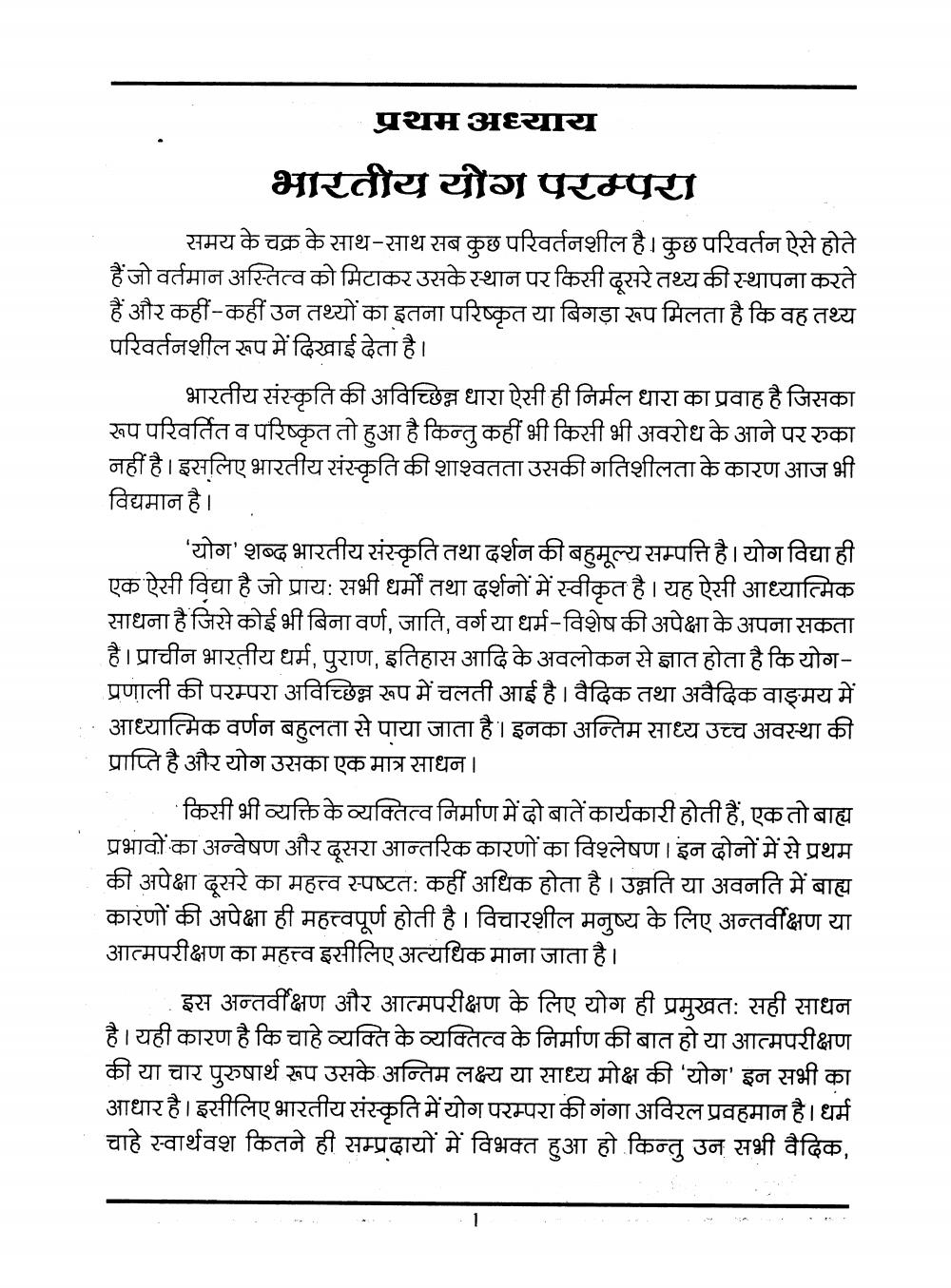________________ प्रथम अध्याय भारतीय योग परम्परा समय के चक्र के साथ-साथ सब कुछ परिवर्तनशील है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो वर्तमान अस्तित्व को मिटाकर उसके स्थान पर किसी दूसरे तथ्य की स्थापना करते हैं और कहीं-कहीं उन तथ्यों का इतना परिष्कृत या बिगड़ा रूप मिलता है कि वह तथ्य परिवर्तनशील रूप में दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति की अविच्छिन्न धारा ऐसी ही निर्मल धारा का प्रवाह है जिसका रूप परिवर्तित व परिष्कृत तो हुआ है किन्तु कहीं भी किसी भी अवरोध के आने पर रुका नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति की शाश्वतता उसकी गतिशीलता के कारण आज भी विद्यमान है। 'योग' शब्द भारतीय संस्कृति तथा दर्शन की बहुमूल्य सम्पत्ति है। योग विद्या ही एक ऐसी विद्या है जो प्राय: सभी धर्मों तथा दर्शनों में स्वीकृत है। यह ऐसी आध्यात्मिक साधना है जिसे कोई भी बिना वर्ण, जाति, वर्ग या धर्म-विशेष की अपेक्षा के अपना सकता है। प्राचीन भारतीय धर्म, पुराण, इतिहास आदि के अवलोकन से ज्ञात होता है कि योगप्रणाली की परम्परा अविच्छिन्न रूप में चलती आई है। वैदिक तथा अवैदिक वाङ्मय में आध्यात्मिक वर्णन बहुलता से पाया जाता है। इनका अन्तिम साध्य उच्च अवस्था की प्राप्ति है और योग उसका एक मात्र साधन। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में दो बातें कार्यकारी होती हैं, एक तो बाह्य प्रभावों का अन्वेषण और दसरा आन्तरिक कारणों का विश्लेषण। इन दोनों में से प्रथम की अपेक्षा दूसरे का महत्त्व स्पष्टत: कहीं अधिक होता है / उन्नति या अवनति में बाह्य कारणों की अपेक्षा ही महत्त्वपूर्ण होती है। विचारशील मनुष्य के लिए अन्तर्वीक्षण या आत्मपरीक्षण का महत्त्व इसीलिए अत्यधिक माना जाता है। इस अन्तर्वी क्षण और आत्मपरीक्षण के लिए योग ही प्रमुखत: सही साधन है। यही कारण है कि चाहे व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण की बात हो या आत्मपरीक्षण की या चार पुरुषार्थ रूप उसके अन्तिम लक्ष्य या साध्य मोक्ष की 'योग' इन सभी का आधार है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में योग परम्परा की गंगा अविरल प्रवहमान है। धर्म चाहे स्वार्थवश कितने ही सम्प्रदायों में विभक्त हुआ हो किन्तु उन सभी वैदिक,