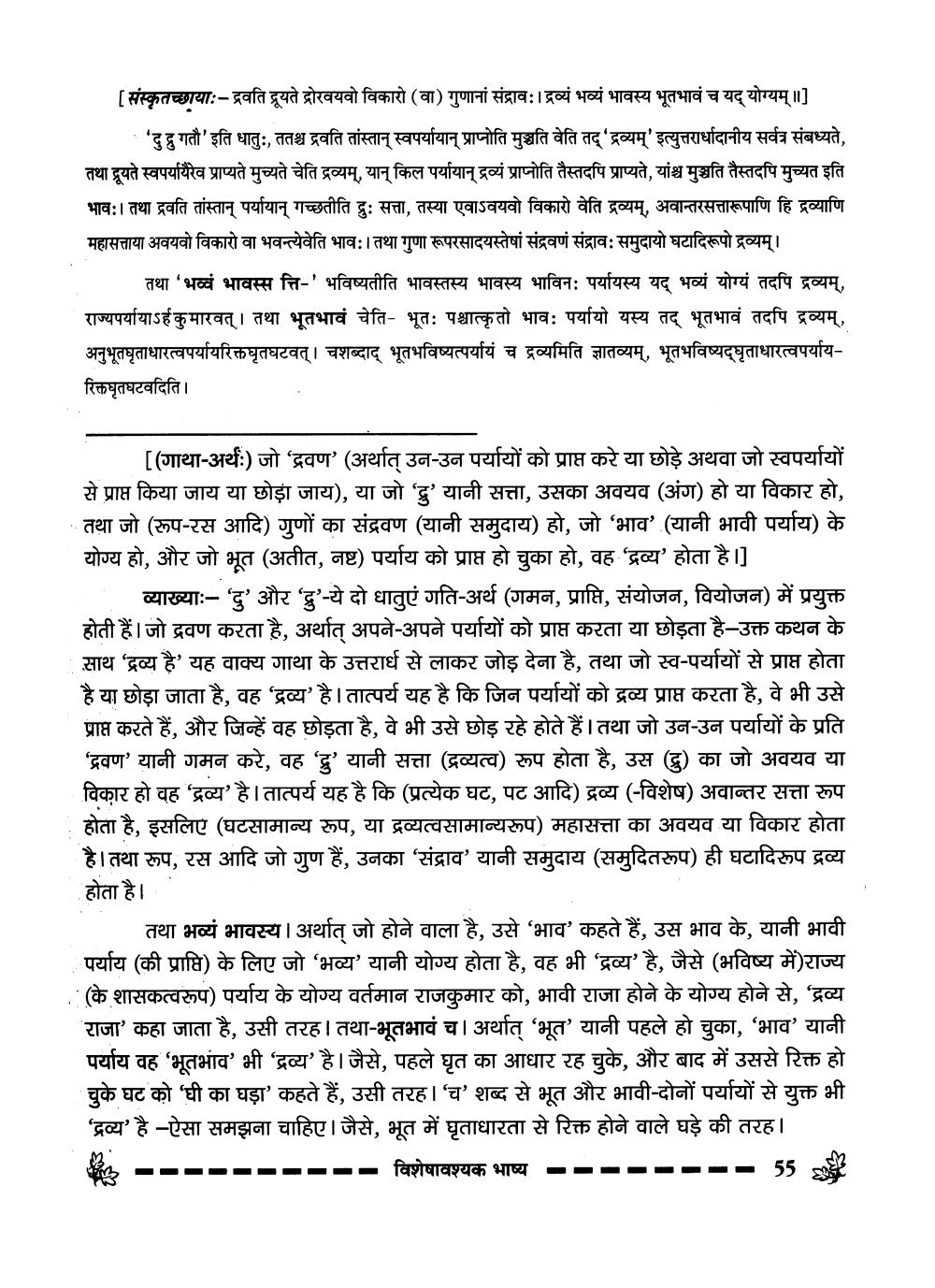________________ [संस्कृतच्छाया:- द्रवति द्रूयते द्रोरवयवो विकारो (वा) गुणानां संद्रावः। द्रव्यं भव्यं भावस्य भूतभावं च यद् योग्यम् // ] .. 'दुद्रु गतौ' इति धातुः, ततश्च द्रवति तांस्तान् स्वपर्यायान् प्राप्नोति मुञ्चति वेति तद् 'द्रव्यम्' इत्युत्तरार्धादानीय सर्वत्र संबध्यते, तथा द्रूयते स्वपर्यायैरेव प्राप्यते मुच्यते चेति द्रव्यम्, यान् किल पर्यायान् द्रव्यं प्राप्नोति तैस्तदपि प्राप्यते, यांश्च मुञ्चति तैस्तदपि मुच्यत इति भावः। तथा द्रवति तांस्तान् पर्यायान् गच्छतीति द्रुः सत्ता, तस्या एवाऽवयवो विकारो वेति द्रव्यम्, अवान्तरसत्तारूपाणि हि द्रव्याणि महासत्ताया अवयवो विकारो वा भवन्त्येवेति भावः। तथा गुणा रूपरसादयस्तेषां संद्रवणं संद्राव: समुदायो घटादिरूपो द्रव्यम्। तथा 'भव्वं भावस्स त्ति-' भविष्यतीति भावस्तस्य भावस्य भाविनः पर्यायस्य यद् भव्यं योग्यं तदपि द्रव्यम्, राज्यपर्यायाऽर्ह कुमारवत् / तथा भूतभावं चेति- भूतः पश्चात्कृतो भावः पर्यायो यस्य तद् भूतभावं तदपि द्रव्यम्, अनुभूतघृताधारत्वपर्यायरिक्तघृतघटवत्। चशब्दाद् भूतभविष्यत्पर्यायं च द्रव्यमिति ज्ञातव्यम्, भूतभविष्यघृताधारत्वपर्यायरिक्तघृतघटवदिति। [(गाथा-अर्थः) जो 'द्रवण' (अर्थात् उन-उन पर्यायों को प्राप्त करे या छोड़े अथवा जो स्वपर्यायों से प्राप्त किया जाय या छोड़ा जाय), या जो 'द्रु' यानी सत्ता, उसका अवयव (अंग) हो या विकार हो, तथा जो (रूप-रस आदि) गुणों का संद्रवण (यानी समुदाय) हो, जो 'भाव' (यानी भावी पर्याय) के योग्य हो, और जो भूत (अतीत, नष्ट) पर्याय को प्राप्त हो चुका हो, वह 'द्रव्य' होता है।] व्याख्याः - 'दु' और 'द्रु'-ये दो धातुएं गति-अर्थ (गमन, प्राप्ति, संयोजन, वियोजन) में प्रयुक्त होती हैं। जो द्रवण करता है, अर्थात् अपने-अपने पर्यायों को प्राप्त करता या छोड़ता है-उक्त कथन के साथ 'द्रव्य है' यह वाक्य गाथा के उत्तरार्ध से लाकर जोड़ देना है, तथा जो स्व-पर्यायों से प्राप्त होता है या छोड़ा जाता है, वह 'द्रव्य' है। तात्पर्य यह है कि जिन पर्यायों को द्रव्य प्राप्त करता है, वे भी उसे प्राप्त करते हैं, और जिन्हें वह छोड़ता है, वे भी उसे छोड़ रहे होते हैं। तथा जो उन-उन पर्यायों के प्रति 'द्रवण' यानी गमन करे, वह 'द्रु' यानी सत्ता (द्रव्यत्व) रूप होता है, उस (द्रु) का जो अवयव या विकार हो वह 'द्रव्य' है / तात्पर्य यह है कि (प्रत्येक घट, पट आदि) द्रव्य (-विशेष) अवान्तर सत्ता रूप होता है, इसलिए (घटसामान्य रूप, या द्रव्यत्वसामान्यरूप) महासत्ता का अवयव या विकार होता है। तथा रूप, रस आदि जो गुण हैं, उनका 'संद्राव' यानी समुदाय (समुदितरूप) ही घटादिरूप द्रव्य होता है। तथा भव्यं भावस्य। अर्थात् जो होने वाला है, उसे 'भाव' कहते हैं, उस भाव के, यानी भावी पर्याय (की प्राप्ति) के लिए जो 'भव्य' यानी योग्य होता है, वह भी 'द्रव्य' है, जैसे (भविष्य में)राज्य (के शासकत्वरूप) पर्याय के योग्य वर्तमान राजकुमार को, भावी राजा होने के योग्य होने से, 'द्रव्य राजा' कहा जाता है, उसी तरह / तथा-भूतभावं च / अर्थात् 'भूत' यानी पहले हो चुका, 'भाव' यानी पर्याय वह 'भूतभाव' भी 'द्रव्य' है। जैसे, पहले घृत का आधार रह चुके, और बाद में उससे रिक्त हो चुके घट को ‘घी का घड़ा' कहते हैं, उसी तरह। 'च' शब्द से भूत और भावी-दोनों पर्यायों से युक्त भी 'द्रव्य' है -ऐसा समझना चाहिए। जैसे, भूत में घृताधारता से रिक्त होने वाले घड़े की तरह। ------ 55 -------- विशेषावश्यक भाष्य - - - - - -