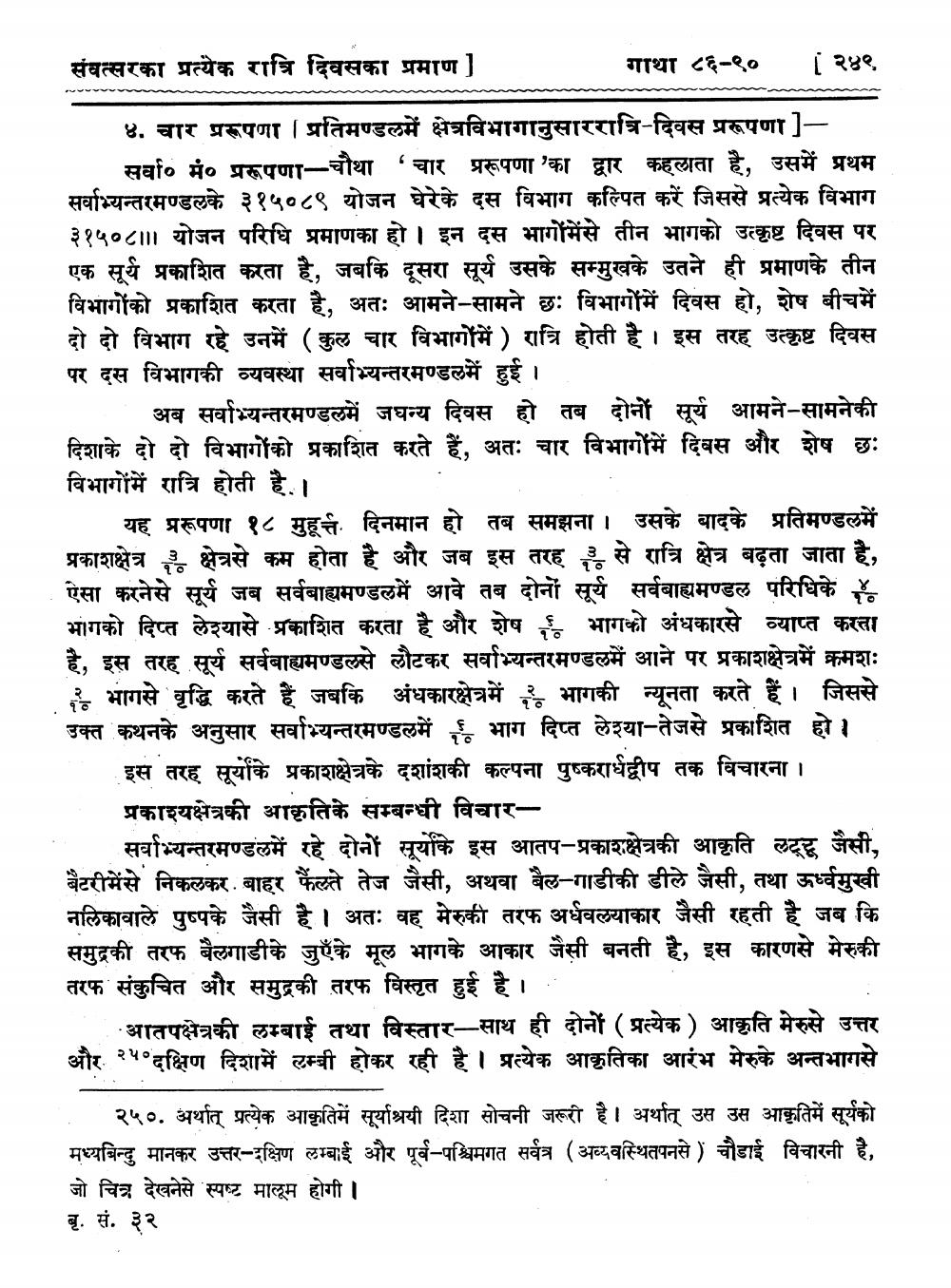________________ संवत्सरका प्रत्येक रात्रि दिवसका प्रमाण ] गाथा 86-90 [249 4. चार प्ररूपणा [ प्रतिमण्डलमें क्षेत्रविभागानुसाररात्रि-दिवस प्ररूपणा] सर्वा० मं० प्ररूपणा-चौथा 'चार प्ररूपणा'का द्वार कहलाता है, उसमें प्रथम सर्वाभ्यन्तरमण्डलके 315089 योजन घेरेके दस विभाग कल्पित करें जिससे प्रत्येक विभाग 31508 // योजन परिधि प्रमाणका हो। इन दस भागोंमेंसे तीन भागको उत्कृष्ट दिवस पर एक सूर्य प्रकाशित करता है, जबकि दूसरा सूर्य उसके सम्मुखके उतने ही प्रमाणके तीन विभागोंको प्रकाशित करता है, अतः आमने-सामने छः विभागोंमें दिवस हो, शेष बीचमें दो दो विभाग रहे उनमें (कुल चार विभागों में ) रात्रि होती है। इस तरह उत्कृष्ट दिवस पर दस विभागकी व्यवस्था सर्वाभ्यन्तरमण्डलमें हुई। ___ अब सर्वाभ्यन्तरमण्डलमें जघन्य दिवस हो तब दोनों सूर्य आमने-सामनेकी दिशाके दो दो विभागोंको प्रकाशित करते हैं, अतः चार विभागोंमें दिवस और शेष छः विभागोंमें रात्रि होती है.। यह प्ररूपणा 18 मुहूर्त दिनमान हो तब समझना। उसके बादके प्रतिमण्डलमें प्रकाशक्षेत्र 3 क्षेत्रसे कम होता है और जब इस तरह 3 से रात्रि क्षेत्र बढ़ता जाता है, ऐसा करनेसे सूर्य जब सर्वबाह्यमण्डलमें आवे तब दोनों सूर्य सर्वबाह्यमण्डल परिधिके / भागको दिप्त लेश्यासे प्रकाशित करता है और शेष भागको अंधकारसे व्याप्त करता है, इस तरह सूर्य सर्वबाह्यमण्डलसे लौटकर सर्वाभ्यन्तरमण्डलमें आने पर प्रकाशक्षेत्रमें क्रमशः 2. भागसे वृद्धि करते हैं जबकि अंधकारक्षेत्रमें 2 भागकी न्यूनता करते हैं। जिससे उक्त कथनके अनुसार सर्वाभ्यन्तरमण्डलमें , भाग दिप्त लेश्या-तेजसे प्रकाशित हो। इस तरह सूर्योंके प्रकाशक्षेत्रके दशांशकी कल्पना पुष्करार्धद्वीप तक विचारना / प्रकाश्यक्षेत्रकी आकृतिके सम्बन्धी विचार सर्वाभ्यन्तरमण्डलमें रहे दोनों सूर्योंके इस आतप-प्रकाशक्षेत्रकी आकृति लटू जैसी, बैटरीमेंसे निकलकर. बाहर फैलते तेज जैसी, अथवा बैल-गाडीकी डीले जैसी, तथा ऊर्ध्वमुखी नलिकावाले पुष्पके जैसी है। अतः वह मेरुकी तरफ अर्धवलयाकार जैसी रहती है जब कि समुद्रकी तरफ बैलगाडीके जुएँके मूल भागके आकार जैसी बनती है, इस कारणसे मेरुकी तरफ संकुचित और समुद्रकी तरफ विस्तृत हुई है। .. आतपक्षेत्रकी लम्बाई तथा विस्तार–साथ ही दोनों (प्रत्येक ) आकृति मेरुसे उत्तर और २५°दक्षिण दिशामें लम्बी होकर रही है। प्रत्येक आकृतिका आरंभ मेरुके अन्तभागसे . 250. अर्थात् प्रत्येक आकृतिमें सूर्याश्रयी दिशा सोचनी जरूरी है। अर्थात् उस उस आकृतिमें सूर्यको मध्यबिन्दु मानकर उत्तर-दक्षिण लम्बाई और पूर्व-पश्चिमगत सर्वत्र (अव्यवस्थितपनसे ) चौडाई विचारनी है, जो चित्र देखनेसे स्पष्ट मालूम होगी। बृ. सं. 32