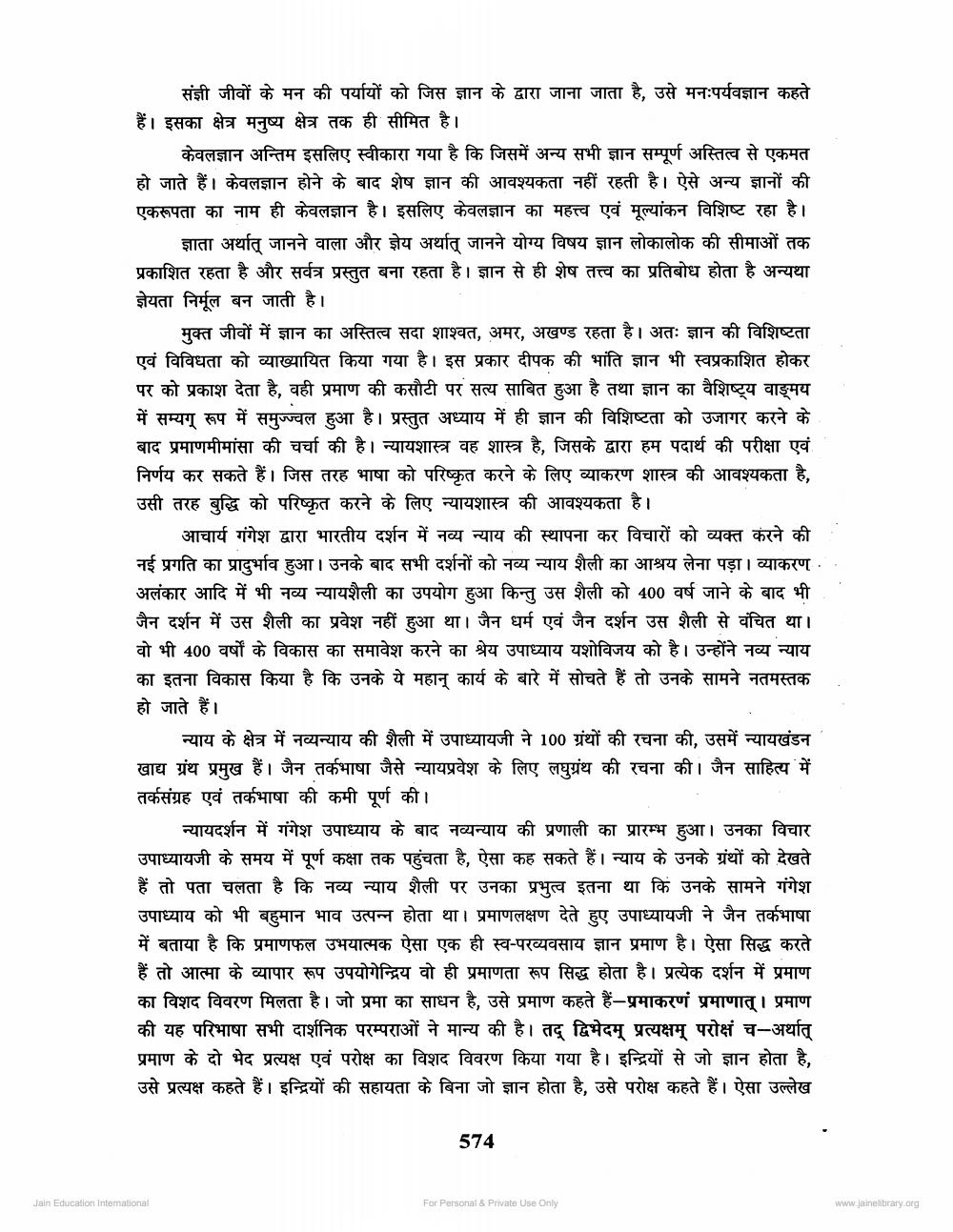________________ संज्ञी जीवों के मन की पर्यायों को जिस ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, उसे मनःपर्यवज्ञान कहते हैं। इसका क्षेत्र मनुष्य क्षेत्र तक ही सीमित है। केवलज्ञान अन्तिम इसलिए स्वीकारा गया है कि जिसमें अन्य सभी ज्ञान सम्पूर्ण अस्तित्व से एकमत हो जाते हैं। केवलज्ञान होने के बाद शेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसे अन्य ज्ञानों की एकरूपता का नाम ही केवलज्ञान है। इसलिए केवलज्ञान का महत्त्व एवं मूल्यांकन विशिष्ट रहा है। ज्ञाता अर्थात् जानने वाला और ज्ञेय अर्थात् जानने योग्य विषय ज्ञान लोकालोक की सीमाओं तक प्रकाशित रहता है और सर्वत्र प्रस्तुत बना रहता है। ज्ञान से ही शेष तत्त्व का प्रतिबोध होता है अन्यथा ज्ञेयता निर्मूल बन जाती है। मुक्त जीवों में ज्ञान का अस्तित्व सदा शाश्वत, अमर, अखण्ड रहता है। अतः ज्ञान की विशिष्टता एवं विविधता को व्याख्यायित किया गया है। इस प्रकार दीपक की भांति ज्ञान भी स्वप्रकाशित होकर पर को प्रकाश देता है, वही प्रमाण की कसौटी पर सत्य साबित हुआ है तथा ज्ञान का वैशिष्ट्य वाङ्मय में सम्यग् रूप में समुज्ज्वल हुआ है। प्रस्तुत अध्याय में ही ज्ञान की विशिष्टता को उजागर करने के बाद प्रमाणमीमांसा की चर्चा की है। न्यायशास्त्र वह शास्त्र है, जिसके द्वारा हम पदार्थ की परीक्षा एवं निर्णय कर सकते हैं। जिस तरह भाषा को परिष्कृत करने के लिए व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता है, उसी तरह बुद्धि को परिष्कृत करने के लिए न्यायशास्त्र की आवश्यकता है। आचार्य गंगेश द्वारा भारतीय दर्शन में नव्य न्याय की स्थापना कर विचारों को व्यक्त करने की नई प्रगति का प्रादुर्भाव हुआ। उनके बाद सभी दर्शनों को नव्य न्याय शैली का आश्रय लेना पड़ा। व्याकरण : अलंकार आदि में भी नव्य न्यायशैली का उपयोग हुआ किन्तु उस शैली को 400 वर्ष जाने के बाद भी जैन दर्शन में उस शैली का प्रवेश नहीं हुआ था। जैन धर्म एवं जैन दर्शन उस शैली से वंचित था। वो भी 400 वर्षों के विकास का समावेश करने का श्रेय उपाध्याय यशोविजय को है। उन्होंने नव्य न्याय का इतना विकास किया है कि उनके ये महान् कार्य के बारे में सोचते हैं तो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। न्याय के क्षेत्र में नव्यन्याय की शैली में उपाध्यायजी ने 100 ग्रंथों की रचना की, उसमें न्यायखंडन खाद्य ग्रंथ प्रमुख हैं। जैन तर्कभाषा जैसे न्यायप्रवेश के लिए लघुग्रंथ की रचना की। जैन साहित्य में तर्कसंग्रह एवं तर्कभाषा की कमी पूर्ण की। न्यायदर्शन में गंगेश उपाध्याय के बाद नव्यन्याय की प्रणाली का प्रारम्भ हुआ। उनका विचार उपाध्यायजी के समय में पूर्ण कक्षा तक पहुंचता है, ऐसा कह सकते हैं। न्याय के उनके ग्रंथों को देखते हैं तो पता चलता है कि नव्य न्याय शैली पर उनका प्रभुत्व इतना था कि उनके सामने गंगेश उपाध्याय को भी बहुमान भाव उत्पन्न होता था। प्रमाणलक्षण देते हुए उपाध्यायजी ने जैन तर्कभाषा में बताया है कि प्रमाणफल उभयात्मक ऐसा एक ही स्व-परव्यवसाय ज्ञान प्रमाण है। ऐसा सिद्ध करते हैं तो आत्मा के व्यापार रूप उपयोगेन्द्रिय वो ही प्रमाणता रूप सिद्ध होता है। प्रत्येक दर्शन में प्रमाण का विशद विवरण मिलता है। जो प्रमा का साधन है, उसे प्रमाण कहते हैं-प्रमाकरणं प्रमाणात्। प्रमाण की यह परिभाषा सभी दार्शनिक परम्पराओं ने मान्य की है। तद् द्विभेदम् प्रत्यक्षम् परोक्षं च-अर्थात् प्रमाण के दो भेद प्रत्यक्ष एवं परोक्ष का विशद विवरण किया गया है। इन्द्रियों से जो ज्ञान होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इन्द्रियों की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है, उसे परोक्ष कहते हैं। ऐसा उल्लेख 574 Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org