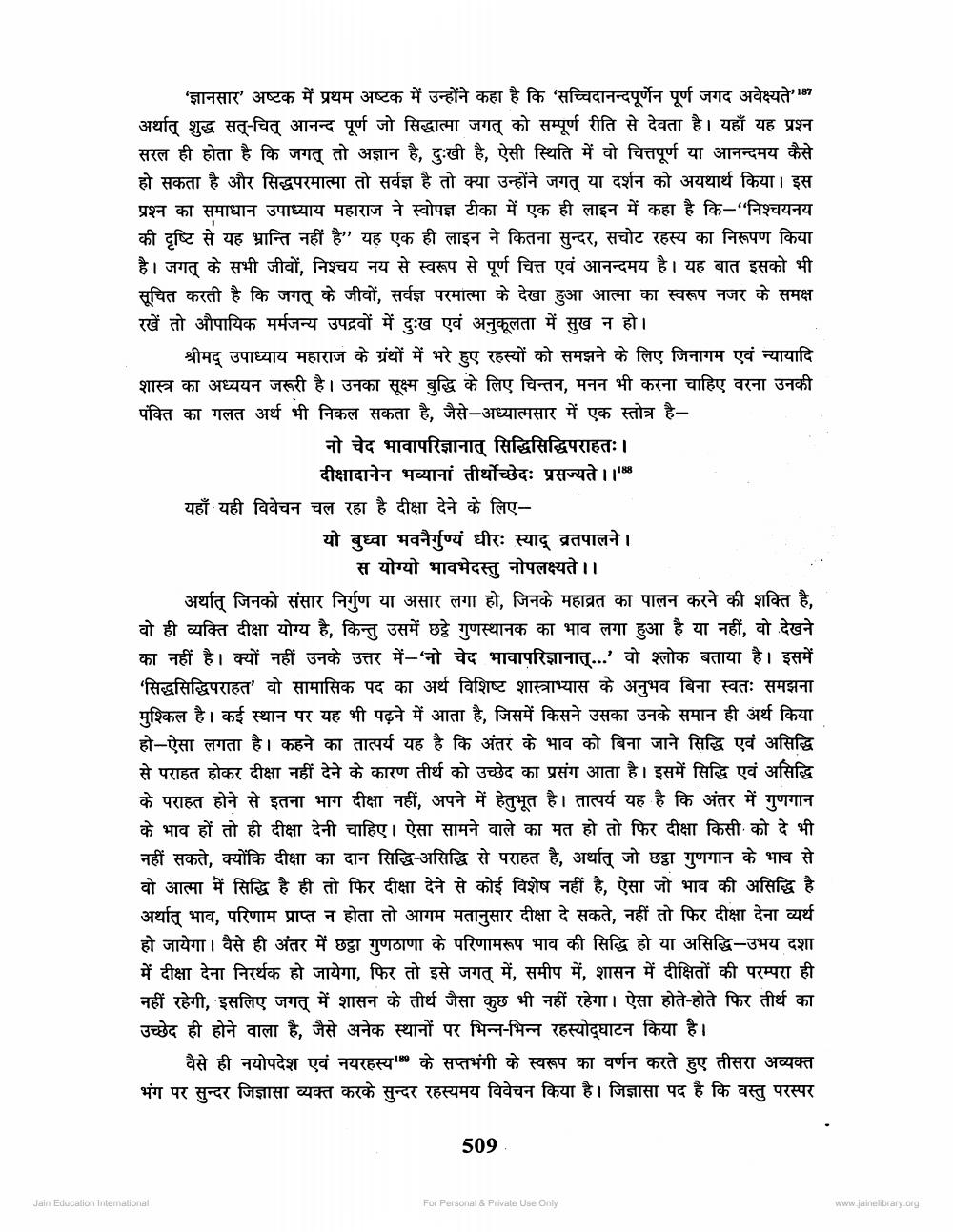________________ 'ज्ञानसार' अष्टक में प्रथम अष्टक में उन्होंने कहा है कि 'सच्चिदानन्दपूर्णेन पूर्ण जगद अवेक्ष्यते'187 अर्थात् शुद्ध सत्-चित् आनन्द पूर्ण जो सिद्धात्मा जगत् को सम्पूर्ण रीति से देवता है। यहाँ यह प्रश्न सरल ही होता है कि जगत् तो अज्ञान है, दुःखी है, ऐसी स्थिति में वो चित्तपूर्ण या आनन्दमय कैसे हो सकता है और सिद्धपरमात्मा तो सर्वज्ञ है तो क्या उन्होंने जगत् या दर्शन को अयथार्थ किया। इस प्रश्न का समाधान उपाध्याय महाराज ने स्वोपज्ञ टीका में एक ही लाइन में कहा है कि-"निश्चयनय की दृष्टि से यह भ्रान्ति नहीं है" यह एक ही लाइन ने कितना सुन्दर, सचोट रहस्य का निरूपण किया है। जगत् के सभी जीवों, निश्चय नय से स्वरूप से पूर्ण चित्त एवं आनन्दमय है। यह बात इसको भी सूचित करती है कि जगत् के जीवों, सर्वज्ञ परमात्मा के देखा हुआ आत्मा का स्वरूप नजर के समक्ष रखें तो औपायिक मर्मजन्य उपद्रवों में दुःख एवं अनुकूलता में सुख न हो। श्रीमद् उपाध्याय महाराज के ग्रंथों में भरे हुए रहस्यों को समझने के लिए जिनागम एवं न्यायादि शास्त्र का अध्ययन जरूरी है। उनका सूक्ष्म बुद्धि के लिए चिन्तन, मनन भी करना चाहिए वरना उनकी पंक्ति का गलत अर्थ भी निकल सकता है, जैसे-अध्यात्मसार में एक स्तोत्र है नो चेद भावापरिज्ञानात् सिद्धिसिद्धिपराहतः। दीक्षादानेन भव्यानां तीर्थोच्छेदः प्रसज्यते / / 88 यहाँ यही विवेचन चल रहा है दीक्षा देने के लिए यो बुध्वा भवनैर्गुण्यं धीरः स्याद् व्रतपालने। स योग्यो भावभेदस्तु नोपलक्ष्यते।। अर्थात जिनको संसार निर्गुण या असार लगा हो, जिनके महाव्रत का पालन करने की शक्ति है, वो ही व्यक्ति दीक्षा योग्य है, किन्तु उसमें छठे गुणस्थानक का भाव लगा हुआ है या नहीं, वो देखने का नहीं है। क्यों नहीं उनके उत्तर में-'नो चेद भावापरिज्ञानात्...' वो श्लोक बताया है। इसमें 'सिद्धसिद्धिपराहत' वो सामासिक पद का अर्थ विशिष्ट शास्त्राभ्यास के अनुभव बिना स्वतः समझना मुश्किल है। कई स्थान पर यह भी पढ़ने में आता है, जिसमें किसने उसका उनके समान ही अर्थ किया हो-ऐसा लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर के भाव को बिना जाने सिद्धि एवं असिद्धि से पराहत होकर दीक्षा नहीं देने के कारण तीर्थ को उच्छेद का प्रसंग आता है। इसमें सिद्धि एवं असिद्धि के पराहत होने से इतना भाग दीक्षा नहीं, अपने में हेतुभूत है। तात्पर्य यह है कि अंतर में गुणगान के भाव हों तो ही दीक्षा देनी चाहिए। ऐसा सामने वाले का मत हो तो फिर दीक्षा किसी को दे भी नहीं सकते, क्योंकि दीक्षा का दान सिद्धि-असिद्धि से पराहत है, अर्थात् जो छट्ठा गुणगान के भाव से वो आत्मा में सिद्धि है ही तो फिर दीक्षा देने से कोई विशेष नहीं है, ऐसा जो भाव की असिद्धि है अर्थात् भाव, परिणाम प्राप्त न होता तो आगम मतानुसार दीक्षा दे सकते, नहीं तो फिर दीक्षा देना व्यर्थ हो जायेगा। वैसे ही अंतर में छट्ठा गुणठाणा के परिणामरूप भाव की सिद्धि हो या असिद्धि-उभय दशा में दीक्षा देना निरर्थक हो जायेगा, फिर तो इसे जगत् में, समीप में, शासन में दीक्षितों की परम्परा ही नहीं रहेगी, इसलिए जगत् में शासन के तीर्थ जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा होते-होते फिर तीर्थ का उच्छेद ही होने वाला है, जैसे अनेक स्थानों पर भिन्न-भिन्न रहस्योद्घाटन किया है। वैसे ही नयोपदेश एवं नयरहस्य के सप्तभंगी के स्वरूप का वर्णन करते हुए तीसरा अव्यक्त भंग पर सुन्दर जिज्ञासा व्यक्त करके सुन्दर रहस्यमय विवेचन किया है। जिज्ञासा पद है कि वस्तु परस्पर 509. Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org