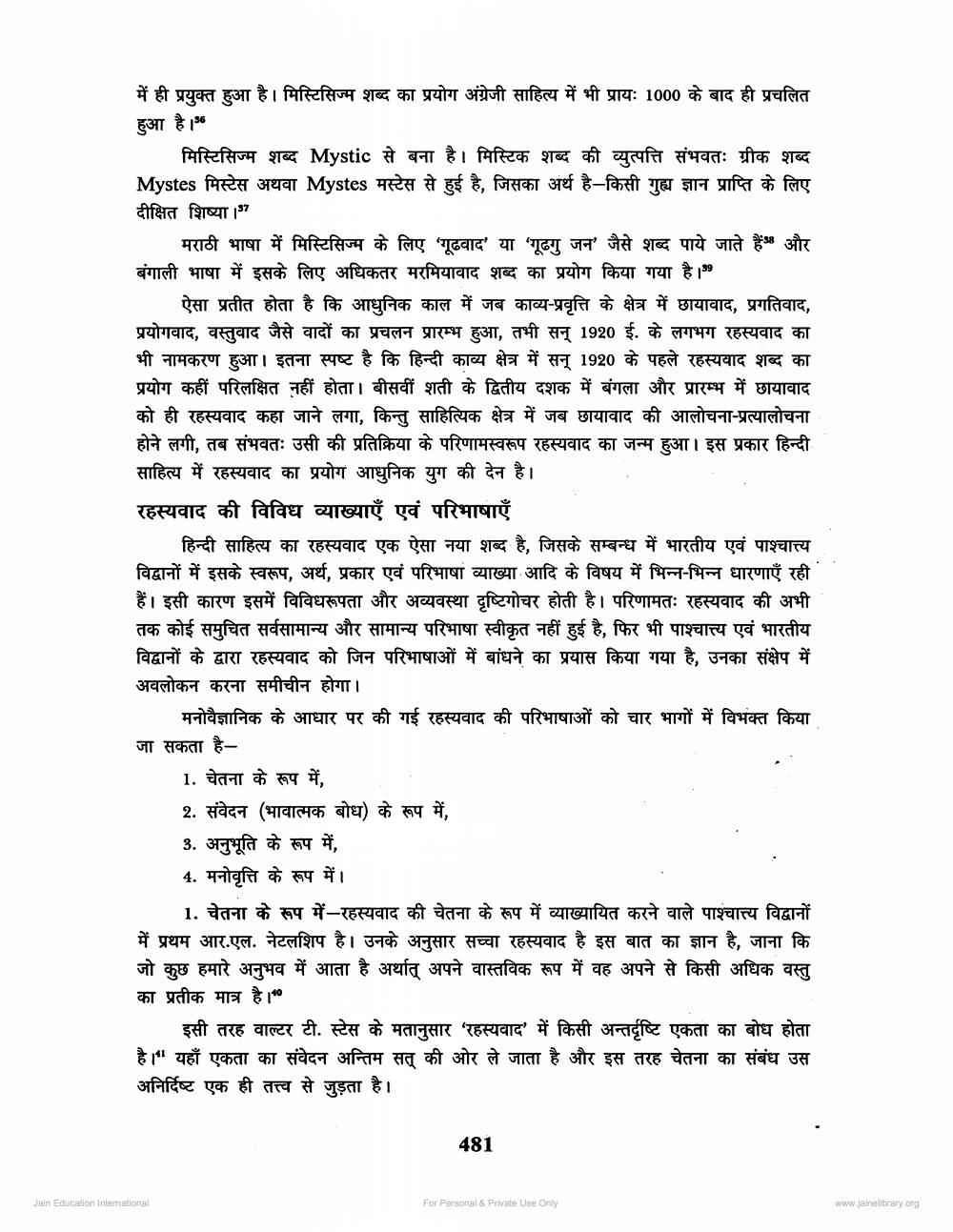________________ में ही प्रयुक्त हुआ है। मिस्टिसिज्म शब्द का प्रयोग अंग्रेजी साहित्य में भी प्रायः 1000 के बाद ही प्रचलित हुआ है। मिस्टिसिज्म शब्द Mystic से बना है। मिस्टिक शब्द की व्युत्पत्ति संभवतः ग्रीक शब्द Mystes मिस्टेस अथवा Mystes मस्टेस से हुई है, जिसका अर्थ है-किसी गुह्य ज्ञान प्राप्ति के लिए दीक्षित शिष्या।" ___मराठी भाषा में मिस्टिसिज्म के लिए 'गूढवाद' या 'गूढगु जन' जैसे शब्द पाये जाते हैं और बंगाली भाषा में इसके लिए अधिकतर मरमियावाद शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक काल में जब काव्य-प्रवृत्ति के क्षेत्र में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, वस्तुवाद जैसे वादों का प्रचलन प्रारम्भ हुआ, तभी सन् 1920 ई. के लगभग रहस्यवाद का भी नामकरण हुआ। इतना स्पष्ट है कि हिन्दी काव्य क्षेत्र में सन् 1920 के पहले रहस्यवाद शब्द का प्रयोग कहीं परिलक्षित नहीं होता। बीसवीं शती के द्वितीय दशक में बंगला और प्रारम्भ में छायावाद को ही रहस्यवाद कहा जाने लगा, किन्तु साहित्यिक क्षेत्र में जब छायावाद की आलोचना-प्रत्यालोचना होने लगी, तब संभवतः उसी की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप रहस्यवाद का जन्म हुआ। इस प्रकार हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद का प्रयोग आधुनिक युग की देन है। रहस्यवाद की विविध व्याख्याएँ एवं परिभाषाएँ हिन्दी साहित्य का रहस्यवाद एक ऐसा नया शब्द है, जिसके सम्बन्ध में भारतीय एवं पाश्चात्त्य विद्वानों में इसके स्वरूप, अर्थ, प्रकार एवं परिभाषा व्याख्या आदि के विषय में भिन्न-भिन्न धारणाएँ रही हैं। इसी कारण इसमें विविधरूपता और अव्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। परिणामतः रहस्यवाद की अभी तक कोई समुचित सर्वसामान्य और सामान्य परिभाषा स्वीकृत नहीं हुई है, फिर भी पाश्चात्त्य एवं भारतीय विद्वानों के द्वारा रहस्यवाद को जिन परिभाषाओं में बांधने का प्रयास किया गया है, उनका संक्षेप में अवलोकन करना समीचीन होगा। मनोवैज्ञानिक के आधार पर की गई रहस्यवाद की परिभाषाओं को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है 1. चेतना के रूप में, 2. संवेदन (भावात्मक बोध) के रूप में, 3. अनुभूति के रूप में, 4. मनोवृत्ति के रूप में। 1. चेतना के रूप में-रहस्यवाद की चेतना के रूप में व्याख्यायित करने वाले पाश्चात्त्य विद्वानों में प्रथम आर.एल. नेटलशिप है। उनके अनुसार सच्चा रहस्यवाद है इस बात का ज्ञान है, जाना कि जो कुछ हमारे अनुभव में आता है अर्थात् अपने वास्तविक रूप में वह अपने से किसी अधिक वस्तु का प्रतीक मात्र है। इसी तरह वाल्टर टी. स्टेस के मतानुसार 'रहस्यवाद' में किसी अन्तदृष्टि एकता का बोध होता है।" यहाँ एकता का संवेदन अन्तिम सत् की ओर ले जाता है और इस तरह चेतना का संबंध उस अनिर्दिष्ट एक ही तत्त्व से जुड़ता है। 481 Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org