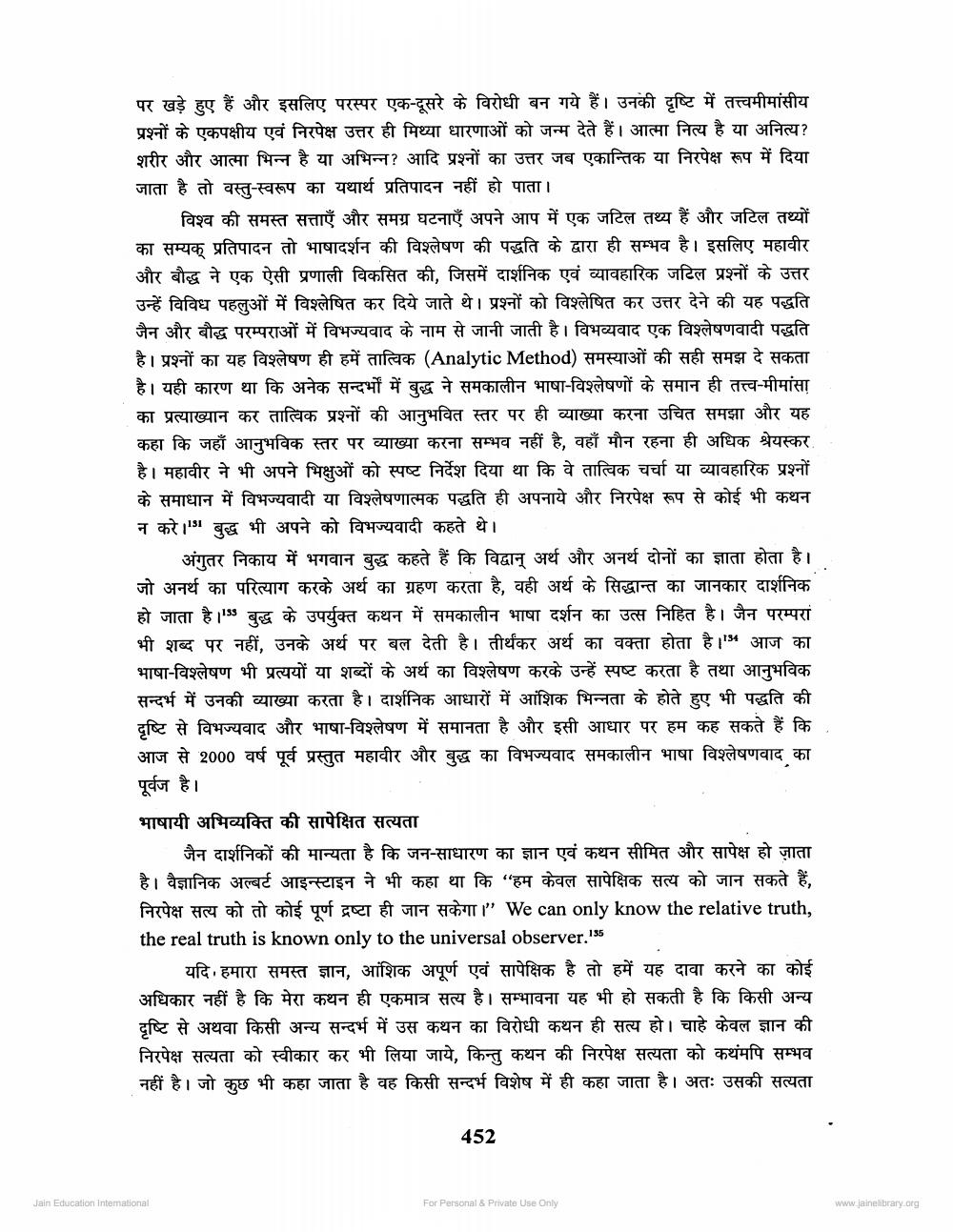________________ पर खड़े हुए हैं और इसलिए परस्पर एक-दूसरे के विरोधी बन गये हैं। उनकी दृष्टि में तत्त्वमीमांसीय प्रश्नों के एकपक्षीय एवं निरपेक्ष उत्तर ही मिथ्या धारणाओं को जन्म देते हैं। आत्मा नित्य है या अनित्य? शरीर और आत्मा भिन्न है या अभिन्न? आदि प्रश्नों का उत्तर जब एकान्तिक या निरपेक्ष रूप में दिया जाता है तो वस्तु-स्वरूप का यथार्थ प्रतिपादन नहीं हो पाता। विश्व की समस्त सत्ताएँ और समग्र घटनाएँ अपने आप में एक जटिल तथ्य हैं और जटिल तथ्यों का सम्यक् प्रतिपादन तो भाषादर्शन की विश्लेषण की पद्धति के द्वारा ही सम्भव है। इसलिए महावीर और बौद्ध ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की, जिसमें दार्शनिक एवं व्यावहारिक जटिल प्रश्नों के उत्तर उन्हें विविध पहलुओं में विश्लेषित कर दिये जाते थे। प्रश्नों को विश्लेषित कर उत्तर देने की यह पद्धति जैन और बौद्ध परम्पराओं में विभज्यवाद के नाम से जानी जाती है। विभव्यवाद एक विश्लेषणवादी पद्धति है। प्रश्नों का यह विश्लेषण ही हमें तात्विक (Analytic Method) समस्याओं की सही समझ दे सकता है। यही कारण था कि अनेक सन्दर्भो में बुद्ध ने समकालीन भाषा-विश्लेषणों के समान ही तत्त्व-मीमांसा का प्रत्याख्यान कर तात्विक प्रश्नों की आनुभवित स्तर पर ही व्याख्या करना उचित समझा और यह कहा कि जहाँ आनुभविक स्तर पर व्याख्या करना सम्भव नहीं है, वहाँ मौन रहना ही अधिक श्रेयस्कर है। महावीर ने भी अपने भिक्षुओं को स्पष्ट निर्देश दिया था कि वे तात्विक चर्चा या व्यावहारिक प्रश्नों के समाधान में विभज्यवादी या विश्लेषणात्मक पद्धति ही अपनाये और निरपेक्ष रूप से कोई भी कथन न करे। बुद्ध भी अपने को विभज्यवादी कहते थे। अंगुतर निकाय में भगवान बुद्ध कहते हैं कि विद्वान् अर्थ और अनर्थ दोनों का ज्ञाता होता है। जो अनर्थ का परित्याग करके अर्थ का ग्रहण करता है, वही अर्थ के सिद्धान्त का जानकार दार्शनिक हो जाता है। बुद्ध के उपर्युक्त कथन में समकालीन भाषा दर्शन का उत्स निहित है। जैन परम्परा भी शब्द पर नहीं, उनके अर्थ पर बल देती है। तीर्थंकर अर्थ का वक्ता होता है। आज का भाषा-विश्लेषण भी प्रत्ययों या शब्दों के अर्थ का विश्लेषण करके उन्हें स्पष्ट करता है तथा आनुभविक सन्दर्भ में उनकी व्याख्या करता है। दार्शनिक आधारों में आंशिक भिन्नता के होते हुए भी पद्धति की दृष्टि से विभज्यवाद और भाषा-विश्लेषण में समानता है और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रस्तुत महावीर और बुद्ध का विभज्यवाद समकालीन भाषा विश्लेषणवाद का पूर्वज है। भाषायी अभिव्यक्ति की सापेक्षित सत्यता जैन दार्शनिकों की मान्यता है कि जन-साधारण का ज्ञान एवं कथन सीमित और सापेक्ष हो जाता है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन ने भी कहा था कि “हम केवल सापेक्षिक सत्य को जान सकते हैं, निरपेक्ष सत्य को तो कोई पूर्ण द्रष्टा ही जान सकेगा।" We can only know the relative truth, the real truth is known only to the universal observer.is यदि हमारा समस्त ज्ञान, आंशिक अपूर्ण एवं सापेक्षिक है तो हमें यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि मेरा कथन ही एकमात्र सत्य है। सम्भावना यह भी हो सकती है कि किसी अन्य दृष्टि से अथवा किसी अन्य सन्दर्भ में उस कथन का विरोधी कथन ही सत्य हो। चाहे केवल ज्ञान की निरपेक्ष सत्यता को स्वीकार कर भी लिया जाये, किन्तु कथन की निरपेक्ष सत्यता को कथमपि सम्भव नहीं है। जो कुछ भी कहा जाता है वह किसी सन्दर्भ विशेष में ही कहा जाता है। अतः उसकी सत्यता 452 Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org