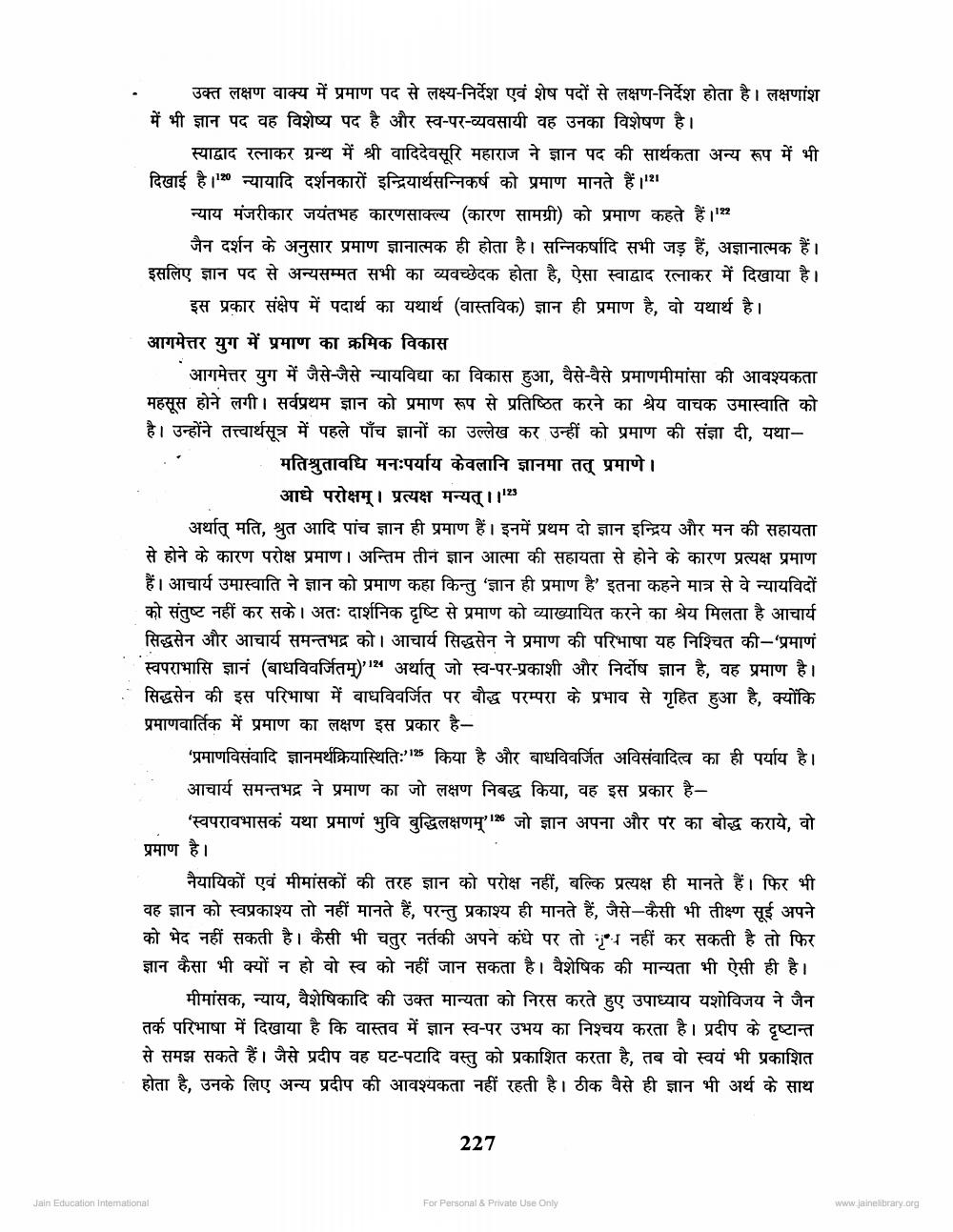________________ उक्त लक्षण वाक्य में प्रमाण पद से लक्ष्य-निर्देश एवं शेष पदों से लक्षण-निर्देश होता है। लक्षणांश में भी ज्ञान पद वह विशेष्य पद है और स्व-पर-व्यवसायी वह उनका विशेषण है। स्याद्वाद रत्नाकर ग्रन्थ में श्री वादिदेवसूरि महाराज ने ज्ञान पद की सार्थकता अन्य रूप में भी दिखाई है।120 न्यायादि दर्शनकारों इन्द्रियार्थसन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं।। न्याय मंजरीकार जयंतभह कारणसाक्ल्य (कारण सामग्री) को प्रमाण कहते हैं। जैन दर्शन के अनुसार प्रमाण ज्ञानात्मक ही होता है। सन्निकर्षादि सभी जड़ हैं, अज्ञानात्मक हैं। इसलिए ज्ञान पद से अन्यसम्मत सभी का व्यवच्छेदक होता है, ऐसा स्वाद्वाद रत्नाकर में दिखाया है। इस प्रकार संक्षेप में पदार्थ का यथार्थ (वास्तविक) ज्ञान ही प्रमाण है, वो यथार्थ है। आगमेत्तर युग में प्रमाण का क्रमिक विकास आगमेत्तर युग में जैसे-जैसे न्यायविद्या का विकास हुआ, वैसे-वैसे प्रमाणमीमांसा की आवश्यकता महसूस होने लगी। सर्वप्रथम ज्ञान को प्रमाण रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय वाचक उमास्वाति को है। उन्होंने तत्त्वार्थसूत्र में पहले पाँच ज्ञानों का उल्लेख कर उन्हीं को प्रमाण की संज्ञा दी, यथा मतिश्रुतावधि मनःपर्याय केवलानि ज्ञानमा तत् प्रमाणे। आधे परोक्षम्। प्रत्यक्ष मन्यत्।। अर्थात् मति, श्रुत आदि पांच ज्ञान ही प्रमाण हैं। इनमें प्रथम दो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से होने के कारण परोक्ष प्रमाण। अन्तिम तीन ज्ञान आत्मा की सहायता से होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आचार्य उमास्वाति ने ज्ञान को प्रमाण कहा किन्तु 'ज्ञान ही प्रमाण है' इतना कहने मात्र से वे न्यायविदों को संतुष्ट नहीं कर सके। अतः दार्शनिक दृष्टि से प्रमाण को व्याख्यायित करने का श्रेय मिलता है आचार्य सिद्धसेन और आचार्य समन्तभद्र को। आचार्य सिद्धसेन ने प्रमाण की परिभाषा यह निश्चित की-'प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं (बाधविवर्जितम्) 14 अर्थात् जो स्व-पर-प्रकाशी और निर्दोष ज्ञान है, वह प्रमाण है। सिद्धसेन की इस परिभाषा में बाधविवर्जित पर बौद्ध परम्परा के प्रभाव से गृहित हुआ है, क्योंकि प्रमाणवार्तिक में प्रमाण का लक्षण इस प्रकार है 'प्रमाणविसंवादि ज्ञानमर्थक्रियास्थितिः 125 किया है और बाधविवर्जित अविसंवादित्व का ही पर्याय है। आचार्य समन्तभद्र ने प्रमाण का जो लक्षण निबद्ध किया, वह इस प्रकार है 'स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्'। जो ज्ञान अपना और पर का बोद्ध कराये, वो प्रमाण है। नैयायिकों एवं मीमांसकों की तरह ज्ञान को परोक्ष नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष ही मानते हैं। फिर भी वह ज्ञान को स्वप्रकाश्य तो नहीं मानते हैं, परन्तु प्रकाश्य ही मानते हैं, जैसे-कैसी भी तीक्ष्ण सूई अपने को भेद नहीं सकती है। कैसी भी चतुर नर्तकी अपने कंधे पर तो य नहीं कर सकती है तो फिर ज्ञान कैसा भी क्यों न हो वो स्व को नहीं जान सकता है। वैशेषिक की मान्यता भी ऐसी ही है। मीमांसक, न्याय, वैशेषिकादि की उक्त मान्यता को निरस करते हुए उपाध्याय यशोविजय ने जैन तर्क परिभाषा में दिखाया है कि वास्तव में ज्ञान स्व-पर उभय का निश्चय करता है। प्रदीप के दृष्टान्त से समझ सकते हैं। जैसे प्रदीप वह घट-पटादि वस्तु को प्रकाशित करता है, तब वो स्वयं भी प्रकाशित होता है, उनके लिए अन्य प्रदीप की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक वैसे ही ज्ञान भी अर्थ के साथ 227 Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org