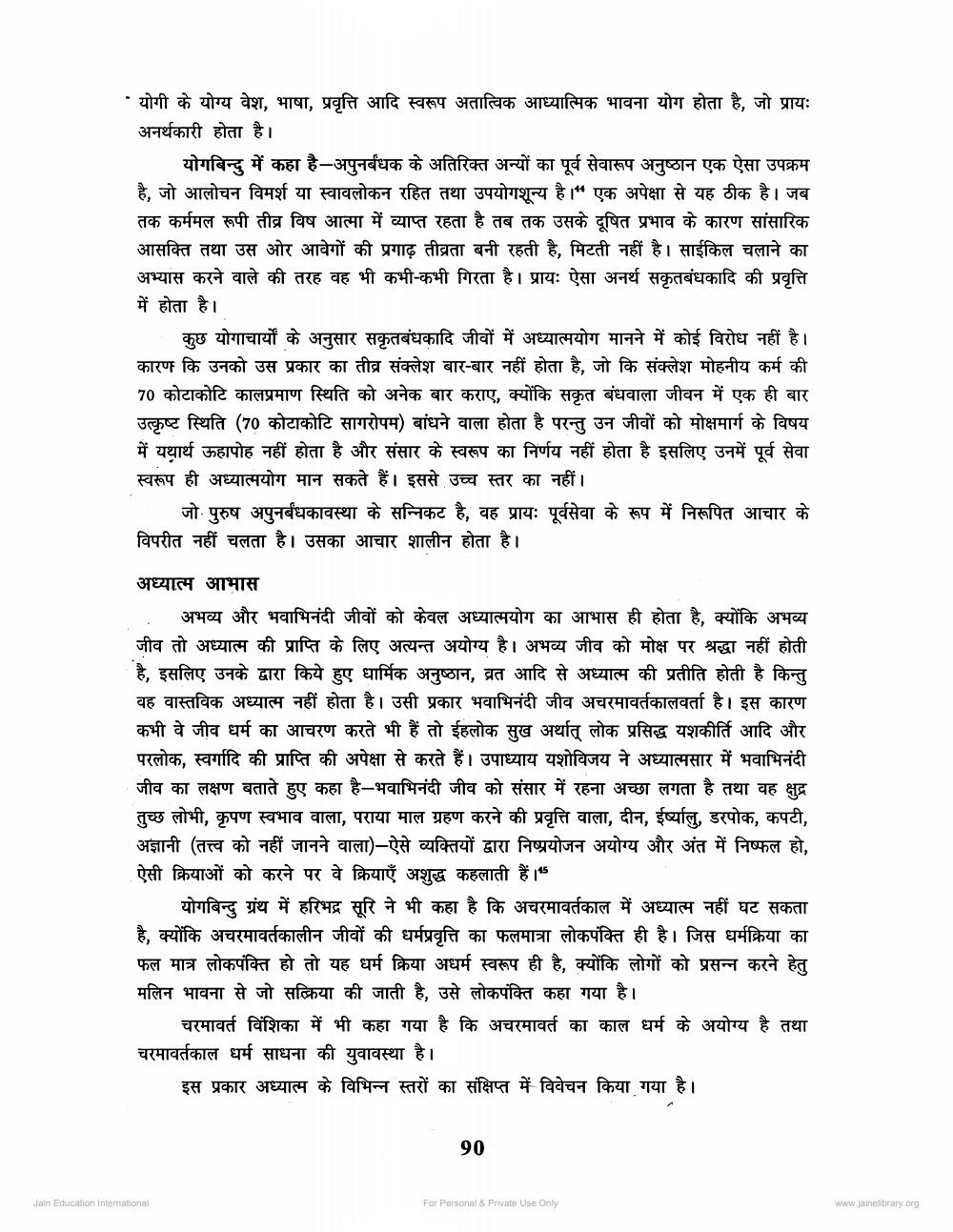________________ योगी के योग्य वेश, भाषा, प्रवृत्ति आदि स्वरूप अतात्विक आध्यात्मिक भावना योग होता है, जो प्रायः अनर्थकारी होता है। योगबिन्दु में कहा है-अपुनर्बंधक के अतिरिक्त अन्यों का पूर्व सेवारूप अनुष्ठान एक ऐसा उपक्रम है, जो आलोचन विमर्श या स्वावलोकन रहित तथा उपयोगशून्य है।" एक अपेक्षा से यह ठीक है। जब तक कर्ममल रूपी तीव्र विष आत्मा में व्याप्त रहता है तब तक उसके दूषित प्रभाव के कारण सांसारिक आसक्ति तथा उस ओर आवेगों की प्रगाढ़ तीव्रता बनी रहती है, मिटती नहीं है। साईकिल चलाने का अभ्यास करने वाले की तरह वह भी कभी-कभी गिरता है। प्रायः ऐसा अनर्थ सकृतबंधकादि की प्रवृत्ति में होता है। कुछ योगाचार्यों के अनुसार सकृतबंधकादि जीवों में अध्यात्मयोग मानने में कोई विरोध नहीं है। कारण कि उनको उस प्रकार का तीव्र संक्लेश बार-बार नहीं होता है, जो कि संक्लेश मोहनीय कर्म की 70 कोटाकोटि कालप्रमाण स्थिति को अनेक बार कराए, क्योंकि सकृत बंधवाला जीवन में एक ही बार उत्कृष्ट स्थिति (70 कोटाकोटि सागरोपम) बांधने वाला होता है परन्तु उन जीवों को मोक्षमार्ग के विषय में यथार्थ ऊहापोह नहीं होता है और संसार के स्वरूप का निर्णय नहीं होता है इसलिए उनमें पूर्व सेवा स्वरूप ही अध्यात्मयोग मान सकते हैं। इससे उच्च स्तर का नहीं। ____जो पुरुष अपुनर्बंधकावस्था के सन्निकट है, वह प्रायः पूर्वसेवा के रूप में निरूपित आचार के विपरीत नहीं चलता है। उसका आचार शालीन होता है। अध्यात्म आभास . अभव्य और भवाभिनंदी जीवों को केवल अध्यात्मयोग का आभास ही होता है, क्योंकि अभव्य जीव तो अध्यात्म की प्राप्ति के लिए अत्यन्त अयोग्य है। अभव्य जीव को मोक्ष पर श्रद्धा नहीं होती है, इसलिए उनके द्वारा किये हुए धार्मिक अनुष्ठान, व्रत आदि से अध्यात्म की प्रतीति होती है किन्तु वह वास्तविक अध्यात्म नहीं होता है। उसी प्रकार भवाभिनंदी जीव अचरमावर्तकालवर्ता है। इस कारण कभी वे जीव धर्म का आचरण करते भी हैं तो ईहलोक सुख अर्थात् लोक प्रसिद्ध यशकीर्ति आदि और परलोक, स्वर्गादि की प्राप्ति की अपेक्षा से करते हैं। उपाध्याय यशोविजय ने अध्यात्मसार में भवाभिनंदी जीव का लक्षण बताते हुए कहा है-भवाभिनंदी जीव को संसार में रहना अच्छा लगता है तथा वह क्षुद्र तुच्छ लोभी, कृपण स्वभाव वाला, पराया माल ग्रहण करने की प्रवृत्ति वाला, दीन, ईर्ष्यालु, डरपोक, कपटी, अज्ञानी (तत्त्व को नहीं जानने वाला)-ऐसे व्यक्तियों द्वारा निष्प्रयोजन अयोग्य और अंत में निष्फल हो, ऐसी क्रियाओं को करने पर वे क्रियाएँ अशुद्ध कहलाती हैं। योगबिन्दु ग्रंथ में हरिभद्र सूरि ने भी कहा है कि अचरमावर्तकाल में अध्यात्म नहीं घट सकता है, क्योंकि अचरमावर्तकालीन जीवों की धर्मप्रवृत्ति का फलमात्रा लोकपंक्ति ही है। जिस धर्मक्रिया का फल मात्र लोकपंक्ति हो तो यह धर्म क्रिया अधर्म स्वरूप ही है, क्योंकि लोगों को प्रसन्न करने हेतु मलिन भावना से जो सक्रिया की जाती है, उसे लोकपंक्ति कहा गया है। चरमावर्त विंशिका में भी कहा गया है कि अचरमावर्त का काल धर्म के अयोग्य है तथा चरमावर्तकाल धर्म साधना की युवावस्था है। इस प्रकार अध्यात्म के विभिन्न स्तरों का संक्षिप्त में विवेचन किया गया है। 90 Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org