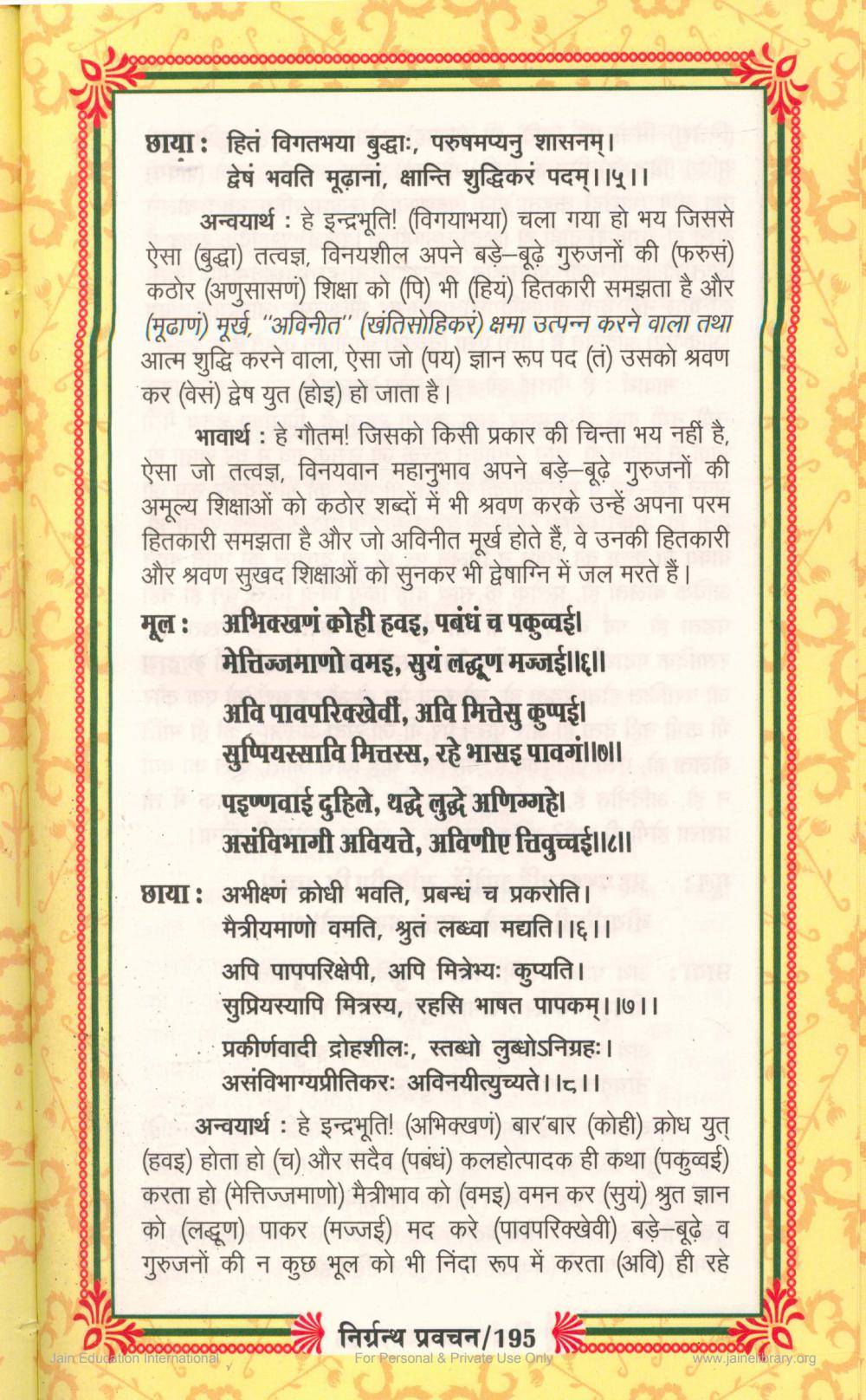________________ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Poo000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 छाया: हितं विगतभया बुद्धाः, परुषमप्यनु शासनम्। द्वेषं भवति मूढ़ानां, शान्ति शुद्धिकरं पदम्।।५।। अन्वयार्थ : हे इन्द्रभूति! (विगयाभया) चला गया हो भय जिससे ऐसा (बुद्धा) तत्वज्ञ, विनयशील अपने बड़े-बूढ़े गुरुजनों की (फरुसं) कठोर (अणुसासणं) शिक्षा को (पि) भी (हियं) हितकारी समझता है और (मूढाणं) मूर्ख, "अविनीत" (खंतिसोहिकर) क्षमा उत्पन्न करने वाला तथा आत्म शुद्धि करने वाला, ऐसा जो (पय) ज्ञान रूप पद (तं) उसको श्रवण कर (वेस) द्वेष युत (होइ) हो जाता है। भावार्थ : हे गौतम! जिसको किसी प्रकार की चिन्ता भय नहीं है, ऐसा जो तत्वज्ञ, विनयवान महानुभाव अपने बड़े-बूढ़े गुरुजनों की अमूल्य शिक्षाओं को कठोर शब्दों में भी श्रवण करके उन्हें अपना परम हितकारी समझता है और जो अविनीत मूर्ख होते हैं, वे उनकी हितकारी और श्रवण सुखद शिक्षाओं को सुनकर भी द्वेषाग्नि में जल मरते हैं। मूल : अभिक्खणं कोही हवइ, पबंधं च पकुम्बई। मेत्तिज्जमाणो वमइ, सुयं लभ्रूण मज्जई||६|| अवि पावपरिक्खेवी, अवि मित्तेसु कुप्पई। सुप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे भासइ पावगं||७|| पइण्णवाई दुहिले, थट्टे लुद्धे अणिग्गहे। असंविभागी अवियत्ते, अविणीए चिवुच्चई|lll छाया: अभीक्ष्णं क्रोधी भवति, प्रबन्धं च प्रकरोति। मैत्रीयमाणो वमति, श्रुतं लब्ध्वा मद्यति।।६।। अपि पापपरिक्षेपी, अपि मित्रेभ्यः कुप्यति। सुप्रियस्यापि मित्रस्य, रहसि भाषत पापकम्।।७।। प्रकीर्णवादी द्रोहशीलः, स्तब्धो लुब्धोऽनिग्रहः / असंविभाग्यप्रीतिकरः अविनयीत्युच्यते।।८।। अन्वयार्थ : हे इन्द्रभूति! (अभिक्खणं) बार बार (कोही) क्रोध युत् (हवइ) होता हो (च) और सदैव (पबंध) कलहोत्पादक ही कथा (पकुव्वई) करता हो (मेत्तिज्जमाणो) मैत्रीभाव को (वमइ) वमन कर (सुयं) श्रुत ज्ञान को (लक्ष्ण) पाकर (मज्जई) मद करे (पावपरिक्खेवी) बड़े-बूढ़े व गुरुजनों की न कुछ भूल को भी निंदा रूप में करता (अवि) ही रहे 9900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000oogl 500000000000000000000000000000000000000000ood निर्ग्रन्थ प्रवचन/195 600000000000000000 Jain Education International For Personal & Private Use Only boo000000000000000 www.jaine brary.org