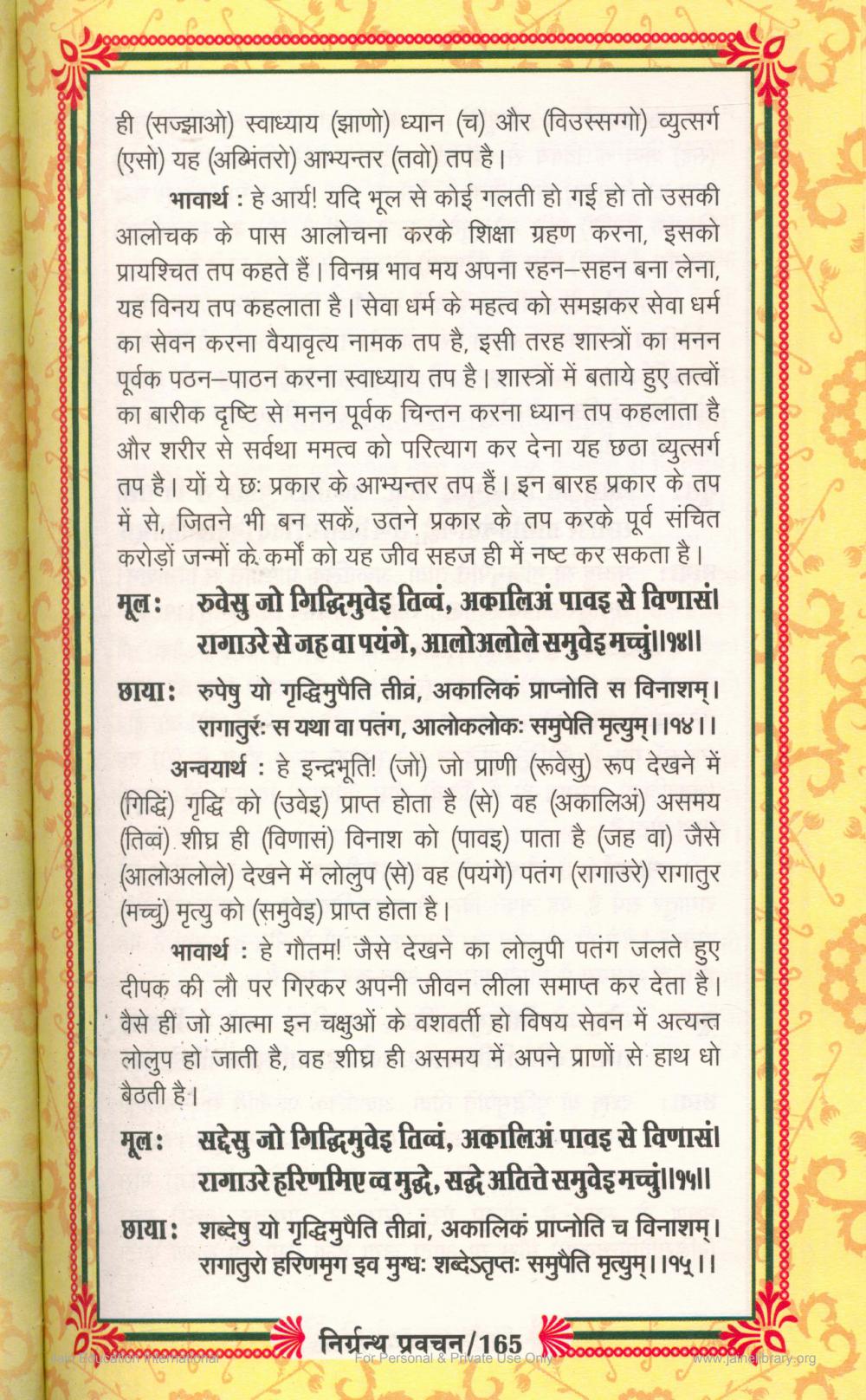________________ 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ope 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ही (सज्झाओ) स्वाध्याय (झाणो) ध्यान (च) और (विउस्सग्गो) व्युत्सर्ग (एसो) यह (अभिंतरो) आभ्यन्तर (तवो) तप है। ___ भावार्थ : हे आर्य! यदि भूल से कोई गलती हो गई हो तो उसकी आलोचक के पास आलोचना करके शिक्षा ग्रहण करना, इसको प्रायश्चित तप कहते हैं। विनम्र भाव मय अपना रहन-सहन बना लेना, यह विनय तप कहलाता है। सेवा धर्म के महत्व को समझकर सेवा धर्म का सेवन करना वैयावृत्य नामक तप है, इसी तरह शास्त्रों का मनन पूर्वक पठन-पाठन करना स्वाध्याय तप है। शास्त्रों में बताये हुए तत्वों का बारीक दृष्टि से मनन पूर्वक चिन्तन करना ध्यान तप कहलाता है और शरीर से सर्वथा ममत्व को परित्याग कर देना यह छठा व्युत्सर्ग तप है। यों ये छः प्रकार के आभ्यन्तर तप हैं। इन बारह प्रकार के तप में से, जितने भी बन सकें, उतने प्रकार के तप करके पूर्व संचित करोड़ों जन्मों के कर्मों को यह जीव सहज ही में नष्ट कर सकता है। मूल: रुवेसु जो गिदिमुवेइ तिवं, अकालिअंपावइ से विणासं। रागाउरेसे जहवापयंगे, आलोअलोले समुवेइमच्||१४|| छायाः रुपेषु यो गृद्धिमुपैति तीवं, अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् / रागातुर्रः स यथा वा पतंग, आलोकलोकः समुपेति मृत्युम्।।१४।। अन्वयार्थ : हे इन्द्रभूति! (जो) जो प्राणी (रूवेस) रूप देखने में (गिद्धि) गृद्धि को (उवेइ) प्राप्त होता है (से) वह (अकालिअं) असमय (तिव्व) शीघ्र ही (विणासं) विनाश को (पावइ) पाता है (जह वा) जैसे (आलोअलोले) देखने में लोलुप (से) वह (पयंगे) पतंग (रागाउरे) रागातुर (मच्छु) मृत्यु को (समुवेइ) प्राप्त होता है। . भावार्थ : हे गौतम! जैसे देखने का लोलुपी पतंग जलते हुए दीपक की लौ पर गिरकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। वैसे ही जो आत्मा इन चक्षुओं के वशवर्ती हो विषय सेवन में अत्यन्त लोलुप हो जाती है, वह शीघ्र ही असमय में अपने प्राणों से हाथ धो बैठती है। मूलः सद्देसु जो गिदिमुवेइ तिळ, अकालिअंपावइ से विणासं| रागाउरे हरिणमिए ब्वमुद्धे,सद्धे अतितेसमुवेइमच्||१५|| छायाः शब्देषु यो गृद्धिमुपैति तीव्रां, अकालिकं प्राप्नोति च विनाशम् / रागातुरो हरिणमृग इव मुग्धः शब्देऽतृप्तः समुपैति मृत्युम्।।१५।। goo00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooood 50000000000000 3000000* निर्ग्रन्थ प्रवचन/165 . MERO For Personal & Pivate Use of 0000000000000000 www.jame brary.org