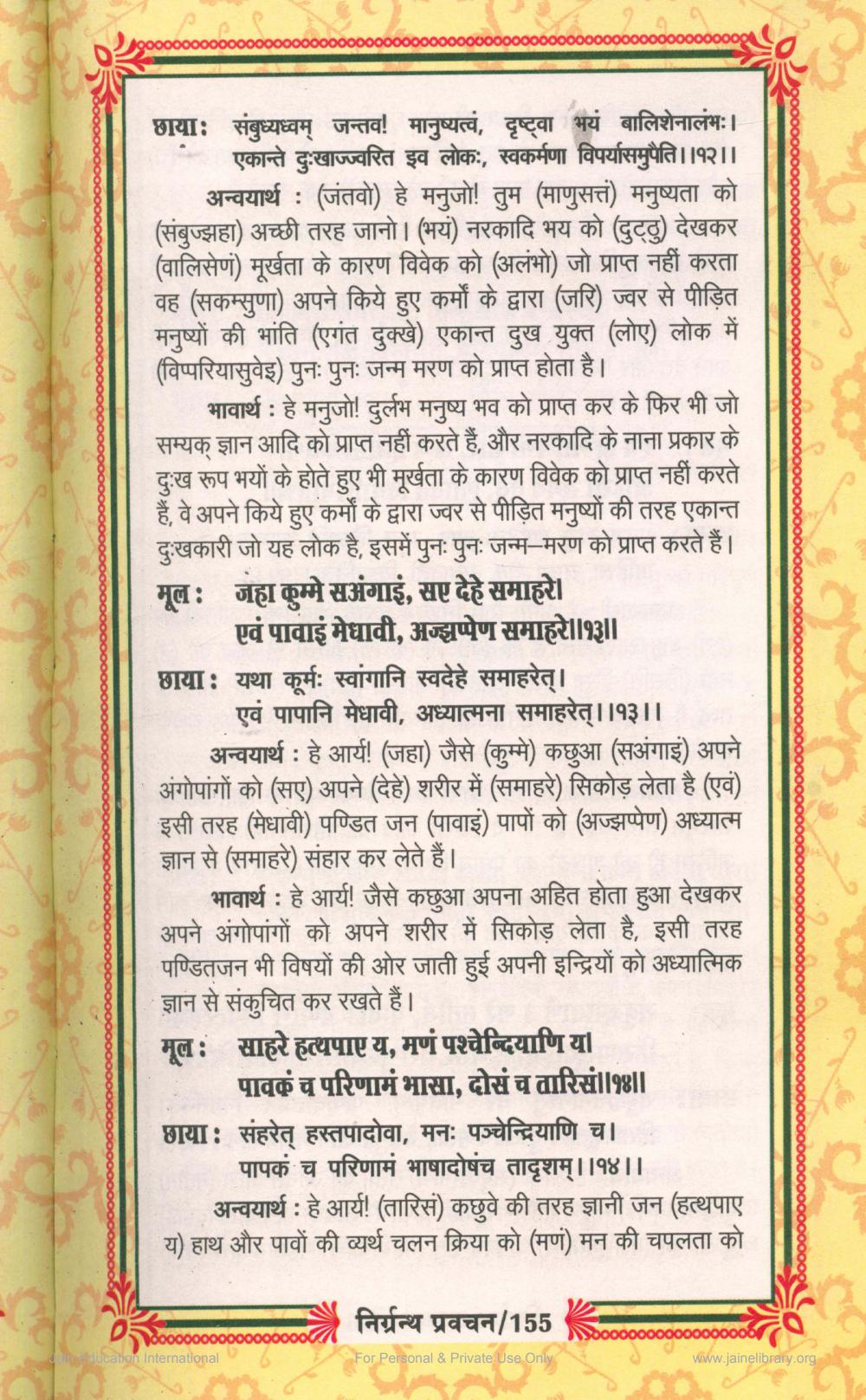________________ 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000oogl 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 छायाः संबुध्यध्वम् जन्तव! मानुष्यत्वं, दृष्ट्वा भयं बालिशेनालंभः। एकान्ते दुःखाज्ज्वरित इव लोकः, स्वकर्मणा विपर्यासमुपैति।।१२।। अन्वयार्थ : (जंतवो) हे मनुजो! तुम (माणुसत्तं) मनुष्यता को (संबुज्झहा) अच्छी तरह जानो। (भयं) नरकादि भय को (दुठ्ठ) देखकर (वालिसेणं) मूर्खता के कारण विवेक को (अलंभो) जो प्राप्त नहीं करता वह (सकम्सुणा) अपने किये हुए कर्मों के द्वारा (जरि) ज्वर से पीड़ित मनुष्यों की भांति (एगंत दुक्खे) एकान्त दुख युक्त (लोए) लोक में (विप्परियासुवेइ) पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त होता है। _भावार्थ : हे मनुजो! दुर्लभ मनुष्य भव को प्राप्त कर के फिर भी जो सम्यक् ज्ञान आदि को प्राप्त नहीं करते हैं, और नरकादि के नाना प्रकार के दुःख रूप भयों के होते हुए भी मूर्खता के कारण विवेक को प्राप्त नहीं करते हैं, वे अपने किये हुए कर्मों के द्वारा ज्वर से पीड़ित मनुष्यों की तरह एकान्त दुःखकारी जो यह लोक है, इसमें पुनः पुनः जन्म-मरण को प्राप्त करते हैं। मूल : जहा कुम्मे सअंगाई, सए देहे समाहरे। एवं पावाई मेधावी, अझप्पेण समाहरे||१३|| छायाः यथा कूर्मः स्वांगानि स्वदेहे समाहरेत्। एवं पापानि मेधावी, अध्यात्मना समाहरेत्।।१३।। अन्वयार्थ : हे आर्य! (जहा) जैसे (कुम्मे) कछुआ (सअंगाई) अपने अंगोपांगों को (सए) अपने (देहे) शरीर में (समाहरे) सिकोड़ लेता है (एवं) इसी तरह (मेधावी) पण्डित जन (पावाइं) पापों को (अज्झप्पेण) अध्यात्म ज्ञान से (समाहरे) संहार कर लेते हैं। __भावार्थ : हे आर्य! जैसे कछुआ अपना अहित होता हुआ देखकर अपने अंगोपांगों को अपने शरीर में सिकोड़ लेता है, इसी तरह पण्डितजन भी विषयों की ओर जाती हुई अपनी इन्द्रियों को अध्यात्मिक ज्ञान से संकुचित कर रखते हैं। मूल: साहरे हत्यपाए य, मणं पश्चेन्दियाणि या पावकं च परिणाम भासा, दोसंच तारिसं||१४|| छायाः संहरेत् हस्तपादोवा, मनः पञ्चेन्द्रियाणि च। पापकं च परिणामं भाषादोषंच तादृशम्।।१४।। _अन्वयार्थ : हे आर्य! (तारिस) कछुवे की तरह ज्ञानी जन (हत्थपाए य) हाथ और पावों की व्यर्थ चलन क्रिया को (मणं) मन की चपलता को 50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000oooog निर्ग्रन्थ प्रवचन/155 GO d 00000000000000000MA ucation International 00000000000 For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.org