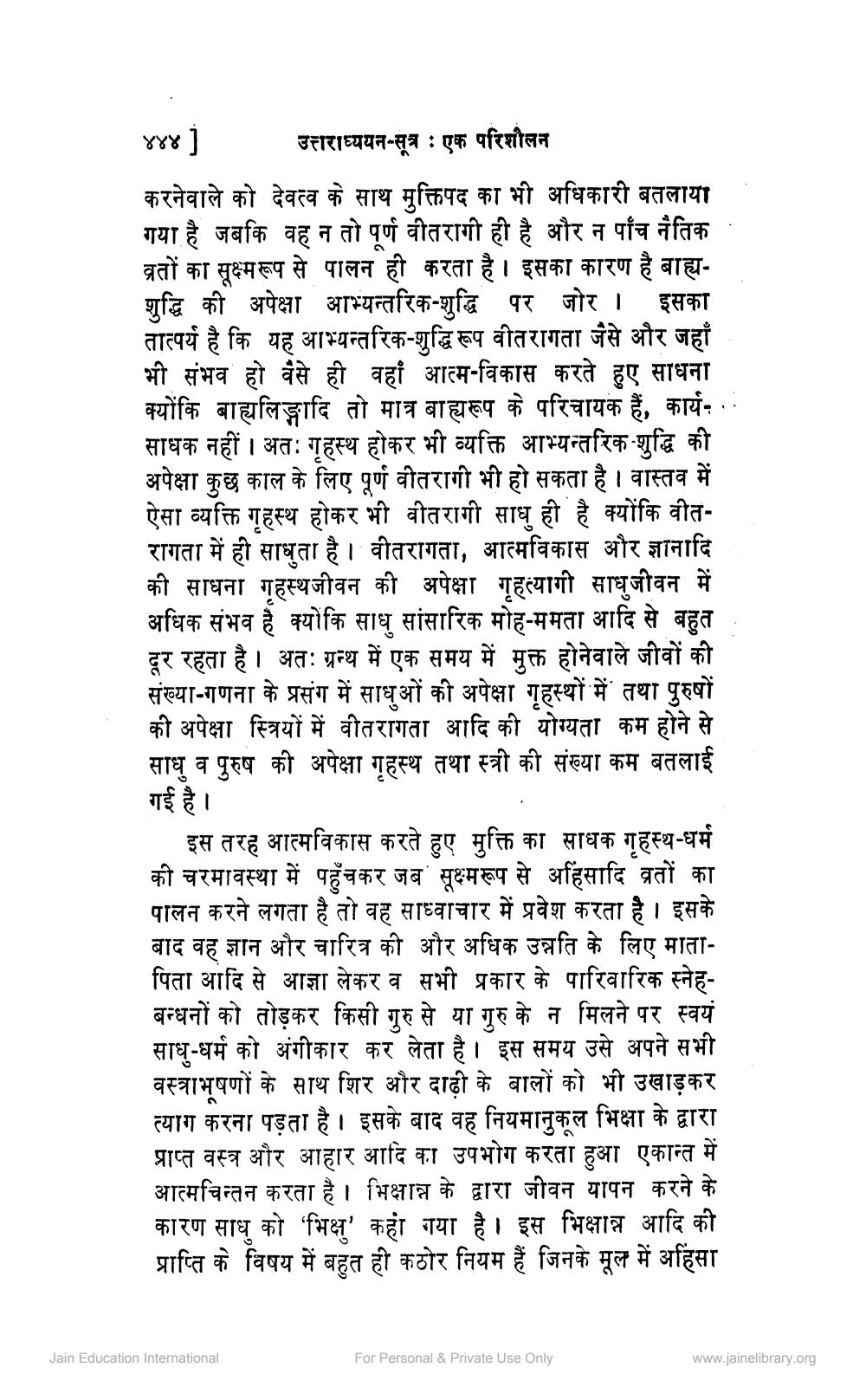________________
४४४ ]
उत्तराध्ययन सूत्र : एक परिशीलन
करनेवाले को देवत्व के साथ मुक्तिपद का भी अधिकारी बतलाया गया है जबकि वह न तो पूर्ण वीतरागी ही है और न पाँच नैतिक व्रतों का सूक्ष्मरूप से पालन ही करता है । इसका कारण है बाह्यशुद्धि की अपेक्षा आभ्यन्तरिक - शुद्धि पर जोर । इसका तात्पर्य है कि यह आभ्यन्तरिक शुद्धि रूप वीतरागता जैसे और जहाँ भी संभव हो वैसे ही वहाँ आत्म-विकास करते हुए साधना क्योंकि बाह्यलिङ्गादि तो मात्र बाह्यरूप के परिचायक हैं, कार्यसाधक नहीं । अतः गृहस्थ होकर भी व्यक्ति आभ्यन्तरिक शुद्धि की अपेक्षा कुछ काल के लिए पूर्ण वीतरागी भी हो सकता है । वास्तव में ऐसा व्यक्ति गृहस्थ होकर भी वीतरागी साधु ही है क्योंकि वीतरागता में ही साधुता है । वीतरागता, आत्मविकास और ज्ञानादि की साधना गृहस्थजीवन की अपेक्षा गृहत्यागी साधुजीवन में अधिक संभव है क्योंकि साधु सांसारिक मोह - ममता आदि से बहुत दूर रहता है । अतः ग्रन्थ में एक समय में मुक्त होनेवाले जीवों की संख्या-गणना के प्रसंग में साधुओं की अपेक्षा गृहस्थों में तथा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में वीतरागता आदि की योग्यता कम होने से साधु व पुरुष की अपेक्षा गृहस्थ तथा स्त्री की संख्या कम बतलाई गई है ।
इस तरह आत्मविकास करते हुए मुक्ति का साधक गृहस्थ-धर्म की चरमावस्था में पहुँचकर जब सूक्ष्मरूप से अहिंसादि व्रतों का पालन करने लगता है तो वह साध्वाचार में प्रवेश करता है । इसके बाद वह ज्ञान और चारित्र की और अधिक उन्नति के लिए मातापिता आदि से आज्ञा लेकर व सभी प्रकार के पारिवारिक स्नेहबन्धनों को तोड़कर किसी गुरु से या गुरु के न मिलने पर स्वयं साधु-धर्म को अंगीकार कर लेता है। इस समय उसे अपने सभी वस्त्राभूषणों के साथ शिर और दाढ़ी के बालों को भी उखाड़कर त्याग करना पड़ता है । इसके बाद वह नियमानुकूल भिक्षा के द्वारा प्राप्त वस्त्र और आहार आदि का उपभोग करता हुआ एकान्त में आत्मचिन्तन करता है । भिक्षान्न के द्वारा जीवन यापन करने के कारण साधु को 'भिक्षु' कहा गया है । इस भिक्षान्न आदि की प्राप्ति के विषय में बहुत ही कठोर नियम हैं जिनके मूल में अहिंसा
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org