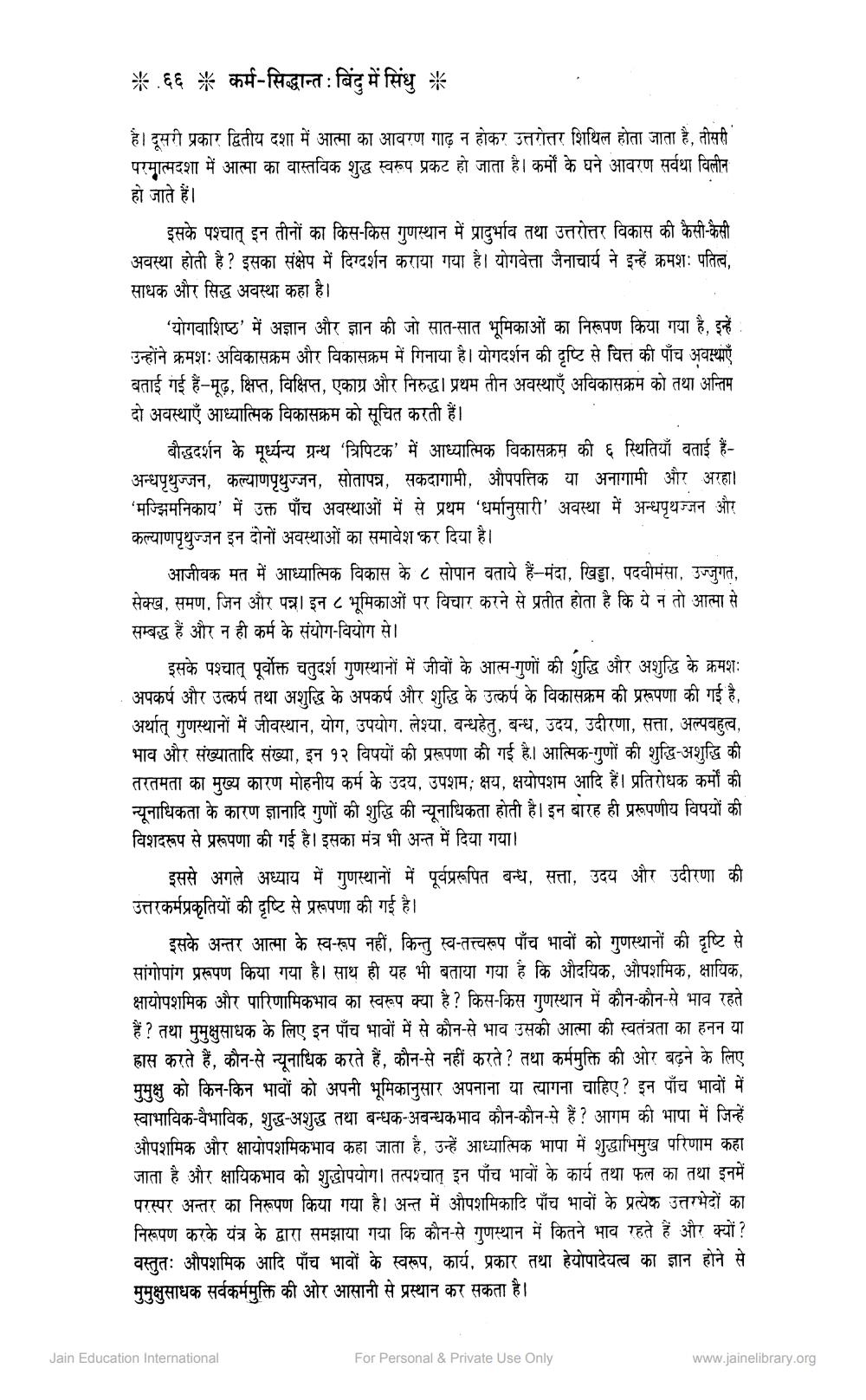________________
*.६६ * कर्म-सिद्धान्त : बिंदु में सिंधु *
है। दूसरी प्रकार द्वितीय दशा में आत्मा का आवरण गाढ़ न होकर उत्तरोत्तर शिथिल होता जाता है, तीसरी परमात्मदशा में आत्मा का वास्तविक शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। कर्मों के घने आवरण सर्वथा विलीन हो जाते हैं।
इसके पश्चात् इन तीनों का किस-किस गुणस्थान में प्रादुर्भाव तथा उत्तरोत्तर विकास की कैसी-कैसी अवस्था होती है ? इसका संक्षेप में दिग्दर्शन कराया गया है। योगवेत्ता जैनाचार्य ने इन्हें क्रमशः पतित्व, साधक और सिद्ध अवस्था कहा है। ___'योगवाशिष्ठ' में अज्ञान और ज्ञान की जो सात-सात भूमिकाओं का निरूपण किया गया है, इन्हें उन्होंने क्रमशः अविकासक्रम और विकासक्रम में गिनाया है। योगदर्शन की दृष्टि से चित्त की पाँच अवस्थाएँ बताई गई हैं-मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। प्रथम तीन अवस्थाएँ अविकासक्रम को तथा अन्तिम दो अवस्थाएँ आध्यात्मिक विकासक्रम को सूचित करती हैं।
बौद्धदर्शन के मू_न्य ग्रन्थ 'त्रिपिटक' में आध्यात्मिक विकासक्रम की ६ स्थितियाँ बताई हैंअन्धपृथुज्जन, कल्याणपृथुज्जन, सोतापन्न, सकदागामी, औपपत्तिक या अनागामी और अरहा। 'मज्झिमनिकाय' में उक्त पाँच अवस्थाओं में से प्रथम 'धर्मानुसारी' अवस्था में अन्धपृथज्जन और कल्याणपृथुज्जन इन दोनों अवस्थाओं का समावेश कर दिया है।
आजीवक मत में आध्यात्मिक विकास के ८ सोपान बताये हैं-मंदा, खिड्डा, पदवीमंसा, उज्जुगत, सेक्ख, समण, जिन और पन्न। इन ८ भूमिकाओं पर विचार करने से प्रतीत होता है कि ये न तो आत्मा से सम्बद्ध हैं और न ही कर्म के संयोग-वियोग से।
इसके पश्चात् पूर्वोक्त चतुदर्श गुणस्थानों में जीवों के आत्म-गुणों की शुद्धि और अशुद्धि के क्रमशः अपकर्ष और उत्कर्ष तथा अशुद्धि के अपकर्ष और शुद्धि के उत्कर्प के विकासक्रम की प्ररूपणा की गई है, अर्थात् गुणस्थानों में जीवस्थान, योग, उपयोग. लेश्या, बन्धहेतु, बन्ध, उदय, उदीरणा, सत्ता, अल्पबहुत्व, भाव और संख्यातादि संख्या, इन १२ विषयों की प्ररूपणा की गई है। आत्मिक-गुणों की शुद्धि-अशुद्धि की तरतमता का मुख्य कारण मोहनीय कर्म के उदय, उपशम; क्षय, क्षयोपशम आदि हैं। प्रतिरोधक कर्मों की न्यूनाधिकता के कारण ज्ञानादि गुणों की शुद्धि की न्यूनाधिकता होती है। इन बारह ही प्ररूपणीय विषयों की विशदरूप से प्ररूपणा की गई है। इसका मंत्र भी अन्त में दिया गया।
इससे अगले अध्याय में गुणस्थानों में पूर्वप्ररूपित बन्ध, सत्ता, उदय और उदीरणा की उत्तरकर्मप्रकृतियों की दृष्टि से प्ररूपणा की गई है।
इसके अन्तर आत्मा के स्व-रूप नहीं, किन्तु स्व-तत्त्वरूप पाँच भावों को गुणस्थानों की दृष्टि से सांगोपांग प्ररूपण किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिकभाव का स्वरूप क्या है ? किस-किस गुणस्थान में कौन-कौन-से भाव रहते हैं ? तथा मुमुक्षुसाधक के लिए इन पाँच भावों में से कौन-से भाव उसकी आत्मा की स्वतंत्रता का हनन या ह्रास करते हैं, कौन-से न्यूनाधिक करते हैं, कौन-से नहीं करते? तथा कर्ममुक्ति की ओर बढ़ने के लिए मुमुक्षु को किन-किन भावों को अपनी भूमिकानुसार अपनाना या त्यागना चाहिए? इन पाँच भावों में स्वाभाविक-वैभाविक, शुद्ध-अशुद्ध तथा बन्धक-अबन्धक भाव कौन-कौन-से हैं ? आगम की भाषा में जिन्हें
औपशमिक और क्षायोपशमिकभाव कहा जाता है, उन्हें आध्यात्मिक भापा में शुद्धाभिमुख परिणाम कहा जाता है और क्षायिकभाव को शुद्धोपयोग। तत्पश्चात् इन पाँच भावों के कार्य तथा फल का तथा इनमें परस्पर अन्तर का निरूपण किया गया है। अन्त में औपशमिकादि पाँच भावों के प्रत्येक उत्तरभेदों का निरूपण करके यंत्र के द्वारा समझाया गया कि कौन-से गुणस्थान में कितने भाव रहते हैं और क्यों? वस्तुतः औपशमिक आदि पाँच भावों के स्वरूप, कार्य, प्रकार तथा हेयोपादेयत्व का ज्ञान होने से मुमुक्षुसाधक सर्वकर्ममुक्ति की ओर आसानी से प्रस्थान कर सकता है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org