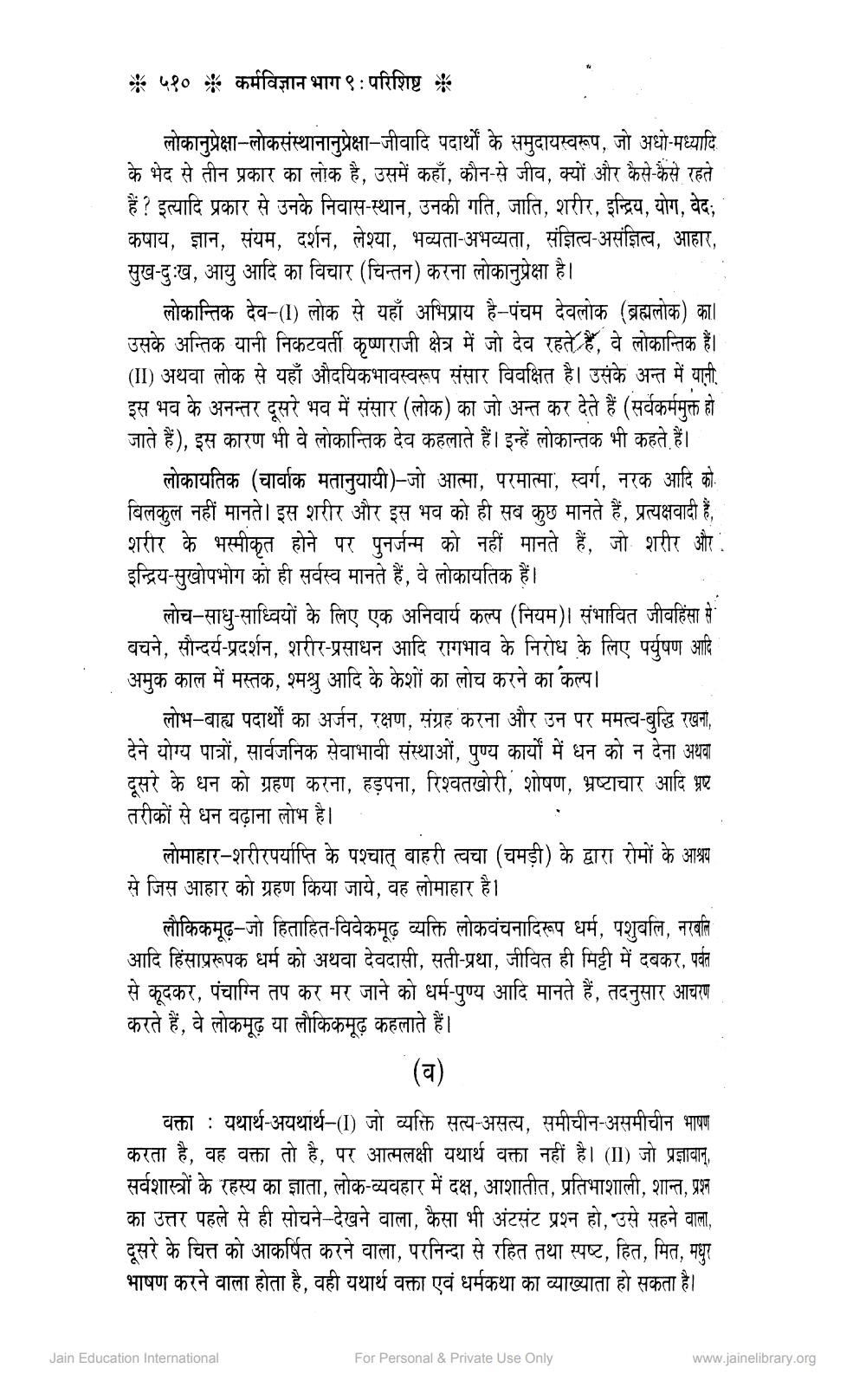________________
* ५१० * कर्मविज्ञान भाग ९ : परिशिष्ट *
लोकानुप्रेक्षा-लोकसंस्थानानुप्रेक्षा-जीवादि पदार्थों के समुदायस्वरूप, जो अधो-मध्यादि के भेद से तीन प्रकार का लोक है, उसमें कहाँ, कौन-से जीव, क्यों और कैसे-कैसे रहते हैं ? इत्यादि प्रकार से उनके निवास-स्थान, उनकी गति, जाति, शरीर, इन्द्रिय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यता-अभव्यता, संज्ञित्व-असंज्ञित्व, आहार, सुख-दुःख, आयु आदि का विचार (चिन्तन) करना लोकानुप्रेक्षा है।
लोकान्तिक देव-(1) लोक से यहाँ अभिप्राय है-पंचम देवलोक (ब्रह्मलोक) का। उसके अन्तिक यानी निकटवर्ती कृष्णराजी क्षेत्र में जो देव रहते हैं, वे लोकान्तिक हैं। (II) अथवा लोक से यहाँ औदयिकभावस्वरूप संसार विवक्षित है। उसके अन्त में यानी. इस भव के अनन्तर दूसरे भव में संसार (लोक) का जो अन्त कर देते हैं (सर्वकर्ममुक्त हो जाते हैं), इस कारण भी वे लोकान्तिक देव कहलाते हैं। इन्हें लोकान्तक भी कहते हैं।
लोकायतिक (चार्वाक मतानुयायी)-जो आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक आदि को. बिलकुल नहीं मानते। इस शरीर और इस भव को ही सब कुछ मानते हैं, प्रत्यक्षवादी हैं, शरीर के भस्मीकृत होने पर पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, जो शरीर और . इन्द्रिय-सुखोपभोग को ही सर्वस्व मानते हैं, वे लोकायतिक हैं।
लोच-साधु-साध्वियों के लिए एक अनिवार्य कल्प (नियम)। संभावित जीवहिंसा से वचने, सौन्दर्य-प्रदर्शन, शरीर-प्रसाधन आदि रागभाव के निरोध के लिए पर्युषण आदि अमुक काल में मस्तक, श्मश्रु आदि के केशों का लोच करने का कल्प। ___लोभ-बाह्य पदार्थों का अर्जन, रक्षण, संग्रह करना और उन पर ममत्व-बुद्धि रखना, देने योग्य पात्रों, सार्वजनिक सेवाभावी संस्थाओं, पुण्य कार्यों में धन को न देना अथवा दूसरे के धन को ग्रहण करना, हड़पना, रिश्वतखोरी, शोषण, भ्रष्टाचार आदि भ्रष्ट तरीकों से धन बढ़ाना लोभ है। __लोमाहार-शरीरपर्याप्ति के पश्चात् बाहरी त्वचा (चमड़ी) के द्वारा रोमों के आश्रय से जिस आहार को ग्रहण किया जाये, वह लोमाहार है। ___ लौकिकमूढ़-जो हिताहित-विवेकमूढ़ व्यक्ति लोकवंचनादिरूप धर्म, पशुबलि, नरबलि आदि हिंसाप्ररूपक धर्म को अथवा देवदासी, सती-प्रथा, जीवित ही मिट्टी में दबकर, पर्वत से कूदकर, पंचाग्नि तप कर मर जाने को धर्म-पुण्य आदि मानते हैं, तदनुसार आचरण करते हैं, वे लोकमूढ़ या लौकिकमूढ़ कहलाते हैं।
वक्ता : यथार्थ-अयथार्थ-(I) जो व्यक्ति सत्य-असत्य, समीचीन-असमीचीन भाषण करता है, वह वक्ता तो है, पर आत्मलक्षी यथार्थ वक्ता नहीं है। (II) जो प्रज्ञावान्, सर्वशास्त्रों के रहस्य का ज्ञाता, लोक-व्यवहार में दक्ष, आशातीत, प्रतिभाशाली, शान्त, प्रश्न का उत्तर पहले से ही सोचने-देखने वाला, कैसा भी अंटसंट प्रश्न हो, उसे सहने वाला, दूसरे के चित्त को आकर्षित करने वाला, परनिन्दा से रहित तथा स्पष्ट, हित, मित, मधुर भाषण करने वाला होता है, वही यथार्थ वक्ता एवं धर्मकथा का व्याख्याता हो सकता है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org