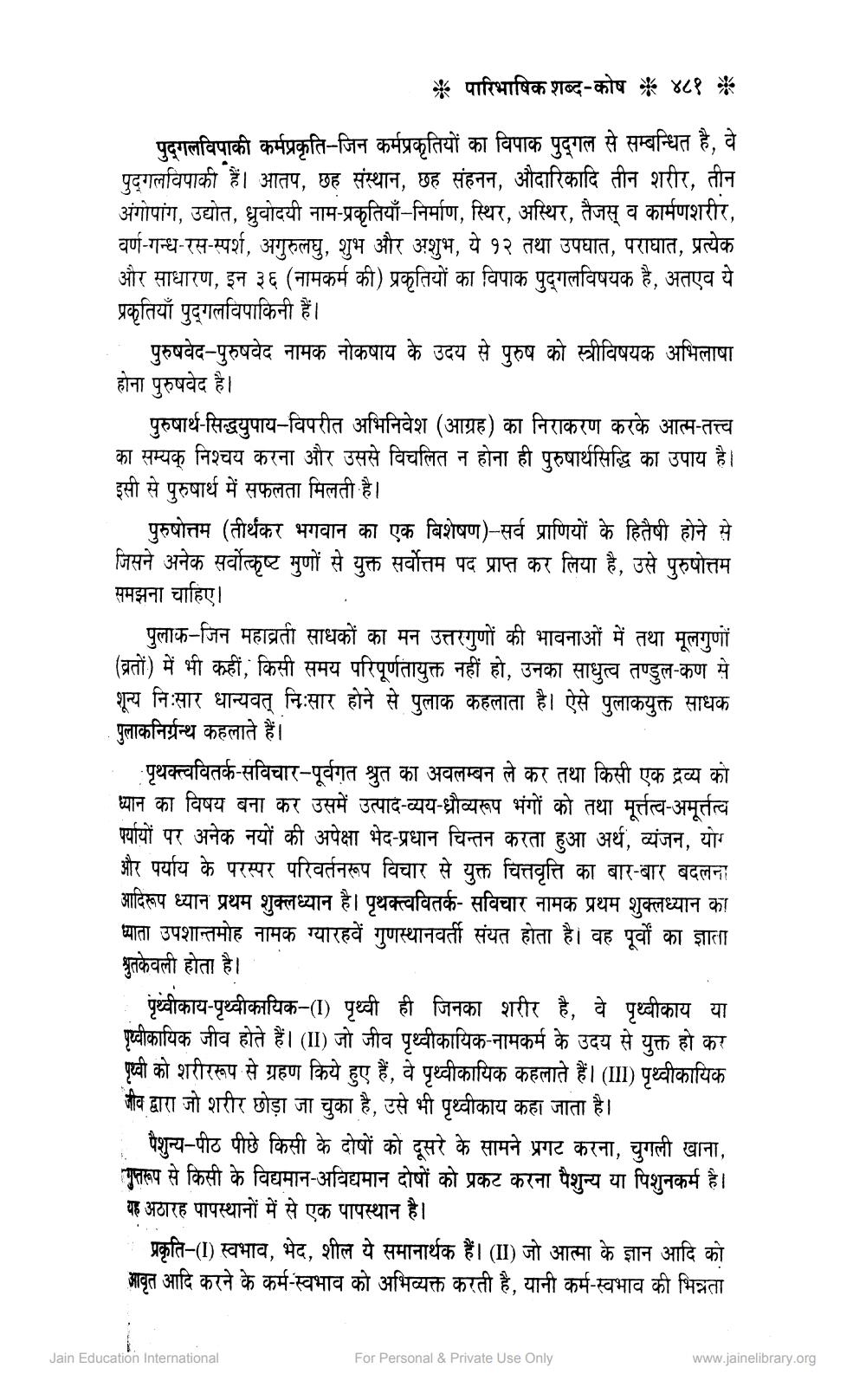________________
* पारिभाषिक शब्द-कोष * ४८१ *
पुद्गलविपाकी कर्मप्रकृति-जिन कर्मप्रकृतियों का विपाक पुद्गल से सम्बन्धित है, वे पुद्गलविपाकी हैं। आतप, छह संस्थान, छह संहनन, औदारिकादि तीन शरीर, तीन अंगोपांग, उद्योत, ध्रुवोदयी नाम-प्रकृतियाँ-निर्माण, स्थिर, अस्थिर, तेजस् व कार्मणशरीर, वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श, अगुरुलघु, शुभ और अशुभ, ये १२ तथा उपघात, पराघात, प्रत्येक
और साधारण, इन ३६ (नामकर्म की) प्रकृतियों का विपाक पुद्गलविषयक है, अतएव ये प्रकृतियाँ पुद्गलविपाकिनी हैं।
पुरुषवेद-पुरुषवेद नामक नोकषाय के उदय से पुरुष को स्त्रीविषयक अभिलाषा होना पुरुषवेद है।
पुरुषार्थ-सिद्धयुपाय-विपरीत अभिनिवेश (आग्रह) का निराकरण करके आत्म-तत्त्व का सम्यक् निश्चय करना और उससे विचलित न होना ही पुरुषार्थसिद्धि का उपाय है। इसी से पुरुषार्थ में सफलता मिलती है। ___पुरुषोत्तम (तीर्थकर भगवान का एक विशेषण)-सर्व प्राणियों के हितैषी होने से जिसने अनेक सर्वोत्कृष्ट मुणों से युक्त सर्वोत्तम पद प्राप्त कर लिया है, उसे पुरुषोत्तम समझना चाहिए।
पुलाक-जिन महाव्रती साधकों का मन उत्तरगुणों की भावनाओं में तथा मूलगुणों (व्रतों) में भी कहीं, किसी समय परिपूर्णतायुक्त नहीं हो, उनका साधुत्व तण्डुल-कण से शून्य निःसार धान्यवत् निःसार होने से पुलाक कहलाता है। ऐसे पुलाकयुक्त साधक पुलाकनिर्ग्रन्थ कहलाते हैं। __-पृथक्त्ववितर्क-सविचार-पूर्वगत श्रुत का अवलम्बन ले कर तथा किसी एक द्रव्य को ध्यान का विषय बना कर उसमें उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप भंगों को तथा मूर्तत्व-अमूर्तत्व पर्यायों पर अनेक नयों की अपेक्षा भेद-प्रधान चिन्तन करता हुआ अर्थ, व्यंजन, योग और पर्याय के परस्पर परिवर्तनरूप विचार से युक्त चित्तवृत्ति का बार-बार बदलना आदिरूप ध्यान प्रथम शुक्लध्यान है। पृथक्त्ववितर्क- सविचार नामक प्रथम शुक्लध्यान का ध्याता उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती संयत होता है। वह पूर्वो का ज्ञाता श्रुतकेवली होता है।
पृथ्वीकाय-पृथ्वीकायिक-(I) पृथ्वी ही जिनका शरीर है, वे पृथ्वीकाय या पृथ्वीकायिक जीव होते हैं। (II) जो जीव पृथ्वीकायिक-नामकर्म के उदय से युक्त हो कर पृथ्वी को शरीररूप से ग्रहण किये हुए हैं, वे पृथ्वीकायिक कहलाते हैं। (III) पृथ्वीकायिक जीव द्वारा जो शरीर छोड़ा जा चुका है, उसे भी पृथ्वीकाय कहा जाता है।
पैशुन्य-पीठ पीछे किसी के दोषों को दूसरे के सामने प्रगट करना, चुगली खाना, गुप्तरूप से किसी के विद्यमान-अविद्यमान दोषों को प्रकट करना पैशुन्य या पिशुनकर्म है। यह अठारह पापस्थानों में से एक पापस्थान है।
प्रकृति-(I) स्वभाव, भेद, शील ये समानार्थक हैं। (II) जो आत्मा के ज्ञान आदि को आवृत आदि करने के कर्म-स्वभाव को अभिव्यक्त करती है, यानी कर्म-स्वभाव की भिन्नता
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org